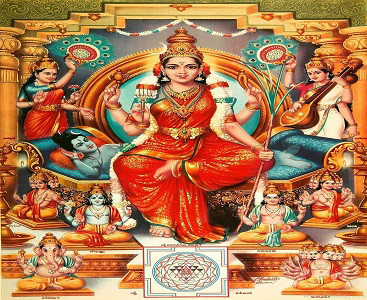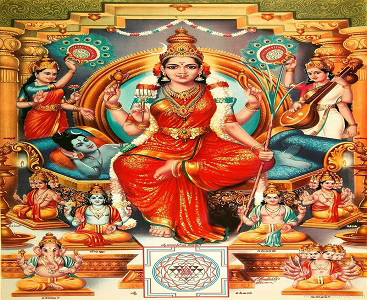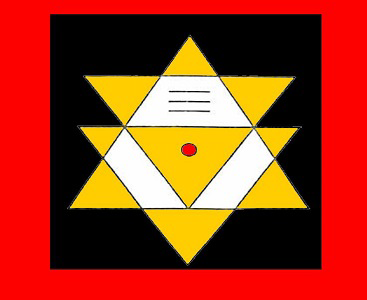रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
संक्षिप्त विवरण - तान्त्रिक-संस्कृति का विहंगावलोकन
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
संक्षिप्त विवरण - वैदिक एवं तान्त्रिक साधना
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
संक्षिप्त विवरण - तन्त्र प्रवर्तक ऋषि
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
संक्षिप्त विवरण - तान्त्रिक सम्प्रदायों का मार्मिक साम्य
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
संक्षिप्त विवरण - बृहत्तर भारत में तान्त्रिक सम्प्रदाय
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
संक्षिप्त विवरण - योग और आत्मसाक्षात्कार
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
संक्षिप्त विवरण - उन्मेष एवं निमेषावस्था
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
संक्षिप्त विवरण - प्राणायाम की प्रक्रिया
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
संक्षिप्त विवरण - बन्ध एवं मुद्राएँ
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
संक्षिप्त विवरण - रुद्रयामलगत स्वरयोग
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
संक्षिप्त विवरण - स्वर-विज्ञान
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
संक्षिप्त विवरण - बिना औषध के रोगनिवारण
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
संक्षिप्त विवरण - हठयोग के षट्कर्म
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
संक्षिप्त विवरण - स्वरयोग से रोग निवारण
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
संक्षिप्त विवरण - कुण्डलिनीयोग
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
संक्षिप्त विवरण - नाडीचक्र का रहस्य
कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।
योगरन्धितकर्माणो ह्रदि योगविभाविते ।
योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् ॥
- श्रीमद्भाग ०८ . ३ . २७
योग के द्वारा कर्म , कर्म वासना और कर्मफल को भस्म करके योगी जन योग से विशुद्ध अपने ह्रदय में जिन योगेश्वर भगवान् का दर्शन करते हैं । उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ ।
पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयंभूस्तस्मात्पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् ।
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥
कठोपनिषद् २ .१ .१
समस्त जन संसार में स्वभावतः बहिर्मुख ही उत्पन्न होते हैं । उनमें कोई विरला योगी ही अमृतत्व की कामना से अन्तर्मुख होकर प्रत्यगात्मा को देखता है ।
ओंकार का जप और तेज का ध्यान ही शब्दब्रह्म की उपासना है । इस लोक में दो प्रकार के शब्द सुने जाते हैं , एक नित्य तथा दूसरा कार्यरुप अनित्य । जो शब्द सुना जाता है या उच्चरित होता हैं , वह लोक व्यवहार के लिए प्रवृत्त वैखरी रुप कार्यात्मक अनित्य है । पश्यन्ती रुप शब्द ब्रह्मात्मक बिम्ब के ही वर्ण (मात्रुकाएँ ), पद और वाक्य प्रतिबिम्ब हैं । पश्यन्ति रुप नित्य शब्दात्मा समस्त साध्य साधनात्मक पद और पदार्थ भेद रुप व्यवहार का उपादान कारण है । अकार ककारादि क्रम का वहाँ उपसंहार हो जाता है । अतः समस्त कर्मों का आश्रय , सुख -दुःख का अधिष्ठान , घट के भीतर रखे हुए दीपक के प्रकाश की भाँति भोगायतन शरीर मात्र का प्रकाशक ‘शब्दब्रह्म ’ उच्चारण करने वाले जनों के ह्रदय में विद्यमान रहता है । योगी उसी शब्द तत्त्व स्वरुप महानात्मा के साथ ऐक्य लाभ करता हुआ वैकरण्य (लय ) को प्राप्त करता है ।
नाद्योग में साधक दक्षिणकर्ण में ‘अनाहत ’ को सुनता है । अभ्यास करने पर क्रमशः घण्टा -वादन , मेघ -गर्जन एवं तालवादन आदि दस प्रकार के नाद सुनायी पडते हैं । अन्तिम नाद ओंकार है , उसी में मन का लय करना चाहिए । तभी स्वरुपस्थिति प्राप्त होती है । ऐसा ही नादबिन्दूपनिषद् में कहा भी है --
सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां सन्धाय वैष्णवीम् ।
श्रुणुयाद् दक्षिणे कर्णे नादमन्तर्गतं सदा ॥
हठयोगप्रदीपिका (४ . २९ , ८३ . ५९ ) में कहा गया है कि ---
इन्दियाणां मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः ।
मारुतस्य लयो नाथः स लयो नादमाश्रितः ॥
अभ्यस्यमानो नादोऽयं ब्राह्ममावृणुते ध्वनिम् ।
पश्चाद् विक्षेपमखिलं जित्वा योगी सुखी भवेत् ॥
कर्पूरमनले यद्वत् सैन्धवं सलिले यथा ।
तथा संघीयमानं च मनस्तत्त्वे विलियते ॥
यह लय योग ही कुण्डलिनी योग के नाम से प्रसिद्ध है ---
लयक्रिया साधनेन सुप्ता सा कुलकुण्डली ।
प्रबुद्ध्य तस्मिन् पुरुषे लीयते नात्र संशयः ॥
शिवत्वमाप्नोति तया सह्रदयस्य साधकः ।
यह कुण्डलिनी योग इस प्रकार से जाना जाता है ---शरीर में मेरुदण्ड के नीचे ‘मूलाधार ’ के नाम से प्रसिद्ध एक कन्द है । बहत्तर हजार नाडियाँ उससे निकलकर सम्पूर्ण देह में व्याप्त रहती हैं । उनमें इडा , पिङुला और सुषुम्ना नामक तीन नाडियाँ मुख्य हैं । मेरुदण्ड के वामभाग में चन्द्ररुपिणी इडा का , दक्षिण भाग में सूर्यरुपिणी पिङुला का और मध्य छिद्र में सुषुम्ना का मार्ग है । भ्रूमध्य में संगम प्राप्त करके ये नाडियाँ सिर में ब्रह्मान्ध्रपर्यन्त जाती है । मूलाधार में महाशक्ति कुलकुण्डलिनी सोती रहती है । ध्यान और जप आदि से उसे जगाकर सहस्त्रार चक्र (मस्तिष्क ) में विराजमान परमेश्वर में लीन करना ही लय योग या कुण्डलिनी योग है । सम्पूर्ण रुद्रयामल के ९० अध्यायों में इन्हीं महाशक्ति कुलकुण्डलिनी के जागरण की प्रक्रिया का साङोपाङ दिग्दर्शन परिलक्षित होता है ।
2.. संक्षिप्त विवरण - आगमशास्त्र
आगमशास्त्र
रुद्रयामलतन्त्र एवं योग ---
प्रस्तुत रुद्रयामल प्राय . ६ हजार श्लोकों में उपनिबद्ध है । इस तन्त्र की मुख्य विषयवस्तु महाशक्ति कुलकुण्डलिनी के जागरण से सम्बन्धित है । इस योग की सिद्धि के लिए साधक (योगी ) के जीवन में यम एवं नियम का अनुष्ठान परमावश्यक है । साथ ही साथ आसन सिद्ध करना भी आवश्यक है । कुछ कुछ मात्रा में प्राणायाम के अभ्यास से प्राणों (श्वासों ) की गति में समत्व लाना भी नितान्त आवश्यक है । जिसका आहार विकृत होता है , उसके प्राण (श्वसन तन्त्र आदि ) भी विकृत एवं कुपित हो जाते हैं । जिनके प्राण विकृत या कुपित होते हैं उनका मन कभी एकाग्र नहीं होता । अतः प्राणों की स्थिरता एवं समत्व के लिए आहार की शुद्धि परमावश्यक होती है । योग के इन्हीं अङों की प्रयोग पद्धति का वर्णन रुद्रयामल में किया गया है । प्रयोग पद्धति में पूजा एवं अर्चना के लिए ८ सहस्त्रनाम अनेक कवच एवं स्तुतियाँ जिनमे कुलकुण्डलिनी की स्तुति मुख्य है ।
आगमशास्त्र और रुद्रयामल
महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज ने अपनी ‘तन्त्र और आगम शास्त्रों का दिग्दर्शन ’ नामक पुस्तक में तत्त्व से प्रारम्भ करके साहित्य तक के शीर्षकों में जो बातें बतलाई हैं उनमें सुविधा की दृष्टी से हम पहले ‘साहित्य ’ शीर्षक लेते है , जिसके अन्तर्गत उन्होंने दस शिवागम , अष्तादश रुद्रागम , चौंसठ भैरवागम , चौसठ कुलमार्ग तन्त्र , समय मार्ग के शुभागम पंचक और नवयुग के चौसठ तन्त्रों का उल्लेख किया है ।
तांत्रिक साहित्य के इतिहास में दस शिवागम और अष्टादश रुद्रागम अष्टाविंश आगम के नाम से प्रसिद्ध हैं ।
‘ किरणागम ’ के अनुसार परमेश्वर ने सबसे पहले दस शिवों को उत्पन्न करके उनमें से प्रत्येक को अपने अविभक्त महाज्ञान का एक - एक हिस्सा दिया । यह अविभक्त महाज्ञान ही पूर्ण शिवागम है । उन दस शिवों तथा उन्हें प्राप्त आगमों तथा उनके तीन श्रोताओं के नाम निम्नलिखित है ; ---
इसी तरह अठारह रुद्र हैं , जिनके अठारह आगम है और उनके दो -दो श्रोता है । उन रुद्रागमों और उनके श्रोताओं के नाम निम्नलिखित हैं ,---
मुकुटतन्त्र में रुद्र -भेद विविध हैं । यद्यपि अठारहवें रुद्र और उनके एक श्रोता का नाम उपलब्ध नहीं होता फिर भी सिद्धान्त के अनुसार १८ x२ =३६ रुद्रज्ञान हैं । शिव तथा रुद्र दोनें के सिद्धान्त ज्ञानों को मिलाकर ३० +३६ =६६ शिव -रुद्र ज्ञान विभक्त हैं ।
कामिकागम के अनुसार सदाशिव के पाँच मुख है -सद्योजात , वामदेव , अघोर , तत्पुरुष और ईशान । जिनके पाँच स्त्रोत हैं ---लौकिक , वैदिक , आध्यात्मिक , अतिमार्ग और मन्त्र ।
सोम -सिद्धान्त के अनुसार उपर्यक्त पाँच स्त्रोतों वाले पाँच तन्त्र , पाँच -पाँच प्रकार के हैं । सिद्धान्तदीपिका एवं "शतरत्न " के अनुसार उपर्युक्त वर्णन हैं । उपर्युक्त विवरण को निम्नलिखित रुपरेखा में देखा जा सकता है।
कविराज जी ने नेपाल लाइब्रेरी में उपलब्ध "निःश्वास -तत्त्व -संहिता " नामक एक पोथी की चर्चा की है , जिसमें ---१ . लौकिक धर्मसूत्र . २ मूलसूत्र , ३ . उत्तर सूत्र (आदि सूत्र ), ४ . नय सूत्र (प्रथम सूत्र ), ५ गुह्य सूत्र इन पाँच सूत्रों या विभागों का उल्लेख किया है और बतलाया है कि आदि या उत्तर सूत्र में अठारह प्राचीन शिव -सूत्रों का उल्लेख है , जो वास्तव में उन नामों से प्रचलित आगम ही हैं । उनमें दस शिवतन्त्र है । ‘कालिकागम ’ के अनुसार अथारह तन्त्र बतलाये गये है । इन्होंने ज्ञान -सम्बन्धी शुद्धमार्ग , अशुद्धमार्ग और मिश्रमार्ग , इन तीन मार्गों का उल्लेख किया है और पशु , माया आदि तत्वों के ज्ञान की अपेक्षा शिवप्रतिपादक ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बतलाया हैं । सिद्धान्त -मत के अनुसार वेदादि -सम्बन्धी ज्ञान से सिद्धान्त ज्ञान को विशुद्ध और श्रेष्ठ बतलाया गया है । यह ज्ञान भी परापर भेद से भिन्न -भिन्न प्रकार का है ।
‘ कामिकागम ’ और " स्वायंभुव आगम " के अनुसार परापर भेद का उल्लेख किया गया है । अधिकारी भेद से ज्ञान के भेद किये गये है । पतिप्रतिपादक ज्ञान को परज्ञान और पशुप्रतिपादक ज्ञान को अपरज्ञान कहा गया है । शिव प्रकाश ज्ञान को पर या श्रेष्ठ कहा गया है तथा पशु - पाश आदि अर्थ प्रकाशज्ञान को अपर - ज्ञान कहा गया है । यहाँ स्मरणीय है कि शिव - ज्ञान और रुद्रज्ञान को सिद्धान्त - ज्ञान कहत हैं । कविराज जी ने यह भी बतलाय है कि पाशुपतों में उपर्युक्त अठारह रौद्रागमों की प्रामाणिकता मानी जाती है क्योंकी उन ( रौद्रागमों ) में द्वैतदृष्टि से अद्वैतदृष्टि का मिश्रण है । प्ररन्तु दस शिवागमों में अद्वैतदृष्टि को अंगीकृत वे नहीं मानते । अतः अभिनवगुप्त भी पाशुपतमत को सर्वथा हेय नहीं मानते । इस प्रकार से शिवागमों और रुद्रागमों की चर्चा करने के बाद चौसठ भैरवागमों का उल्लेख किया गया है ।
चौसठ भैरवागम
तन्त्रालोक के प्रसिद्ध टीकाकार जयरथ ने श्रीकंठ -सहिता के अनुसार चौसठ भैरवागम -अद्वैतागमों का उल्लेख किया है । वे निम्नलिखित आठ अष्टकों में विभक्त हैं --१ भैरवाष्टक , २यामलाष्टक , ३ .मताष्टक ४ . मंगलाष्टक , ५ .चक्राष्टक , ६ .बहुरुपाष्टक , ७ .वागीशाष्टक , और ८ .शिखाष्टक (६४ )।
इन आठ अष्टकों में प्रथम और द्वितीय अष्टक के एक -एक तन्त्र का नाम नहीं मिलता । नवीं शताब्दी के प्रारम्भ में शिखाष्टक के वीणाशिवा , सम्मोह और शिरश्छेद नामक तन्त्र भारत से कम्बोज देश पहुँचे गये थे । यहाँ यह भी बतलाया गया है कि एक चौथा तन्त्र भी जो ‘नयोत्तर ’ नाम से प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख प्रबोधचन्द्र वागची ने स्टडीज इन दि तन्त्राय , वाल्यूम १ , पृष्ठ २ में किया हैं और उन्होंने बतलाया है , कि नेपाल में सरंक्षित "निःश्वास तत्त्व संहिता "" अठारह रौद्रागमों के अन्तर्गत "निःश्वास तन्त्र " क ही दूसरा नाम है । जिसके चार भाग हैं , उन सभी को मिलाकर ‘नयोत्तर तन्त्र ’ कहा जाता है ।
3…संक्षिप्त विवरण - चौसठ तन्त्र
चौसठ तन्त्र (कुल मार्ग)
शंकराचार्य द्वारा लिखित आनन्दलहरी में चौसठ तन्त्रो की चर्चा की गई है । आनन्द लहरी के प्रसिद्ध टीकाकार लक्ष्मीधर ने "चतुःषष्ट्या तन्त्रैः सकलमनुन्धाय भुवनम् " श्लोक संख्या -३१ का पाठ संशोधन करते हुए बतलाया है कि इस श्लोक में महामाय , शम्बर आदि चौसठ तन्त्रों के द्वारा सभी प्रपञ्चो की वञ्चना की बात की गयी है । इन तन्त्रों में से प्रत्येक में किसी न किसी सिद्धि का वर्णन किया गया है । अतः देवी के अनुरोध से भगवान् शंकर ने एक महत्त्वपूर्ण पुरुषार्थ साधक भगवती -तन्त्र का निर्माण किया । "चतुःशती " "नित्याषोडशिकार्णव " एवं भास्कर राय के सेतुबंध टीका में चौंसठ तन्त्रों की विस्तृत व्याख्या है । लक्ष्मीधर की व्याख्या के अनुसार ये कुलामार्ग के चौसठ तन्त्र वैदिक मार्ग से पृथक् और जगत् के विनाशक हैं । पैसठवें तन्त्र के विषय में कया गया है कि भग्वान् के मन्त्र -रहस्य शिव शक्ति दोनों के सम्मिश्रण से उभयात्मक है । चतुःशती में उल्लिखित चौसठ तन्त्रों का उल्लेख किया गया है , जिनमें बहुरुपाष्टक के भीतर आठ तन्त्रों में एक का नाम नहीं मिलता तथा अन्तिम सप्तक में सात की जगह आठ क्षपणक मत के तन्त्रो का उल्लेख किया गया है ।
इन सभी तन्त्रों ऐहिक फलों पर विशेष ध्यान है पारमार्थिक पर नहीं । इसीलिए लक्ष्मीधर ने इन्हें अवैदिक कहा है । लेकिन उन्होने यह भी प्रश्न उठाया है कि करुणावरुणालय उस परमेश्वर ने इस प्रकार की ऐहिकता सिद्धि वाले शास्त्रों की अवतारणा क्यों की ? और वहाँ उत्तर भी दिया है कि पशुपतिशिव ने सभी वर्णो के लिए तन्त्रों की रचना की । किन्तु प्रत्येक वर्ण का अधिकार सभी तन्त्रों के लिए नहीं है । ब्राह्मण , क्षत्रिय , वैश्य (षडशी )विशुद्ध चन्द्रकला विद्या के अधिकारी है । शूद्र लोग ही इन चौसठ तन्त्रों के अधिकारी हैं । ये आठ विशुद्ध चन्द्रकला विद्याएँ अवैदिक चन्द्रकला विज्ञान से भिन्न हैं । इनके नाम १ . चन्द्रकला , २ज्योत्स्नावती , ३ कुलार्णव , ४ .कुलेश्वरी , ५भुवनेश्वरी , ६ .बार्हस्पत्य , ७दुर्वासामत और ८ . आठवीं का नाम नहीं दिया गया है । इन सभी तन्त्रों के त्रिवर्ण के साथ शूद्र भी अधिकारी हैं । पर त्रिवर्ण दक्षिणमार्गी और शूद्र वाम मार्गी होते है । पण्डित कविराज ने इस विद्या कुल मार्ग और समय मार्ग का मिश्रण बतलाया है ।
समय मार्ग या शुभागम पञ्चक
१ . सनक , २ .सनन्दन , ३ .सनत्कुमार , ४ .वसिष्ठ और ५ .शुक -संहिताओं को शुभागम पञ्चक कहा जाता है । यह वैदिक मार्ग है . । यह समयाचार के आधार पर अवलम्बित है । लक्ष्मीधर के अनुसार स्वयं शंकराचार्य इस समयाचार का अनुगमन करते थे । शुभागम पंचक में मूल विद्या कें अन्तर्गत षोडश विद्याएँ स्वीकृत हैं और चौसठ विद्याओं की चन्द्रज्ञानविद्या के अन्तर्गत सोलह नित्याओं की प्रधानता मान्य है । इसीलिए यह मार्ग कौल मार्ग कहा जाता है । ऊपर जिस एक पृथक पैसथवें तन्त्र की बात की गई है , भास्कर राय के अनुसार यह सम्भवतः "वामकेश्व्र तन्त्र " है , जिसके भीतर ही नित्याषोडशिकार्णव आ जाता है । "सौंदर्यलहरी " के टीकाकार गौरीकान्त के अनुसार यह पैसठवाँ तन्त्र ‘ज्ञानार्णव ’ तोडल की सूची में प्राप्त है । दूसरे लोग उस स्वतन्त्र तन्त्र को विशिष्ट मानकर उसे "तन्त्रराज " कहते है ।
नवयुग के चौसठ तन्त्र
" तोडल तन्त्र "," सर्वोल्लास तन्त्र " में आए चौसठ तन्त्रों के नामों की तुलना चतुःशती और श्रीकण्ठी की सूची से करनेके बाद इनमें अन्तर पाया है । " तोडल तन्त्र " की सूची सर्वान्द के सर्वोल्लास में दी गई है जिसमें काली , मुण्डमाला , तारा से लेकर कामाख्या तन्त्र मे चौसठ तन्त्रों का नाम उल्लिखित बतलाया है । इसकी सूची उपर्युक्त सूची से भिन्न है । इस तन्त्र की सन् १७५४ ई० की लिपिबद्ध की गई पोथी " इण्डिया आफिस लाइब्रेरी " लंदन में हैं ।
आठवीं सदी से पहले " जयद्रथयामल " की तन्त्र सम्बन्धी बहुत सी बाते स्पष्ट होती है । आठ प्रकार के यामलों का मूल है ब्रह्मयामल । यामलाष्टक की भाँति ही मंगलाष्टक , चक्राष्टक , शिखाष्टक आदि तन्त्र वर्ग की चर्चा जयद्रथयामल में है ।
जयद्रथयामल में विद्यापीठ के तन्त्रों का नाम लिया गया है । इस पुस्तक की एक पोथी नेपाल दरबार में संरक्षित है । यहाँ ११७४ ई० की लिखी पिंगलामत नामक भी एक पोथी है । जिसे ब्रह्मयामल का परिशिष्ट बतलाया गया है । पिंगलामत के अनुसार पुराने समय में ब्रह्मयामल के अनुसरण करने वाले सात तन्त्र प्रचलित थे जिनमें दुर्वासामत और सारस्वतमत प्रसिद्ध थे ।
इस प्रकार महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज ने तन्त्र साहित्य से परिचय कराने के लिए दस शिवागम , अष्टादश रुद्रागम , चौसठ भैरवागम , चौसठ तन्त्र -कुल मार्ग , शुभागम पंचक (समय मार्ग ) तथा नवयुग के चौसठ तन्त्रों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है ।
4………..संक्षिप्त विवरण - तान्त्रिक-संस्कृति का विहंगावलोकन
तान्त्रिक-संस्कृति का विहंगावलोकन
यह अत्यन्त आनन्द का विषय है कि वर्तमान युग में हम लोगों का ध्यान अपनी प्राचीन संस्कृति के स्वरुप के अनुसन्धान में क्रमशः सचेत एवं आकृष्ट होता जा रहा है । वेद तथा लुप्तप्राय वैदिक साहित्य के पुनरुद्धार के लिए प्रतीच्य एवं भारतीय विद्वामों ने जो सुदीर्घ कालव्यापी अक्लान्त परिश्रम किया , उससे हम सब लोग परिचित हैं । तत्कालीन भारतीय शासन की ओर से पुरातत्त्व विभाग की जब से स्थापना हुई , तब से यहाँ के प्राचीन इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों में -विशेषतः स्थापत्य , भास्कर्य ,मुद्रा , शिलालेख प्रभृति विषयों में -बहुत से भूले हुए तथ्यों का उद्घाटन हुआ है । यह एक विचित्र संयोग है कि आधुनिक युग में विस्मृतप्राय वैदिक वाङ्मय के पुनरुद्धार की दिशा में जिस प्रकार मोक्षमूलर प्रभृति प्रतीच्य मनीषियों का प्राथमिक उद्यम रहा है , ठीक उसी प्रकार विस्मृतप्राय तान्त्रिक वाङ्मय की ओर सब से पहले दृष्टि आकृष्ट करने का श्रेय भी प्रतीच्य मनीविषयों को ही प्राप्त है । इस विषय में सर जान उडरफ उपनाम आर्थर एवलेन को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए । यद्यापि विभिन्न स्थानों से आंशिक एवं विकीर्ण रुप में तान्त्रिक ग्रन्थों का प्रकाशन -कार्य हो रहा है , किन्तु मात्र वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से ही इस कार्य में अधिक उत्साह दिखाया जा रहा है ।
भारतीय आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रायः सभी प्रकार के साधनों का एक विशिष्ट स्थान काशी रहा है । बुद्धदेव के समय से ही , बल्कि उनके भी पहले से विद्या के केन्द्र रुप में काशी की प्रसिद्धि थी । विदेशी से आये पर्यटकों के विवरण से भी यह बात सिद्ध होती है । ऐतिहासिक गवेषणा के प्रभाव से प्रभाव से इस विषय में विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी । मध्ययुग से वर्तमान समय तक दृष्टि देने प्रतीत होगा कि इस समय में भी बहुसंख्यक विशिष्ट तान्त्रिक साधक और ग्रन्थकार काशी में आविर्भूत हुए थे ।
उदाहरणस्वरुप कई साधकों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं ---
( १ ) सरस्वती तीर्थ --- ये परमहंस परिव्राजकाचार्य थे और दक्षिण से आये हुए प्रकाण्ड विद्वान् थे । ये वेदान्त , मीमांसा , सांख्य , साहित्य तथा व्याकरण के छात्रों को पढाया करते थे । इनका मुख्य ग्रन्थ शङ्कराचार्य कृत प्रपञ्चसारतन्त्र की टीका थी ।
( २ ) राघवभट्ट --- इनके पिता नासिक से काशी आकर बस गये । राघवभट्ट जन्म से ही काशी में थे । इन्होंने शारदातिलक की टीका पदार्थादर्श लिखी थी जो सर्वत्र प्रसिद्ध है । इस टीका की रचना काशी में हुई थी । रचनाकाल १४९४ ई० है ।
( ३ ) सर्वानन्द परमहंस --- पूर्वबङके बहुत उच्चकोटि के सिद्ध पुरुष थे । इन्होंने दसों महाविद्याओं का एक साथ साक्षात्कार किया था । यह भी प्रायः चार सौ वर्ष पहले की बात है । इनका अन्तिम समय काशी में ही बीता । किसी - किसी के मत से ये राजगुरु मठ में रहते थे । इनकी अलौकिक शक्तियाँ बहुत थीं । सर्वोल्लासतन्त्र इनका संकलित तन्त्रग्रन्थ है ।
( ४ ) विद्यानन्दनाथ --- ये दक्षिण भारत के निवासी थे । काञ्ची से भी दक्षिण में इनका घर था । ये सर्वशास्त्र के पण्डित थे , किन्तु तन्त्रशास्त्र में विशेष अनुराग था । ये तीर्थयात्रा के प्रसंग से जलन्धर नामक सिद्धपीठ में गये थे । वहाँ सुन्दराचार्य या सच्चिदानन्दनाथ नामक एक सिद्ध पुरुष से मिले थे , उनसे दीक्षा लेकर स्वयं ‘ विद्यानन्दनाथ दीक्षित ’ यह नाम धारण किया और गुरु के आदेश से काशी में आकर रहने लगे । काशी रहते हुए इन्होंने तन्त्रशास्त्र के अनेक विशिष्ट ग्रन्थो का प्रणयन किया । ये भी प्रायः चार सौ वर्ष पहले के आचार्य होंगे ।
( ५ ) महीधर --- ये अहिच्छत्र उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मण्डल के रामनगर से आये थे और काशी में आन्तिम समय तक रहे । इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ नौका टीका सहित मन्त्रमहोदधि है । रचनाकाल १६४५ वि ) सं० ( १५८८ ईशवीय ) है ।
( ६ ) नीलकण्ठ चतुर्द्धर --- ये प्रतिष्ठान ( पैठान ) के थे , किन्तु आजीवन काशी में रहे । महाभारत के टीकाकार रुप से इनकी विशेष प्रसिद्धि है । इन्होंने तन्त्रशास्त्र में शिवताण्डव की टीका लिखी जिस टीका का नाम ‘ अनूपाराम ’ है । रचनाकाल १६८० ईशवीय माना जाता है ।
( ७ ) प्रेमनिधि पन्त --- ये कूर्माचल से काशी आये हुए थे । ये जीवनान्त तक काशी में ही रहे । इन्होंने बहुत से तान्त्रिक ग्रन्थों का निर्माण किया जिनमें शिवताण्डव की टीका मल्लादर्श का नाम लिया जा सकता है । शारदातिलक तथा तन्त्रराज पर भी इन्होंने टीका लिखी थी । ये करीब २५० वर्ष पहले रहा करते थे ।
( ८ ) भास्कर राय --- ये दक्षिण देश के निवासी थे , किन्तु दीर्घकाल तक काशी में ही रहे । सिद्धपुरुष के रुप में इनकी ख्याति थी । इन्होंने ललितासहस्त्रनाम की टीका , योगिनीह्रदय पर सेतुबन्ध टीका , वरिवस्यारहस्य आदि अनेक ग्रन्थ लिखे थे । १९२९ ईशवीय के आसपास इनका जानना चाहिए ।
( ९ ) शंकरानन्दनाथ --- इनका पूर्व नाम प० शंभु भट्ट था । ये अद्वितीय मीमांसक प० खण्डदेव के शिष्य थे और मीमांसा में ग्रन्थ लिखे । ये श्री विद्या के अनन्य उपासक थे । इनका सुन्दरीमहोदय नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । १७०७ ई० इनका समय माना जाता है ।
( १० ) माधवानन्दनाथ --- ये सौभाग्यकल्पद्रुम के रचियता हैं । यह ग्रन्थ परमानन्द - तन्त्र के आधार पर लिखा गया है । ये भी काशी में ही रहे । इनका समय आज से १५० वर्ष पूर्व माना जाता हैं ।
( ११ ) क्षेमानन्द --- माधवानन्द के शिष्य क्षेमानन्द प्रसिद्ध तान्त्रिक विद्वान् थे । इन्होंने सौभाग्यकल्पलतिका का निर्माण किया था ।
( १२ ) सुभगानन्दनाथ --- एक प्रसिद्ध तान्त्रिक आचार्य काशी में रहते थे । ये केरल देश के थे , इनका पूर्वनाम श्रीकण्ठ था । ये काशी में तन्त्र तथा वेद दोनों के अध्यापक थे । ये माधवानन्दजी के ही समसामायिक माने जाते हैं ।
( १३ ) काशीनाथ भट्ट --- इनका भी नाम उल्लेख योग्य है । इन्होंने छोटे - छोटे अनेक तान्त्रिक ग्रन्थ लिखे थी । ये अधिक प्राचीन नहीं , अपितु १०० वर्ष पहले के हैं ।
5………संक्षिप्त विवरण - वैदिक एवं तान्त्रिक साधना
…वैदिक एवं तान्त्रिक साधना
इस विशाल भारतीय संस्कृति का विश्लेषण करने पर प्रतीत होगा कि इसके विभिन्न अंश हैं , और अङ -प्रत्यङु रुप में इसके विभिन्न विभाग हैं । इसमें सन्देह नहीं कि इसमें ‘वैदिक -साधना ’ ही प्रधान है , किन्तु इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि भिन्न -भिन्न समयों में इस धारा में नये -नये ववर्यन हो चुके हैं । धर्मशास्त्र , नीतिशास्त्र , इतिहास -पुराणादि के आलोचन से तथा भारतीय समाज के आन्तरिक जीवन का परिचय मिलने से उपर्युक्त तथ्य का स्पष्टतया ज्ञान होगा । वैदिकधारा का प्राधान्य होने पर भी , इसमें सन्देह नहीं है कि इसमें विभिन्न धाराओं का संमिश्रण है । इन सब धाराओं के भीतर यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो ज्ञात होगा कि ‘तन्त्र की धारा ’ ही प्रथम एवं प्रधान है । इस धारा की भी बहुत से दिशाएँ हैं , जिनमे एक वैदिकधारा के अनुकूल थी । अगली पीढियों के गवेषण -गण इस तथ्य का निरुपण करेंगे कि वैदिकधारा की जो उपासना की दिशा है , वह अविभाज्य रुप से बहुत अंशों में तान्त्रिकधारा से मिलि हुई है , और बहुत से तान्त्रिक विषय अति प्राचीन समय से परम्पराक्रम से चले आ रहे थे। उपनिषद् आदि में जिन विद्याओं का परिचय मिलता है , यथा संवर्ग , उद्गीथ , उपकोशल , भूमा , दहर , पर्यङ्क आदि , ये सभी विद्याएँ इसी के अन्तर्गत हैं । वेद के रहस्य अंश में भी इन सब रहस्य विद्याओं के परिज्ञान का आभास मिलता है । यहाँ तक कहा जा सकता है कि वैदिक क्रिया -काण्ड भी अध्यात्म -विद्या का ही बाह्य रुप है , जो निम्न अधिकारियों के लिए उपयोगी माना जाता था । यदि इन सब अध्यात्म -विद्याओं का रहस्य -ज्ञान कभी हो जाय , तो पता चलेगा कि मूलभूत वैदिक तथा तान्त्रिक या आगामिक ज्ञानों में विशेष भेद नहीं रहा ।
वेद एवं तन्त्रों की मौलिक दृष्टि
यहाँ प्रसंगतः एक बात का उल्लेख आवश्यक है कि साधारण दृष्टि से संभव है यह समझ में न आवे , फिर भी यह सत्य है कि वेद और तन्त्र का निगूढ रुप एक ही प्रकार का है । दोनों ही अक्षरात्मक है , अर्थात् शब्दात्मक ज्ञान विशेष हैं । ये शब्द लौकिक नहीं दिव्य हैं , और अपौरुषेय हैं । मन्त्रदर्शीगण इसे ही प्राप्त कर सर्वज्ञत्व -लाभ किया करते थे ; वे अन्त में आत्मसाक्षात्कार के द्वारा अपना जीवन सफल करते थे । ‘पुराकल्प ’ में लिखा है --
यां सूक्ष्मां विद्याम् अतीन्द्रियां वाचम् ऋषयः साक्षात्कृतधर्माणः मन्त्रदृशः पश्यन्ति , ताम् असाक्षात्कृतधर्मेभ्यः प्रतिवेदयिष्यमाणा बिल्मं समामनन्ति , स्वप्रवृत्तमिव दृष्टश्रुतानुभूतम् आचिख्यासन्ते ।
निरुक्त प्रभृति ग्रन्थों के आलोचन से यह प्रतीत होता है कि ऋषिगण साक्षात्कृत -धर्मा थे और वे उन सामान्य लोगों को उपदेश द्वारा मन्त्र -दान करते थे , जो असाक्षात्कृतधर्मा थे । साक्षात्क्रृतधर्मा होने के कारण ऋषिगण वस्तुतः शक्तिशाली थे , अतः वे किसी से उपदेश -श्रवण करके ऋषित्व -लाभ नहीं करते थे ; प्रत्युत वे स्वयं वेदार्थ -दर्शन करते थे । इसी अभिप्राय से उन्हें मन्त्रद्रष्टा कहा जाता है । मन्त्रार्थ -ज्ञान का मुख्य उपाय है प्रतिभान , इसे ही प्रातिभ या अनौपदेशिकं ज्ञान कहते हैं । इसी के विषय में कहा जाता है ---
गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः ।
गुरु शब्द से यहाँ अन्तर्गुरु या अन्तर्यामी समझना चाहिए । ऐसे उत्तम अधिकारियों को दृष्टर्षि भी कहा जाता है । शक्ति की मन्दता के कारण मध्यम अधिकारी इनसे अवर समझे जाते थे । इनका परिचय श्रुतर्षि नाम से मिलता है । उत्तम अधिकारी को दर्शन मिलता था उपदेश -निरपेक्ष होकर , और मध्यम अधिकारी को श्रवण -प्राप्त होता था उपदेश -सापेक्ष होकर । प्रथम ज्ञान का नाम आर्षज्ञान और द्वितीय का नाम औपदेशिक ज्ञान है । मनुसंहिता के अनुसार धर्मज्ञ वही है जो ऋषिदृष्ट वेद तथा तन्मूलक स्मृति शास्त्रों को वेदानुकूल तर्क से विचारता है ---
आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्रविरोधिना ।
यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्मं वेद नेतरः ॥ मनु० १२ १०६
किन्तु साधारण अधिकारी को जो ज्ञान होता है , वह सत् तर्क के द्वारा । सत्तर्क से अभिप्रेत है वेद शास्त्र के अविरोधी तर्क के द्वारा अनुसंधान । आगम शास्त्र (त्रि० र० तथा त्रिकदार्शनिक साहित्य ) में सत्तर्क का विशेष रुप से मण्डन किया गया है । वैदिक साहित्य में भी यह लिखित मिलता है । ऋषिगण जब अन्तर्हित होने लगे तो तर्क पर ही ज्ञान का भार दिया गया । सभी साधारण जिज्ञासु लोग अवर -कोटि में है , हम सभी इसी कोटि के है । इस प्रकार के लिए सत्तर्क ही अवलम्बनीय है ।
आगम
तन्त्र शास्त्रों के अनुसार तन्त्र का मूल आधार कोई पुस्तक नहीं है , वह अपौरुषेय ज्ञान विशेष है । ऐसे ज्ञान का नाम ही ‘आगम ’ है । यह ज्ञानात्मक आगम शब्दरुप में अवतरित होता है । तन्त्र -मत में परा -वाक् ही अखण्ड आगम है । पश्यन्ति अवस्था में यह स्वयं वेद्य रुप में प्रकाशित होता है और अपना प्रकाश अपने साथ रखता है । यही साक्षात्कार की अवस्था है , यहाँ द्वितीय या अपर में ज्ञान -संचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । वही ज्ञान मध्यमा वाक् में अवतीर्ण होकर ‘शब्द ’ का आकार धारण करता हैं और यह शब्द चित्तात्मक है । इसी भूमि में गुरु -शिष्य भाव का उदय होता है । फलतः ज्ञान एक आधार से अपर आधार में संचारित होता है । विभिन्न शास्त्रों एवं गुरु -परस्पराओं का प्राकट्य मध्यमा -भूमि में ही होता है । वैखरी में वह ज्ञान या शब्द जब स्थूल रुप धारण करता है , तब वह दूसरों के इन्द्रिय का विषय बनता है ।
उपर्युक्त संक्षित्प विवेचन से प्रतीत होगा कि वेद और तन्त्रों की मौलिक दृष्टि एक ही है यद्यपि वेद एक है किन्तु विभक्त होकर यह त्रयी या चतुर्विध होता है , अन्ततः वह अनन्त है। ‘वेदा अनन्ताः ’ यह भी वेद की ही वाणी है । आगमों की स्थिति भी ठीक इसी प्रकार की हैं । अवश्य ही तन्त्र की एक और भी दिशा है जिससे उसका वैदिक आदर्शो से किसी अंश में पार्थक्य प्रतीत होता है , और उस कारण से तान्त्रिक साधना का वैशिष्ट्य भी समझ में आता हैं । कुछ भी हो , ये सभी मिल कर भारतीय संस्कृति के अंगीभूत हो चुके है । जैसे बृहत् जलधारायें मिलकर नदी का रुप धारण करती है , और अन्त में महासमुद्र में विलीन हो जाती हैं ; वैसे ही वैदिक तान्त्रिक आदि अन्यान्य सांस्कृतिक -धारायें भारतीय संस्कृति में आश्रय -लाभ करती हैं और उसे विशाल से विशालत बनाती हैं ।
6…..संक्षिप्त विवरण - तन्त्र प्रवर्तक ऋषि
तन्त्र प्रवर्तक ऋषि
ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति का विचार करने पर प्रतीत होता है कि प्राचीन काल से ही वैदिक तथा तान्त्रिक -साधन -धाराओं में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है ; यह बात जैसे सत्य है , वैसे ही यह बी सत्य है कि दोनों में अंशतः वैलक्षण्य भी है । अति प्राचीन काल से ही शिष्ट जनों द्वारा तन्त्रों के समादार के असंख्य प्रमाण उपलब्ध है । ऐसी प्रसिद्धि है कि बहुसंख्यक देवता भी तान्त्रिक साधना के द्वारा सिद्धि -लाभ करते थे । तान्त्रिक साधना का परम आदर्श था -शाक्त -साधना , जिसका लक्ष्य था - महाशक्ति जगदम्बा की मातृरुप में उपासना अथवा शिवोपासना । ब्रह्मा , विष्णु , इन्द्र , चन्द्र , स्कन्द , वीरभद्र , लक्ष्मीश्वर , महाकाल , काम या मन्मथ ये सभी श्रीमाता के उपासक थे । प्रसिद्ध ऋषियों में कोई -कोई तान्त्रिक मार्ग के उपासक थे , और कोई -कोई तान्त्रिक उपासना के प्रवर्तक भी थे । ब्रह्मयामल में बहुसंख्यक ऋषियों का नामोल्लेख है , हो शिव -ज्ञान के प्रवर्तक थे ; उनमें उशना , बृहस्पति , दधीचि , सनत्कुमार , नमुलीश आदि उल्लेख्य हैं । जयद्रथयामल के मंगलाष्टक प्रकरण में तन्त्र प्रवर्तक बहुत से ऋषियों के नाम हैं , जैसे दुर्वासा , सनक , विष्णु , कस्प्य , संवर्त , विश्वामित्र , गालव , गौतम , याज्ञवल्क्य , शातातप , आपस्तम्ब , कात्यायन , भृगु आदि ।
१ . क्रोधभट्टारक ‘दुर्वासा ’
सबसे पहले दुर्वासा का नाम उल्लेखनीय है । तान्त्रिक साहित्य में ‘क्रोध भट्टारक ’ नाम से इनका परिचय मिलता हैं । प्रसिद्धि के अनुसार इन्होंने श्रीकृष्ण को ६४ अद्वैतागमों को पढाया था । यह भी किंवदन्ती है कि कलियुग में दुर्वासा द्वारा ही आगम प्रकाश में लाय गये । नेपाल दरबार के ग्रन्थागार में सुरक्षित महिम्नः स्तोत्र की एक पोथी में इनके सम्बन्ध में लिखा है - ‘सर्वासामुपनिषदां दुर्वासा जयति देशिकाः प्रथमः ’ । जयद्रथयामल नामक आगम है अनुसार भी तन्त्र के प्रवर्तक ऋषियों में दुर्वासा का नाम ब्रह्मयामलानुसारी सभी तन्त्रों के भीतर दुर्वासा -मत प्रथम है । यह बात दरबार ग्रन्थागार में उपलब्ध पिंगलागम में पिंगला -मत के प्रसंग में उल्लिखित है । अर्धचन्द्रकला विद्याओं के भीतर भी दुर्वासा का मत उल्लेखनीय है । चन्द्रकला (श्री ) विद्याएँ कौल तथा सोम (कापालिक ) मतों की संमिश्रम हैं । प्राचीन काल में इन विद्याओं में चारों वर्णो का अधिकार था , किन्तु विशेष यह था त्रैवार्णिक लो दक्षिण -मार्ग से अनुष्ठान करते थे और अन्य लोग वाम -मार्ग से ।
दुर्वासा श्रीमाता के उपासक थे । श्रीमाता के द्वादशविध उपासकों में उनका भी एक नाम है । सुनने में आता है उनकी उपास्य षडक्षरी विद्या थी । किसी -किसी के मत में ये त्रयोदशाक्षरी विद्या के उपासक थे । सौन्दर्य -लहरी की टीका में कैवल्याश्रम ने इस विद्या का कादि मत के अनुसार उद्धार भी किया है । इतने बाद भी दुर्वासा का सम्प्रदाय इस समय लुप्तप्राय ही है ।
निम्नलिखित ग्रन्थों में दुर्वासा की चर्चा है ---
१ . त्रिपुर -सुन्दरी (देवी ) - महिम्नःस्तोत्र -टीका में नित्यानन्द नाथ ने कहा है -
सकलागमाचार्यचक्रवती साक्षात् शिव एव अनसूयागर्भसस्भूतः क्रोधभट्टारका -ख्यो दुर्वासा महामुनिः ।
२ . ललितास्तव -रत्न ।
३ . परशिव -महिम्नः स्तोत्र अथवा परशम्भु -स्तुति।
इस प्रकार दुर्वासा श्रीविद्या तथा परमशिव के उपासक थे । कालीसुधानिधि ग्रन्थ से यह पता चलता है कि ये काली के भी उपासक थे ।
२ . अगस्त्य ऋषि
प्रसंगवश इस समय अगस्त्य के सम्बन्ध में कुछ कहा जा रहा है । यह वैदिक ऋषि थे । इनके सम्बन्ध में पाञ्चरात्र तथा शाक्तागमों में भी चर्चा है । इन प्रसिद्ध ऋषि का विवरण पुराण , रामायण महाभारतादि प्रायः सभी प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है । विदर्भराज की कन्या लोपामुद्रा उनकी धर्मपत्नी थीं । उनकी चर्चा भी प्रायः सर्वत्र देखी जाती है , यह भी अगस्त्य के सदृश ही वैदिक ऋषि थीं । रामायण के अरण्यकाण्ड में सुतीक्ष्ण मुनि ने भगवान् को गोदावरी तट -स्थित अगस्त्याश्रम का मार्ग दिखाया था । अगस्त्य ने श्रीरामचन्द्रजी को वैष्णव धनु ब्रह्मदत्त नामक शस्त्र (बाण ), अक्षय तूणीर एवं खड्ग दिया था । विध्र्य पर्वत के साथ अगस्त्य का सम्बन्ध प्रायः सर्वविदित है । दक्षिण दिशा के साथ अगस्त्य का विशेष रुप से सम्बन्ध प्रतीत होता है । यह भी प्रसिद्ध है कि दक्षिण भारतीयों में एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति का भी प्रसार इन्हीं की देन है । ४ अध्यायों और ३०२ सूत्रों का ‘शक्तिसूत्र इन्हीं की रचना है । इसके अतिरिक्त इनके ग्रन्थों में ‘श्रीविद्या -भाष्य ’ भी है ; यह हयग्रीव से प्राप्त ‘पञ्चदशी विद्या ’ की व्याख्या है । अगस्त्य और लोपामुद्रा दोनों ही श्रीविद्या के उपासक थे । प्रसिद्ध है कि ब्रह्मसूत्र पर भी ऋषि अगस्त्य ने एक टीका लिखी थी । किवंदन्ती के अनुसार श्रीपति पण्डित का श्रीकरभाष्य उन्हीं के मतानुसारी हैं । त्रिपुरा -रहस्य के माहात्म्य -खण्ड से पता चलता है कि अगस्त्य उच्च कोटि के वैदिक ऋषि होते हुए भी मेरु -स्थित श्रीमाता के दर्शनार्थ जब उत्सुक हुए तो दर्शन से वे वंचित इसलिए हो गये कि तब तक उन्हें तान्त्रिक दीक्षा प्राप्त नहीं थी , फलतः श्रीमाता के दर्शनोपयोगी विशुद्ध शाक्त देह भी प्राप्त नहीं थी । अन्त में पराशाक्ति की निगूढ उपासना के निमित्त अधिकार -लाभ के लिए देवी -माहात्म्य के श्रवण के अनन्तर उन्होंणे शाक्त -दीक्षा प्राप्त की । उपासना के प्रभाव से पति -पत्नी दोनें ने ही सिद्धि -लाभ किया । बाद में इनकी सिद्धि का इतना महत्त्व स्वीकार किया गया कि इन दोनों ने ही गुरु -मण्डल में उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया । मानसोल्लास के अनुसार श्रीविद्या के मुख्य उपासकों के बीच अग्स्त्य और लोपामुद्रा दोनों का स्थान है ।
३ . दत्तात्रेय
भगवान् दत्तात्रेय भी श्रीविद्या के एक श्रेष्ठ उपासक थे । दुर्वासा के समान ये भी आ सूया गर्भ से समुद्भूत थे । प्रसिद्ध के अनुसार इन्होंने शिष्यों के हितसाधन के लिए श्रीविद्या के उपासनार्थ श्रीदत्त -संहिता नामक एक विशाल ग्रन्थ की रचना की थी । बाद में परशुराम ने उसका अध्ययन करके पचास खण्डों में एक सूत्र ग्रन्थ की रचना की थी । कहा जात है कि इनके बाद शिष्य सुमेधा ने दत्त -संहिता और ‘परशुराम कल्प सूत्र ’ का सारांश लेकर ‘त्रिपुर -रहस्य ’ की रचना की । प्रसिद्धि यह भी है कि दत्तात्रेय ‘महाविद्या महाकालिका ’ के भी उपासक थे ।
४ .नन्दिकेश्वर
शिव -भक्त नन्दिकेश्वर भी श्रीविद्या के उपासक थे । ‘ज्ञानार्ण्वतन्त्र ’ में उनकी उपासित विद्या का उद्धार भी किया गया है । इनका रचित ग्रन्थ ’ है । यह छोटा सा कारिकात्मक ग्रन्थ है । इस पर उपमन्यु की टीका है । नन्दिकेश्वर भी षट्त्रिंशत् -तत्त्ववादी थे । वे परम शिव को तत्त्वातीत और विश्व को ३६ तत्त्वों से बना मानते थे । परन्तु इनके द्वारा तत्त्वों की परिगणना में प्रचलित धारा से कुछ विलक्षणता है । इसमें सांख्य सम्मत पञ्चविंशति तत्त्व तो हैं ही , उसके बाद शिव , शक्ति , ईश्वर , प्राणादि -पञ्चक तथा गुण -त्रय भी माने गये हैं । यहाँ प्रधान और गुण -त्रय पृथक् -पृथक् माने गये हैं । कोई -कोई कहते हैं कि ‘अकारः सर्ववर्णाग्र्यः प्रकाशः परमः शिवः ’ यह कारिका नन्दिकेश्वर की कारिको के अन्तर्गत ही है । किसी -किसी ग्रन्थ में लिखा मिलता है कि दुर्वासा मुनि श्रीनन्दिकेश्वर के ही शिष्य थे । यह भी सुना जाता है कि वीरशैवाचार्य प्रभुदेव के वचनों के कन्नड भाषा के टीकाकार दुर्वासा -सम्प्रदाय के ही अन्तर्गत थे ।
५ . श्रीगौडपाद एवं ६ . श्रीशङ्कराचार्य
ऐतिहासिक युग की तरफ दृष्टिपात करने पर दीखेगा कि भारतवर्ष की संस्कृति के वास्तविक प्रतिनिधित्व में श्रीशङ्कराचार्य , उनके पूर्वगामी या उत्तरवर्तियों के अन्तर्गत भी तान्त्रिक उपासकों की न्यूनता नहीं थी । श्रीशङकर के परमगुरु श्रीगौडपाद तथा गुरुदेव श्रीगोविन्दपाद का स्थान भारतीय दार्शनिक सम्प्रदायों के इतिहास में उच्चतम है । इस सम्बन्ध में यहाँ इस दुर्भेद्य रहस्य का संकेत करना असंगत नहीं होगा कि श्रीशङ्कराचार्य एक ओर तो वैदिक धर्म के संस्थापक थे , दूसरी ओर वही तान्त्रिक साधना के उपदेष्टा एवं प्रचारक भी थे । इस रहस्य का उचित समाधान आगे के गवेषकगण करेंगे । शङ्कराचार्य की उभय पक्षों में प्रसिधियाँ हैं , ऊर्ध्वतम और अधस्तन गुरु -परम्पराओं के आलोचन से प्रतीत के आचार्यों को एक समझते हैं , ऊर्ध्वतम और अधस्तन गुरु -परम्पराओं के आलोचन से प्रतीत होता है कि दोनों ओर आचार्य -परस्परायें प्रायः समान ही हैं । कुछ लोग इन दोनों प्रकार के आचार्यों को एक समझते हैं , दूसरे लोग इसे संभव नहीं मानते ; किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि वैदिक तथा तान्त्रिक मतों का घनिष्ठ सम्बन्ध आरब्ध हो चुका था । गौडपाद महान् वैदान्तिक हैं , उनकी माण्डूक्यकारिका अपूर्व रचना है ; यह एक ओर ब्रह्मपदनिष्ठा तथा दूसरी ओर ज्ञान -निष्ठा का परिचायक है । गौडपाद एक ओर जिस प्रकार माध्यमिक अद्वयवाद में पारंगत थे उसी प्रकार पक्षान्तर में योगाचारों के अद्वयवाद में भी माध्यमिक अद्वयवाद में पारंगत थे उसी प्रकार पक्षान्तर में योगाचारो के अद्वयवाद में भी निष्णात थे । बौद्धदर्शन में बे विशिष्ट रुप में प्रविष्ट थे । शून्यवाद तथा विज्ञाप्तिमात्रतावाद दोनों का हीं उन्हें अच्छा परिचय था । आगम -मत में भी उनका ज्ञान उत्कृष्ट कोटि का था , क्योंकि देवीकालोत्तर का कोई -कोई वचन उनकी कारिकाओं में उपलब्ध होता हैं ’ क्योंकि देवीकालोत्तर का कोई -कोई वचन उनकी कारिकाओं में उपलब्ध होता हैः अवश्य ही इस पर अधिक जोर दिया जा सकता है । वैदिक गौडपाद का यही स्वरुप है ।
आगम की दृष्टी से जान पडता है कि वे समयाचार -सम्मत तान्त्रिक मत के पोषक थे । उनकी ‘सुभगोदय -स्तुति ’ प्राचीन स्तुतियों में प्रधान है । इस बहुत सी टीकायें थीं । प्रसिद्धि के अनुसार इस पर शंकर ने भी टीका लिखी थी । इनकी एक रचना ‘श्रीविद्यारत्नसूत्र ’ है , इस पर भी बहुत सी टीकायें हैं । सुना जाता है कि गौडपाद ने उत्तर -गीता की तरह ही देवीमाहात्म्य की भाष्य -रचना भी की थी । देवी -माहात्म्या की टीका का नाम चिदानन्द्रकमल (?) हैं । इसके लेखक तान्त्रिक नाम से परिचित गौडपाद हैं , यह भी परमहंस परिव्राजकाचार्य और अद्वैत विद्या में निष्णात थे ।
भगवान् शंकराचार्य के विषय में चार प्राचीन ग्रन्थों से कुछ विवरणों का संग्रह किया गया है , जिनके समालोचन से उनके विषय में वैदिकत्त्व , तान्त्रिकत्व आदि आरोपणों का निर्धारण हो सकेगा ।
( १ ) प्रथम ग्रन्थ का नाम श्रीक्रमोत्तम हैं इसका निर्माण - काल प्रायः चार सौ पचास वर्ष पूर्व है । इस ग्रन्थ में शंकर की एक गुरु - परम्परा दी गयी है , उससे पता चलता है कि आदि गुरु शिव से लेकर वशिष्ठ , शक्ति , पराशर , व्यास , शुकदेव , गौडपाद , गोविन्दपाद और शंकर का क्रम है । इसके अनुसार शंकर के शिष्य विश्वदेव थे , उनके बाद बोधघन , ग्रन्थकार मल्लिकार्जुन तक का क्रम है । इस ग्रन्थ का विषय श्रीविद्या है ।
( २ ) द्वितीय ग्रन्थ है --- सुमुखि पूजा - पद्धति । इस ग्रन्थ विषय मातंगीपूजा हैं । यह ग्रन्थ सुन्दरानन्दनाथ के शिष्यं शंकर की रचना है । इस ग्रन्थ में ऊर्ध्वतम शिव से गोविन्दपाद तक का क्रम एक समान दिखाई पडता है , उसके बाद शंकर । परन्तु शंकर के अनन्तर पहले हँ बोधघन और उसके बाद ज्ञानघन ; इस प्रकार परम्परा का क्रम भारती तीर्थ तक अवतीर्ण हुआ है ।
( ३ ) तृतीय ग्रन्थ है --- श्रीविद्यार्णव । यह ग्रन्थ संप्रति प्रसिद्ध है। इससे जान पडता है कि शंकर के १४ शिष्य थे , ५ भिक्षु तथा ९ गृहस्थ।
( ४ ) चौथा ग्रन्थ है --- भुवनेश्वरी - रहस्य । पृथ्वीधर शंकर के शिष्य , गोविन्दपाद के प्रशिष्य और गौडपाद के वृद्धप्रशिष्य थे ।
इन सब के परिशीलन से ज्ञान होता है कि शंकर श्रीविद्या के अतिरिक्त मातंगी और श्रीभुवनेश्वरी के भी उपदेष्टा थे । आशा है , ऐतिहासिक विद्वान् इस विषय में गवेषणा करेंगे ।
एक बात और भी है शंकर को शिष्य कोटि में वेदान्त प्रस्थान के जो आचार्य पदमपाद हैं , जिन्होंने पञ्चपादिका की रचना की थी , क्या उन्होंने ही शंकर कृत प्रपञ्चसार पर टीका भी लिखी थी ? कोई -कोई प्राचीन आचार्य इस पर विश्वास करते हैं , किन्तु वर्तमान पण्डितगण इस पर संशय करते हैं । श्री शंकर की तान्त्रिक रचनाओं में प्रपञ्चसार प्रधान माना जाता है , उसके बाद सौन्दर्य -लहरी प्रभृति को । आनन्द -लहरी की सौभाग्य -वर्धिनी टीका में श्री शंकर कृत एक ‘क्रम -स्तुति ’ की बात मिलती है , जिसमें एक प्रसिद्ध श्लोक है , जिसका तात्पर्य है कि वेद के अनुसार माया -बीज ही भगवती पराशक्ति का नाम है और यही पराशक्ति जगन्माता त्रिपुरा और त्रियोनि -रुपा है । अभिनवगुप्त की परात्रिंशिका में क्रमस्तोत्र की जो बात कही गयी है , वह विचारणीय हैं कि क्या वह शङ्कराचार्य कृत क्रम -स्तोत्र तो नहीं है ?
7…संक्षिप्त विवरण - तान्त्रिक सम्प्रदायों का मार्मिक साम्य
तान्त्रिक सम्प्रदायों का मार्मिक साम्य
तान्त्रिक -संस्कृति में मूलतः साम्य रहने पर भी देश -काल और क्षेत्र -भेद से उसमें विभिन्न सम्प्रदायों का आविर्भाव हुआ है । इस प्रकार का भेद साधकों के प्रकृति -गत भेद के अनुरोध से स्वभावतः ही होता हैं । भावी पीढी के ऐतिहासिक विद्वान् जब भिन्न तान्त्रिक साम्प्रदायों के इतिहास का संकलन करेंगे और गहराई से उसका विश्लेषण करेंगे तो इस निष्कर्ष पर पहुँच सकेंगे कि यद्यपि भिन्न -भिन्न तान्त्रिक सम्प्रदायों में आपाततः वैषम्य प्रतिभासित हो रहा है किन्तु उनमें निगूढ रुप से मार्मिक साम्य है ।
संख्या में तान्त्रिक सम्प्रदाय कितने आविर्भूत हुए और पश्चात् -काल में कितने विलुप्त हुए यह कहना कठिन है । उपास्य -भेद के कारण उपासना -प्रक्रियाओं में भेद तथा आचारादि -भेद होते है , साधारनतया पार्थक्य का यही कारण हैं। १ .शैव , २ . शाक्त , ३ . गाणपत्य ये तो सर्वत्र ही प्रसिद्ध हैं । इन सम्प्रदायों के भी अनेकानेक अवान्तर भेद हैं । शैव तथा शैव -शाक्त -मिश्र सम्प्रदायों में कुछ के निम्नलिखित उल्लेखनीय नाम हैं -सिद्धान्त शैव , वीरशैव , अथवा जंगम शैव , रौद्र , पाशुपत , कापालिक अथवा सोम , वाम , भैरव आदि। अद्वैतदृष्टि से शैवसम्प्रदाय में त्रिक अथवा प्रत्यभिज्ञा , स्पन्द प्रभृति विभाग हैं । अद्वैत -मत में भी शक्ति की प्रधानता मानने पर स्पन्द , महार्थ , क्रम इत्यादि भेद अनुभूत होते हैं । दश शिवागम और अष्टादश रुद्रागम तो सर्वप्रसिद्ध ही हैं । इनमें भी परस्पर किंचित् -किंचित् भेद नहीं है यह नहीं कहा जा सकता । द्वैत -मत में कोई कट्टर द्वैत , कोई द्वैतद्वैत और कोई शुद्धाद्वैतवादी है । इनमें किसी सम्प्रदाय को भेदवादी , किसी को शिव -साम्यवादी और किसी को शिखा -संक्रान्तिवादी कहते हैं । काश्मीर का त्रिक या शिवद्वैतवाद अद्वैतस्वरुप से आविष्ट से आविष्ट है । शाक्तों में उत्तरकौल प्रभृति भी ऐसे ही हैं ।
किसी समय भारतवर्ष में पाशुपत संस्कृति का व्यापक विस्तार हुआ था । न्यानवर्तिककार उद्योतकर संभवतः पाशुपत रहे और न्यायभूषणकार भासर्वज्ञ तो पाशुपत थे ही । इनकी बनाई गण -कारिका आकार में यद्यपि छोटी है किन्तु पाशुपतदर्शन के विशिष्ट ग्रन्थों में इसकी गणना है ।
लकुलीश पाशुपत की भी बात सुनने में आती है । यह पाशुपतदर्शन पञ्चार्थवाद -दर्शन तथा पञ्चार्थलाकुलाम्नाय नाम से विख्यात था । प्राचीन पाशुपत सूत्रों पर राशीकर का भाष्य था , वर्तमान समय में दक्षिण से इस पर कौण्डिन्य -भाष्य का प्रकाशन हुआ है । लाकुल -मत वास्तव में अत्युन्त प्राचीन है , सुप्रभेद और स्वयम्भू आगमों में लाकुलागमों का उल्लेख दिखाई देता है ।
महाव्रत -सम्प्रदाय कापालिक -सम्प्रदाय का ही नामान्तर प्रतीत होता है । यामुन मुनि के आगम प्रामाण्य , शिवपुराण तथा आगमपुराण में विभिन्न तान्त्रिक सम्प्रदायों के भेद दिखाय गये हैं । वाचस्पति मिश्र ने चार माहेश्वर सम्प्रदायों के नाम लिये हैं । यह प्रतीत होता है कि श्रीहर्ष ने नैषध (१० ,८८ ) में समसिद्धान्त नाम से जिसका उल्लिखित है , वह कापालिक सम्प्रदाय ही है ।
कपालिक नाम के उदय का कारण नर -कपाल धारण करना बताय जाता है । वस्तुतः यह भी बहिरंग मत ही है । इसका अन्तरंग रहस्य प्रबोध -चन्द्रोदय की प्रकाश नाम की टीका में प्रकट किया गया है । तदनुसार इस सम्प्रदाय के साधक कपालस्थ अर्थात् ब्रह्मारन्ध्र उपलक्षित नरकपालस्थ अमृत या चान्द्रीपान करते थे । इस प्रकार के नामकरण का यही रहस्य है । इन लोगों की धारणा के अनुसार यह अमृतपान है , इसी से लोग महाव्रत की समाप्ति करते थे , यही व्रतपारणा थी । बौद्ध आचार्य हरिवर्मा और असंग के समय में भी कापालिकों के सम्प्रदाय विद्यमान थे । सरबरतन्त्र में १२ कापालिक गुरुओं और उनके १२ शिष्यों के नाम सहित वर्णन मिलते हैं । गुरुओं के नाम हैं -- आदिनाथ , अनादि , काल , अमिताभ , कराल , विकराल आदि । शिष्यों के नाम हैं --नागार्जुन , जडभरत , हरिश्चन्द्र , चर्पट आदि। ये सब शिष्य तन्त्र के प्रवर्तक रहे हैं । पुराणादि में कापालिक मत के प्रवर्तक धनद या कुबेर का उल्लेख है ।
कालामुख तथा भट्ट नाम से भी सम्प्रदाय मिलते हैं , किन्तु इनका विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है । प्राचीन काल में शाक्तों में भी समयाचार और कौलाचार का भेद विद्यमान था । कुछ लोग समझते हैं कि समयाचार वैदिक मार्ग का सहवर्ती था और गौडपाद , शंकर प्रभृति समयाचार के ही उपासक थे ।
कौलाचारसंप्रद्राय में कौलों के भीतर भी पूर्व कौल और उत्तर कौल का भेद विद्यमान था । पूर्व कौल मत शिव एवं शक्ति , आनन्द -भैरव और आनन्द -भैरवी से परिचित है । इस मत में दोनों के मध्य शेष -शेषिभाव माना जाता था , किन्तु उत्तर कौल के अनुसार शेष -शेषिभाव नहीं हैं । इस मत में सदा शक्ति का ही प्राधान्य स्वीकृत है , शक्ति कभी शेष होती है , शिव तत्त्व रुप में परिणत हो जाते हैम और शक्ति तत्त्वातीत ही रहती है । रुद्रयामल के उत्तरतन्त्र ’ होने का यही रहस्य हैं - पूर्व कौल शिव और शक्ति के मध्य शेष -शेषिभाव मानते हैं । अतः पूर्व कौल के मत में शेष -शेषिभाव पूर्वतन्त्र का परिचायक होना चाहिए । जब शक्ति कार्यात्मक समग्र प्रपञ्च को अपने में आरोपित करती है तो उसका नाम होता है - कारण , और उसका पारिभाषिक नाम आधार कुण्डलिनी है । कुण्डलिनी के जागरण से शक्ति शेष नहीं रहती । तत्त्व रुप में सदाशिव परिणत हो जाते हैं और शक्ति तत्त्वातीत ही रहती है । यही उत्तरतन्त्र का उत्तरत्व है ।
कौल मत की आलोचना
प्राचीन समय से ही कौल -मत की आलोचना हो रही है । कौल मत में ही मानवीय चरम उत्कर्ष की अवधि स्वीकृत होती है । इन लोगों का कहना है कि तपस्या , मन्त्र -साधना प्रभृति से चित्तशुद्धि होने पर ही कौल -ज्ञान धारण करने की मनुष्य में योग्यता आता है । योगिनीह्रदय की सेतुबन्धटीका (पृ०२५ ) में कहा है ---
पुराकृततपोदानयज्ञतीर्थजपव्रतैः ।
शुद्धचित्तस्य शान्तस्य धर्मिणो गुरुसेविनः ॥
अतिगुप्तस्य भक्तस्य कौलज्ञानं प्रकाशते ।
विज्ञान -भैरव की टीका में क्षेमराज ने कहा है ---
वेदादिभ्यः परं शैवं शैवात् वामं तु दक्षिणम् ।
दक्षिणात् परतः कौलं कौलात् परतरं नहि ॥
किन्तु शुभागमपञ्चक के अन्तर्गत सनत्कुमारसंहिता में कौल -ज्ञान की निन्दा की गयी है । १ . कौलक , २ . क्षपणक , ३ . दिगम्बर , ४ . वामक आदि के सम्प्रदाय बराबर माने गये हैं ।
शक्तिसंगमतन्त्र के विभिन्न खण्डों में विभिन्न तान्त्रिक सम्प्रदायों के यत्किञ्चित् विवरण मिलते हैं । बौद्ध तथा तन्त्रों के विषय में भी बहुत कुछ कहना था , किन्तु यहाँ संभव नहीं होगा और रुद्रयामल के प्रसंग में असंगत भी है । यद्यपि बुद्ध की चर्चा रुद्रयामल के १७ वें अध्याय में आयी है ।
8…संक्षिप्त विवरण - बृहत्तर भारत में तान्त्रिक सम्प्रदाय
बृहत्तर भारत में तान्त्रिक सम्प्रदाय
बृहत्तर भारत में किसी समय में भारतवर्ष के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्तों तक और देश से बाहर भी तन्त्रों का व्यापक विस्तार हुआ था । तन्त्रों में कादि और हादि मत ५६ प्रदेशों में प्रचलित थे । इन दोनों मतों की स्थानसूचिओं को परस्पर मिलाने पर पता चलता है कि किसी -किसी प्रदेश में कादि -हादि दोनों मत प्रचलित थे । ये सब देश भारतवर्ष के चारों ओर और मध्यभाग में अवस्थित हैं यथा --(१ ) पूर्व में अंग , वंग , कलिंग , विदेह , कामरुप , उत्कल , मगध , गौड , सिलहट्ट , कैकट आदि ; (२ ) दक्षिण में -- केरल , द्रविण , तैल ~उ , मलयाद्रि , चोल , सिंहल , आदि ; (३ ) पश्चिम में -सौराष्ट्र , आभीर , कोंकण , लाट , मत्स्य , सैन्धव , आदि ; (४ ) उत्तर में -काश्मीर , शौरसेन , किरात , कोशल आदि ; (५ ) मध्य में - महाराष्ट्र विदर्भ , मालव , आवन्तक आदि। (६ ) भारत के बाहर हैं - वाहलीक , कम्बोज , भोट , चीन , महाचीन , नेपाल , हूण , कैकय , मद्र , यवन आदि।
कादि या हादि दोनों मतों में नाना प्रकार के अवान्तर विभाग भी थे ।
तन्त्र -विस्तार का जो यत्किञ्चित् परिचय दिया गया है , उससे ज्ञात होता है कि भारतवर्ष के प्रायः सभी क्षेत्रों में वैदिक -संस्कृति के समानान्तर तान्त्रिक संस्कृति का विस्तार भी था । कभी - कभी इसकी स्वतन्त्र पृथक् सत्ता थी । कभी तटस्थ रुप में और कभी अंगीभूत रुप में । कभी - कभी तो प्रतिकूल रुप में भी इस संस्कृति का प्रचार हुआ । किन्तु सदा और सर्वत्र यह भारतीय संस्कृति के अंश में ही परिगणित होता था । भारतवर्ष के बाहर पूर्व तत्था पश्चिम में भारतीय संस्कृति का प्रभाव फैला हुआ था । वह केवल बौद्ध संस्कृति के स्त्रोत से ही नहीं , ब्राह्मण्य -संस्कृति की धाराअं से भी । प्रायः १२सौ वर्ष पूर्व जयवर्मा द्वितीय के राज्य काल में कम्बोज अथवा कम्बोडिया में भारतवर्ष से तन्त्र -ग्रन्थ पहुँचे थे । ये तन्त्र बौद्ध -तन्त्र नहीं थे , अपितु ब्राह्मण -तन्त्र थे , इन्हें शिवागम कहा जा सकता है । इन ग्रन्थों के नाम हैं --- (१ ) नयोत्तर (२ ) शिरश्च्छेद (३ ) विनय -शीख और (४ ) सम्मोह । ऐतिहासिकों ने प्रमाणित किया है कि नयोत्तर संभवतः निःश्वास -संहिता के अन्तर्गय ‘नय ’ है और उत्तर सूत्र के साथ अभिन्न है । अष्टम शतक का लिखा निःश्वासतत्त्वसंहिता गुप्त लिपि में दरबार पुस्तकालय नेपाल में अभी भी उपलब्ध है । ये ग्रन्थ प्रायः षष्ठ या सप्तम शतक के माने जाते हैं । प्रतीत होता है कि शिरश्छेद -तन्त्र जयद्रथयामल का ही नामान्तर है । जयद्रथयामल की एक प्रति नेपाल दरबार पुस्तकालय में है । विनयशीख को कोई कोई जयद्रथयामल का परिशिष्ट मानते हैं । सम्मोहन -तन्त्र भी प्रकार से परिशिष्ट ही माना जाता है । यह प्रचलित सम्मोहन -तन्त्र का प्राचीन रुप है ।
जैसे भारत तन्त्र या तान्त्रिक -संस्कृति के बाहर जाने बात कही गयी है , इसी प्रकार बाहर से भी किन्हीं तन्त्रों का भारत में आने विवरण सुना जाता है । इस विषय में कुब्जिका -तन्त्र का नाम लिया जा सकता है । वशिष्ठ के उपाख्यान के प्रसंग में चीन अथवा महाचीन से भारत में उपासक -क्रम के आने की किंवदन्ती सुनी जाती है । तारा , एकजटा तथा नीलसरस्वती से अभिन्न है । तारातन्त्र नामक ग्रन्थ में संक्षिप्त विवरण निर्दिष्ट है ।
पहले जो बात कम्बोज के विषय में कही गयी है , वह केवल कम्बोज ही नहीं , निकटवर्ती देशोम में भी लागू है । देवराज नाम से शिव की उपासना तथा विभिन्न प्रकार की शक्तियों की उपासना भारतवर्ष से बाहर जाकर प्रचलित हुई । इन देव -देवियों के नाम हैं - भगवती , महादेवी , उमा , पार्वती , महाकाली , महिषमर्दिनी , पाशुपत भैरव आदि -आदि । चीनी भाषा में लिखित प्राचीन इतिहासों से इसका पूर्ण विवरण जाना जा सकता है । इस दिशा आन्ध्र हिस्टारिकल सोसाईटी थोडा - बहुत कार्य कर रही है ।
अब कुछ तन्त्र -पीठ , विद्या -पीठ , मन्त्र -पीठ आदि के सम्बन्ध में भी विवेचन करना चाहिए । १ कामकोटि , २ .जालन्धर , ३पूर्णगिरि तथा . ४ .उड्डियान इन चतुष्पीठों के सम्बन्ध मे कुछ परिचय लोगों को ज्ञात है । कामह्रद के साथ मत्स्येन्द्रनाथ का सम्बन्ध था , जालन्धर -पीठ के साथ अभिनवगुप्त के गुरु शम्भुनाथ का सम्बन्ध था , जो आजकाल ज्योतिर्लिङ का स्थान माना जाता है । ये सभी प्राचीनकाल में विद्या -क्रेन्द्र कि स्वयं नागार्जुन भी अन्तिम समय में यही तिरोहित हुए। विभिन्न तान्त्रिक विद्याओं की साधन , उसका प्रत्यक्षीकरण तथा योग्य आधार में अर्पण इन सभी पीठों में होता था । परवर्तीकाल में बौद्ध लोगों दे द्वारा नालन्दा , विक्रमशील , उदन्तपुरी प्रभृति स्थानों में इन प्राचीन पीठों का अनुवर्तन किया गया । तक्षशिला का नाम तो सर्वत्र प्रसिद्ध ही है । सम्पूर्ण भारत देश में ४९ या ५० पीठ हैं जिनका विस्तार से विवरण तन्त्र -शास्त्रों में उपलब्ध होता है । इस विषय पर डा०डी०सी सरकार ने कुछ आलोचना की है । पीठ -तत्त्व का रहस्य अति गम्भीर है । वास्तव में पीठ का तात्पर्य है ---वह स्थान है जहाँ शक्ति जागृत हैं और जहाँ मन , बुद्धि , चित्त , अहंकार आदि का विषय अलिङु परमतत्त्व ज्योति रुप है ।
देह में भी चतुष्पीठ माने जाते है , अम्बिका और शान्ता शक्तियों का सामरस्य जहाँ है , वह प्रधान पीठ है , वहाँ अलिङु अव्यक्त महाप्रकाश परम ज्योति रुप से अभिव्यक्त होता है । इस पीठ का पारिभाषिक नाम है --परावाक् । इसी प्रकार जहाँ इच्छा , ज्ञान , क्रिया तथा वामा ज्येष्ठा एवं रौद्री शक्तियों का सामरस्य हुआ है , अस्तु , रहस्य -विस्तार यहाँ अनावश्यक है ।
अब तक जो कुछ कहा गया है , वह तान्त्रिक -संस्कृति के बाह्य -अंगो की एक लघु चित्र -छाया है , मात्र विहङावलोकन है , किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि संस्कृति का महत्त्व उसके बाह्य अवयवों के चयन तथा आडम्बरों पर निर्भर नहीं है । संस्कृति के महत्त्व का परिचायक है ---मानव आत्मा की महनीयतां का आदर्श -प्रदर्शन । जिस संस्कृति में आत्मा का स्वरुप -स्वातन्त्र्य और सामर्थ्य की अतिशयता जितनी अधिक व्यक्त हुई , उस संस्कृति का गौरव उतना अधिक मानना होगा । वैदिक संस्कृति के प्रतिनिधि के रुप में आर्य ऋषियों ने यह गाया था ---
श्रृन्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ (ऋ० १० .१३ .१ )
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् , आदित्यवर्ण तमसः परस्तात् ॥ (वाज०३१ .१८ )
मानव आत्मा ही वह महान् आदित्यवर्ण पुरुष है , जो ज्ञान -भेद या अपरोक्षानुभव कर अतिमृत्यु -अवस्था का लाभ करता है ।
तान्त्रिक -संस्कृति का निर्णय भी इसी मान -दण्ड से करना होगा । आत्मा का स्वरुप -गत और सामर्थ्य -गत पूर्णता का आदर्श ही इसके महत्त्व को प्रकट करता है । आगम शास्त्रों में इसका स्पष्ट निर्देश है कि यद्यपि आत्मा स्वरुपतः नित्यशुद्ध है , किन्तु उसकी अप्रबुद्ध अवस्था श्रेष्ठ है । अप्रबुद्ध अवस्था के चित् स्वरुप होने पर भी चेतन न होने के कारण वह अचित् कल्प ही है । विमर्शहीन चित् या प्रकाश चित् होने पर भी अचित् के ही सदृश है , प्रकाश होने पर अप्रकाशवत् , शिव होने पर भी शववत् है । इसीलिए भर्तृहरि ने कहा है ---
वागरुपता चेदुत्क्रामेत् अवबोधस्य शाश्वती ।
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी ॥
( वाक्यपदीय १ . १२४ )
इसीलिए आणव -मल को आदि मल माना जाता है और उसके अपनयन न होने से चित्स्वरुप अवस्था को शिवत्व -हीन पशु -कल्प अवस्था कहते हैं । उस समय आत्मा साञ्जन न होते हुए भी निरञ्जन पशुमात्र है ।
इसी आधार पर तान्त्रिक -संस्कृति की उदात्त घोषणा यह है कि मनुष्य के सुप्त रहने से काम नहीं चलेगा , उसे जागना चाहिए ---
प्रबुद्धः सर्वदा तिष्ठेत् ।
मानव -जीवन का लक्ष्य जिस पूर्णत्व को माना जाता है , उसकी उपलब्धि के लिए सबसे पहले आवश्यक है ---अनादि निद्रा से जागना अर्थात् प्रबोधन , उसके बाद आत्मा की क्रमिक ऊर्ध्व -गति मार्ग से परम शिव या परा संवित् या परा सत्ता का साक्षात्कार करना और यही रुद्रयामल का उद्देश्य है ।
9…संक्षिप्त विवरण - योग और आत्मसाक्षात्कार
योग और आत्मसाक्षात्कार
मनुष्य को जागना होगा , यह पहली बात है , किन्तु यह अत्यन्त कठिन व्यापार है । साधारण दृष्टि से जितनी आत्माओं की ओर दृष्टी जाती है तो देखते है वे सभी सुप्त हैं ,निद्रा में डुबे है । चाहे वे कर्मरत हों , ज्ञानी हों , चाहे किसी अन्य ही भूमि के हों , किन्तु उनमें अधिकांशतः आत्म -विमर्श नहीं है । मानव आत्मा जब अपनी विशुद्ध स्थिति में अवस्थित रहता है , तो वह अनवच्छिन्न चैतन्य शिव से अभिन्न रहता हैं ।
अशुद्ध अवस्था में चैतन्य का अवच्छेद रहता है , इसीलिए उस समय वह ग्राहक रुप में अर्थात् परिमित ‘अहम् ’ के रुप में खण्ड प्रमाता बनकर अभिव्यक्त होता है । खण्ड प्रमाता के समक्ष अन्य सब प्रमेय एवं ग्राह्य रुप में प्रतीत होते हैं । ग्राहक आत्मा अपने से पृथक ग्राह्य -सत्ता को इदं रुपेण देखता है । चैतन्य को अवच्छिन्नता की प्रतीति ग्राह्य की ओर आत्मा की उन्मुखता से होती है । पिण्ड -विशेष से सम्बन्ध रहने के कारण दूसरे के साथ अहन्ता य अभिमन अपूर्ण है । परन्तु की अवस्था में अनाश्रित शिव से लेकर पृथ्वी पर्यन्त ३६ तत्त्वात्मक समग्र विश्व ही उनका रुप या शरीर बन जाता है । अपूर्ण अहं को पूर्णत का लाभ मिलना चाहिए , यही आत्मा का परम जागरण है , इसे परम लक्ष्य के रुप में अद्वैत साधना ही संकेत करती है ।
अनवच्छिन्न चैतन्य में नियत विशेष रुपों का भान नहीं होता । यदि हो , तब उस अवस्था को अनवाच्छिन्न न मानकर उसे ग्राहक कोटि में ही निविष्ट करना चाहिए । पूर्णत्व का भान होता है - अखण्ड सामान्य -सत्ता के रुप से । इस सामान्यत्मक महासत्ता का भान सविशेष और निर्विशेष उभय रुप से हो सकता है । सर्वातीत रिक्त -रुप ‘भा ’ मात्र है और पूर्ण -रुप सर्वात्मक ‘भा ’ है । ‘भा ’ स्वरुपता उभयत्र ही विद्यमान है । इस सामान्य -सत्ता का भान ही ‘स्वभाव ’ शब्द से बोधित होता है । वस्तुतः यह बहु के भीतर एक का अनुसन्धान है । ग्राहक आत्मा को पहले जो प्रतिनियत दर्शन होता था , वह इस अवस्था में कट जाता हैं , निवृत्त हो जाता है । इस प्रकार क्रमशः अनवच्छिन्न चैतन्य की ओर प्रगति होती जाती है ।
आत्मा जब तक सुप्त रहता है , अर्थात् जब तक कुण्डलिनी प्रबुद्ध -शक्ति नहीं बनती , तब तक उसका स्तर -भेद स्वाभविक रुप से बना रहता है । उस समय उसकी अस्मिता योग्यता के तारतम्यानुसार देह , प्राण , इन्द्रिय अथवा शून्य या मा में क्रिया करती रहती है । यह स्मरण रखना चाहिए कि यह अस्मि -भाव वास्तविक संवित् का है , ग्राहक का नहीं है। पदों की बहुत संख्या है , इसका विस्तार -क्षेत्र भी अनाश्रित से लेकर पृथ्वी पर्यन्त है । किन्तु ये किसी पद के धर्म नहीं है , प्रत्युत चिति के धर्म हैं । किसी भी पद में उसकी धारना हो सकती है , धारणा का अभिप्राय है --दृढ अभिनिवेश । इसके प्रभा के कारण इच्छा -मात्र से क्रियान्त उद्भव हो सकता है ।
शुद्ध आत्मा का अस्मिता -जन्य जो अभिनिवेश है , वह शुद्ध अवस्था में विश्व में सर्वत्र विद्यमान है , क्योंकि शुद्ध आत्मा ग्राहक नहीं है यह पहले ही कहा गया है । बिन्दु से देह पर्यन्त विभिन्न स्थितियों में यह सर्वत्र ही व्यापक है , किन्तु व्याप्त रहने पर भी सर्वत्र ही विकास नही है , क्योंकि वह भावना -सापेक्ष है । जिसको कर्तृत्व , ईश्वर या स्वातंत्र्य कहा जाता है , वह अहन्ता का विकास छोडकर अन्य कुछ नहीं है । इसे ही तान्त्रिक सिद्ध गण चित्स्वरुपता कहते हैं । जितने प्रकार की सिद्धियाँ हैं , वे सब अहन्ता से ही अनुप्राणित हैं ।
तान्त्रिक -योग या ज्ञान -साधना का लक्ष्य सुप्त आत्मा को जागृत करना है । जिन आत्माओं से हम लोग परिचित हैं , वे प्रायः सुप्त हैं , क्योंकि इनकी दृष्टी से चिद् अचित् परस्पर विलक्षण हैं । सुप्त आत्मा की दृष्टि से ग्राहक चिद्रूप है और ग्राह्य अचिद्रूप । समग्र विश्व अखण्ड प्रकाश लोक है और आत्मा के ही अन्तः स्थित है । फिर भी सुप्त आत्माएँ उन्हे अपने बाहर समझती हैं । यह सुप्त आत्मा ही संसारी आत्मा है जिससे हम लोग परिचित है ।
आत्मा की सुप्ति भंग होने के साथ -साथ इस स्थिति में भी परिवर्तन होने लगता है , और यह शुद्ध विद्या के प्रभाव से होता है । इन आत्माओं की तात्कालिक अवस्था को ठीक -ठीक न सुप्ति और न जागरण ही कहा जाता है । यह अवस्था दोनों के बीच की कही जा सकती है । उस समय सुप्तिजनित -भेद की प्रतीति रहती है , किन्तु जागरण का अभेद भी प्रतीत होता रहता है । इन लोगों का संसार नहीं रहता , किन्तु संसार का संस्कार रह जाता है । इन लोगों की स्थिति न भव की और न उद्भव की कही जा सकती है , किसी अंश में यह पातञ्जल दर्शन के संप्रज्ञात समाधि के अनुरुप है , क्योंकि उस दशा में अविवेक रह जाता है । इसके बाद शुद्ध चित् का प्रकाश होता है , जो किसी अंश में पातञ्जल मार्ग के विवेकख्याति के सदृश है । यह स्वप्नवत् अवस्था है , न ठीक सुप्ति है और न ठीक जाग्रत् । इसीलिए एसे ठीक -ठीक प्रबुद्ध अवस्था नही कहा जा सकता । यहाँ यह स्मरण अवश्य रखना चाहिए कि इस अवस्था में कर्म -क्षय सिद्ध हो चुका है । इसलिए एक दृष्टि से इन आत्माओं को मुक्त भी किया जा सकता हैं । फिर भी तान्त्रिक दृष्टी से इन्हें मुक्त नहीं कहा जा सकता । तान्त्रिक परिभाषा में ये आत्माएँ रुद्राणु नाम से अभिहित होती हैं और पशु कोटि में गिनी जाती है । हाँ , ये आत्माएँ अवश्य ही सवित् मार्ग के सिद्धान्त -ग्रहण का अधिकार प्राप्त कर लेती हैं ।
इसके बाद ही यथार्थ जागरण की सूचना मिलती है । उस समय प्रमाता वस्तुतः प्रबुद्ध हो जाता है , इसमें भेद दृष्टी नहीं रहती , किन्तु साथ -साथ भेद और अभेद दोनों कें संस्कार रहते है । इस अवस्था में भी इंदरुपेण जडावस्था की प्रतीति रहती हैं । ये सभी आत्माएँ समग्र जगत् को अपने शरीर के सदृश अनुभव करती हैं । किसी प्रकार यह अवस्था ईश्वर के अनुरुप है , इसके भीतर अधिकाधिक वैचित्र्य है जो स्वानुभव -संवेद्य है ।
इसके बाद जागरण और भी स्पष्टरुप से होता है । उस समय प्रबुद्ध ‘भा की वृद्धी होती है और उसके प्रभाव से इंद -प्रतीति -वेद्य -प्रमेय अहं -रुप -आत्मस्वरुप में निमग्न होकर निमिषवत् प्रतीत होता है । इतना होने पर भी यह सुप्रबुद्ध अवस्था नहीं है ; यद्यपि प्रबुद्ध अवस्था से उत्कृष्ट अवश्य है । तान्त्रिक योगी गण इन आत्माओं को उद्भवी नाम से आख्यात करते है । ये सभी आत्माएँ अभेद -प्रतिपत्ति अथवा कैवल्य -प्राप्ति के द्वारा अहमात्मक -स्वरुप में निमग्न रहती हैं , यहाँ भी इदन्ता रहती है , किन्तु वह अहन्ता से आच्छादित रहने के कारण अस्फुट रहती है । इस अवस्था को किसी अंश में सदाशिव के अनुरुप माना जा सकता है । किन्तु यह भी पूर्णत्व नहीं है ।
10……संक्षिप्त विवरण - उन्मेष एवं निमेषावस्था
उन्मेष एवं निमेषावस्था
इतने बडे दीर्घमार्ग के अतिक्रमण करने पर वास्तव -पूर्णता का उदय होता है , किन्तु उदय -मात्र होता है , उसका स्तायित्व नहीं रहता ; क्योंकि उस समय भी उन्मेष निमेष का व्यापार चलता रहता है । इस व्यापार के प्रभाव से स्थिति रहती है ईश्वर के सदृश । उस समय उन्मेष विद्यमान रहता है , और किसी समय उसकी स्थिति रहती है सदाशिव के सदृश , जब उसमें निमेष विद्यमान रहता है । इन दोनों ही अवस्थाओं में सभी समय महाप्रकाश अनावृत रहता है । शिवादि -धरान्त विश्व का भान कभी रहता हैं , कभी नहीं रहता । जब विश्व का भान रहता है , तब प्रकाशात्मक रुप से ही उन्मेष रहता हैं और जब नहीं रहता तब प्रकाशात्मक रुप से ही निमेष रहता है , इसके बाद पूर्णता को स्थायित्व प्राप्त होता हैं।
उन्मनी अवस्था --- वस्तुतः पूर्णत्व का स्फुरण बताया गया है। वह पूर्णत्व होते हुए भी स्थायी नहीं हो सका , क्योंकि उसके साथ मन का सम्बन्ध था । मन के रहने के समय उसके सम्बन्धे से उन्म्ष होता है और मन के निमग्न हो जाने पर मन का सम्बन्ध न रहने से निमेष रहता हैं । मन के रहने के कारण ही उन्मेष या निमेष की संभावन बनी हुई थी । उसके बाद मन भी उत्क्रान्त हो जाता हैं इस अवस्था में उन्मनी अवस्था का आविर्भाव हो जाता है , और उसके प्रभाव से पूर्णत्व सिद्ध हो जाता है । इसे ही आगमवित् सुपबुद्ध अवस्था के रुप के रुप में गणना करत हैं । इस अवस्था में आत्मा का जागरण पूर्ण हुआ यह कहा जा सकता है । इस समय इच्छामात्र विभूति की सिद्धि या आविर्भाव होता है ।
सिद्धि के रहस्य के संबंध में भी कुछ विवेचन करना चाहिए । यह स्मरण रखना होगा कि तत्त्व और अर्थ दोनों में किसी एक का आश्रय करके ही सिद्धि का उदय हो सकता हैं । जागतिक दृष्टि से जाग्रत् के प्रत्येक पदार्थ का कोई विशिष्ट क्रियाकारित्व है , योगी गण संयम के द्वारा तत्तद् अर्थो से भिन्न -भिन्न कर्म संपादन कर सकते हैं ।
तत्त्वमूलक सिद्धि के दो प्रकार हैं १ .परा तथा २ . अपरा । पातञ्जल योग में भी तत्त्व -त्रय के आधार पर सिद्धियों का विवरण मिलता है । अर्थ विशेष में आत्म -भावना करके योगी तद्रूप होते है और उस कार्य का संपादन करते हैं । जो देवता जिस अर्थ का संपादन करता है योगी उस देवभाव में अहंभाव करके उस अर्थ का संपादन उस देवता से कर लेता है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी तत्त्व में अहन्ता का अभिनिवेश करने पर तदनुरुप सिद्धि का उदय हो सकता है । माया पर्यन्त ३१ तत्त्वों का अवलम्बन करके इसी प्रकार की सिद्धियाँ की जाती हैं । इन सिद्धियों का नामान्तर गुन्हा -सिद्धि है , ‘गुहा ’ माया का ही पर्याय है । मायातीत शुद्ध विद्या अथवा सरस्वती का आश्रय करके जिन सिद्धियों का उदय होता है उनका नाम तत्त्वमूलक परा -सिद्धि है । लौकिक कार्यो की सिद्धि के लिए अपरा -सिद्धियाँ की जाती हैं ।
ये परा एव्म सिद्धियाँ खण्ड सिद्धियाँ ही हैं । महासिद्धि नहीं । महासिद्धि इनसे भी उत्कृष्ट है । ये दो प्रकार की है - एक सकलीकरण और अन्तिम महासिद्धि जिससे शिवत्व लाभ करते हैं । उसके बाद ही आती है शान्त स्निग्ध शीतलता । जिस समय कालाग्नि योगी के देह में अवस्थित सभी पाशों को दग्ध करता है , उस समय षडध्वजा का दाह हो जाता है । उसी अवस्था में भीषण ताप का अनुभव होता है । योगी अपने शरीर में इस ताप का अनुभव करता है । इसके बाद स्निग्ध अमृत रस से मानों योगी की सकल सत्ता आप्लावित हो जाती है । इसी समय योगी पूर्णतया इष्टदेवता का साक्षात्कार लाभ करते है । उस समय योगी शोधित अध्वा या समग्र विश्व का अनुग्राहक बन जाता है , यह जो अमृत -प्लावन है इसी का नाम ‘पूर्णाभिषेक ’ है । योगी इस अवस्था में प्रतिष्ठित होकर जगद -गुरु पद में अधिष्ठित होते हैं । इस प्रकार का पूर्णत्व प्राप्त करने पर भी उसे भी अतिक्रम करके उठना पडता है क्योंकि यह अपूर्ण स्थिति है। इसके बाद यथार्थकः पूर्ण ख्याति का उदय होता हैं । उसी का नाम शिवत्व या परम शिव की अवस्था है। यही वास्तविक पूर्णत्व है , इस अवस्था में पूर्णस्वातन्त्र्य का अविर्भाव होता है । इस अवस्था में इच्छा -मात्र से भुवन -रचना का अर्थात् विश्व -रचना के अधिकार की प्राप्ति होती है , पञ्चकृत्यकारित्व का आविर्भाव भी इसी समय होता है ।
बौद्धशास्त्र में सुखावती की रचना अमिताभ बुद्ध के द्वारा हुइ थी , कहा जाता है कि यह इसी स्थिति के अनुरुप व्यापार है । विश्वमित्र प्रभृतियों की जगद् रचना का विवरण -प्रकार भी शास्त्र में परिचित है । तान्त्रिक अध्यात्म संस्कृति का लक्ष्य इसी परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है , केवल मात्र स्वर्गादि ऊर्ध्व लोक तथा लोकान्तरों में गति या कैवल्य अथवा निञ्जन भाव की प्राप्ति अथवा मायातीत अधिकारी पद का है । इस प्रकार यह तान्त्रिक -संस्कृति का अवदान तुच्छ नहीं समझा जा सकता है ।
रुद्रयामल और अष्टाङयोग --- बिना यौगिक क्रियाओं के शरीर शुद्ध नहीं होता है और बिना शरीर शुद्धि के कुण्डलिनी जागरण या लय योग असम्भव है । अतः रुद्रयामल के २३वें से लेकर २७ पटलों में सक्षिप्त रुप से अष्टाङु योगगत प्राणायाम की चर्चा की गई है । इनका विस्तृत विवरण होना अत्यन्त आवश्यक है । इनमें भी सर्वप्रथम हमे प्राणवायु (जिससे शरीर संचालित है ) को समझना चाहिए क्योंकि प्राणायाम के द्वारा योगी योग में प्रवेश करता है ।
11……संक्षिप्त विवरण - प्राणायाम की प्रक्रिया
.. प्राणायाम की प्रक्रिया
प्राणायाम का अर्थ है श्वास की गति को कुछ काल के लिये रोक लेना । साधारण स्थिति में श्वासों की चाल दस प्रकार की होती है ---पहले श्वास का भीतर जाना , फिर रुकना , फिर बाहर निकलना ; फिर रुकना , फिर भीतर जाना , फिर बाहर निकलना इत्यादि । प्राणायाम में श्वास लेने का यह सामान्य क्रम टूट जाता है । श्वास (वायु के भीतर जाने की क्रिया ) और प्रश्वास (बाहर जाने की क्रिया ) दोनों ही गहरे और लम्बे होते हैं और श्वासों का विराम अर्थात् रुकना तो इतनी अधिक देर तक होता है कि उसके सामने सामान्य स्थिति में हम जितने काल तक रुकते है वह तो नहीं के समान और नगण्य ही है । योग की भाषा में श्वास खींचन को ‘पूरक ’ बाहर निकालने को ‘रेचक ’ और रोक रखने को ‘कुम्भक ’कहते हैं । प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं और जितने प्रकार के प्राणायाम हैं , उन सबमें पूरक , रेचक और कुम्भक भी भिन्न -भिन्न प्रकार के होते हैं । पूरक नासिका से करने में हम दाहिने छिद्र का अथवा बायें का अथवा दोनों का ही उपयोग कर सकते हैं । रेचक दोनोम नासारन्धों से अथवा एक से ही करना चाहिये । कुम्भक पूरक के भी पीछे हो सकता है और रेचक के भी , अथवा दोनों के ही पीछे न हो तो भी कोई आपत्ति नहीं। पूरक , कुम्भक और रेचक के इन्हीं भेदों को लेकर प्राणायाम के अनेक प्रकार हो गये हैं ।
पूरक , कुम्भक और रेचक कितनी -कितनी देर तक होना चाहिये , इसका भी हिसाब रखा गया हैं । यह आवश्यक माना गया है कि जितनी देर तक पूरक किया जय , उससे चौगुना समय कुम्भक में लगाना चाहिये और दूना समय रेचक में अथवा दूसरा हिसाब यह है कि जितना समय पूरक में लगाया जाय उससे दूना कुम्भक में और उतरना ही रेचक में लगाया जाय । प्राणायाम की सामान्य प्रक्रिया का दिग्दर्शन कराकर अब हम प्राणायाम सम्बन्धी उन खास बातों पर विचार करेंगे जिनसे हम यह समझ सकेंगे कि प्राणायाम का हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव पडता है ।
पूरक करते समय जब किं साँस अधिक -से -अधिक गहराई के साथ भीतर खींचे जाती है तथा कुम्भक के समय भी , जिसमें बहुधा साँस को भीतर रोकना होता है , आगे की पेट की नसों को सिकोडकर रखा जाता है । उन्हें कभी फुलाकर आगे की ओर नहीं बढाया जाता । रेचक भी जिसमें साँस को अधिक -से अधिक गहराई के साथ बाहर निकालना होता है , पेट और छाती को जोर से सिकोडना पडता है और उड्डीयान ----बन्ध के लिये पेट को भीतर की ओर खींचा जाता है । प्राणायाम के अभ्यास के लिये कोई -सा उपयुक्ति आसन चुन लिया जाता है , जिसमें सुखपूर्वक पालथी मारी जा सके और मेरुदण्ड सीधा रह सके ।
एक विशेष प्रकार का प्राणायाम होता है जिसे भस्त्रि का प्राणायाम करते हैं । उसके दो भाग होते हैं , जिनमें से दूसरे भाग कीं प्रक्रिया वही है जो ऊपर कही गयी है ।
पहले भाग में साँस को जल्दी -जल्दी बाहर निकालना होता है , यहाँ तक कि एक मिनट में २४० बार साँस बाहर आ जाते हैं । योग में एक श्वास की क्रिया होती है जिसे ‘कपालभाति ’ कहते हैं । भस्त्रिका के पहले भाग में ठीक वैसी ही क्रिया की जाती है ।
प्राणायाम का शरीर पर प्रभाव
सामान्य शरीरविज्ञान में मानवशरीर के अंदर काम करने वाले भिन्न -भिन्न अङुसमूह हैं । इन अङुसमूहों में प्रधान हैं - स्नायुजाल (Nervous system),ग्रन्थिसमूह (Glandular system),श्वासोपयोगी अङुसमूह (Pespiratory system) रक्तवाह , अङुसमूह (Digestive system) | इन सभी पर प्राणायाम का गहरा प्रभाव पडता हैं । मल को बाहर निकालने वाले अङो में हम देखते हैं कि आँते और गुर्दा तो पेट के अंदर हैं और फेफडे छाती के अन्दर । साधारण तौर पर साँस लेने में उदर की मांसपेशियाँ क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर जाती हैं , जिससे आँतो और गुर्दे में भी हलचल और हलकी -हलकी मालिश होती रहती है । प्राणायाम में पूरक एवं रेचक तथा कुम्भक करते समय यह हलचल और मालिश और भी स्पष्टरुप से होने लगाती है । इससे यदि कहीं रक्त जमा हो गया हो तो इस हलचल के कारण उस पर जोर पडने से वह हट सकता है । यही नहीं , आँतो और गुर्दे के व्यापार को नियन्त्रण में रखने वाले स्नायु और मांसपेशियाँ भी सुदृढ हो जाती हैं । इस प्रकार आँतो और गुर्दे को प्राणायाम करते समय ही नहीं , बल्कि शेष समय में भी लाभ पहुँचता है । स्नायु और मांसपेशियाँ जो एक बार मजबूत हो जाती हैं , वे फिर चिरकाल तक मजबूत ही बनी रहती है और प्राणायाम से अधिक स्वस्थ हो जाने पर आँते और गुर्दे अपना कार्य और भी सफलता के साथ करने लगते हैं ।
यही हाल फेफडों का है । श्वास की क्रिया ठीकर तरह से चलती रहे , इसके लिये आवश्यकता है श्वासोपयोगी मांसपेशियों के सुदृढ होने की और फेफडों के लचकदार होने की । शारीरिक दृष्टि से प्राणायाम के द्वारा इन मांसपेशियों और फेफडों का संस्कार होता है और कार्बनडाई आक्साईड नामक दूषित गैस का भी भली भाँति निराकरण हो जाता है । इस प्रकार प्राणायाम आँतो , गुर्दे तथा फेफडों के लिये , हो शरीर से मल को निकाल बाहर करने के तीन प्रधान अङु हैं , बडी मूल्यवान कसरत है ।
आहार का परिपाक करने वाले और रस बनाने वाले अङों पर भी प्राणायाम का अच्छा असर पडता है । अन्न -जल के परिपाक में आमाशय , उसके पृष्ठभाग में स्थित Pancreasनामक ग्रन्थि और यकृत मुख्य रुप से कार्य करते हैं और प्राणायाम में इन सबकी अग्रेजी में Diaphragm कहते हैं और पेट की मांसपेशियाँ , ये दोनों ही बारी -बारी से खूब सिकुडते हैं और फिर ढीले पड जात हैं , जिससे उपर्युक्त पाकोपयोगी अङो की एक प्रकार से मालिश हो जाती है । जिन्हें अग्निमान्द्य और बध्दकोष्ठता की शिकायत रहती है , उनमें से अधिक लोगों के जिगर में सदा ही रक्त जमा रहता है और फलतः उसकी क्रिया दोषयुक्त होती है । इस रक्तसंचय को हटाने के लिये प्राणायाम एक उत्तम साधन है ।
किसी भी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसकी नाडियों में होने वाले रक्त को ऑक्सिजन प्रचुर मात्रा में मिलता रहे । योगशास्त्र में बतायी हुई पद्धति के अनुसार प्राणायाम करने से रक्त को जितना अधिक ऑक्सिजन मिल सकता है , उतना अन्य किसी व्यायाम से नहीं मिल सकता । इसका कारण यह नहीं कि प्राणायाम करते समय मनुष्य बहुत -सा ऑक्सिजन पचा लेता हैं , बल्कि उसके श्वासोपयोगी अङसमूह का अच्छा व्यायाम हो जाता है ।
जो लोग अपने श्वास की क्रिया को ठीक करने के लिये किसी प्रकार का अभ्यास नहीं करते , वे अपने फेफडों के कुछ अंशो से ही साँसे लेते हैं , शेष अंश निकम्मे रहते हैं , इस प्रकार निकम्मे रहने वाले अंश बहुधा फेफडों के अग्रभाग होते हैं । इन अग्रभागों में ही जो निकम्मे रहते है और जिनमें वायु का संचार अच्छी तरह से नहीं होता , राजयक्ष्मा के भयङकर कीटाणु बहुधा आश्रय पाकर बढ जाते हैं । यदि प्राणायाम के द्वारा फेफडों के प्रत्येक अंश से काम लिया जाने लगे और उनका प्रत्येक छिद्र दिन में कई बार शुद्ध हवा से धुल जाया करे तो फिर इन कीटाणुओं का आक्रमण असम्भव हो जायगा और श्वास सम्बन्धी इन भयंकर रोगों से बचा जा सकता हैं ।
प्राणायाम के कारण पाकोपयोगी , श्वालोपयोगी एवं मल को बाहर निकालने वाले अङों को क्रिया ठीक होने से रक्त अच्छा बना रहेगा । यही रक्त विभक्त होकर शरीर के भिन्न -भिन्न अङों में पहुँच जायगा । यह कार्य रक्तवाहक अङों का खास कर ह्रदय का हैं । रक्तसंचार से सम्बन्ध रखने वाला प्रधान अङु ह्रदय है और प्राणायाम के द्वारा उसके अधिक स्वस्थ हो जाने से समस्त रक्तवाहक अङु अच्छी तरह से काम करने लगते हैं ।
परन्तु बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती । भस्त्रिका प्राणायाम में , खास कर उस हिस्से में जो कपालभाति से मिलता -जुलता है , वायवीय स्पन्दन प्रारम्भ होकर मानव -शरीर के प्रायः प्रत्येक सूक्ष्म -से -सूक्ष्म अङु को , यहाँ तक कि नाडियों एवं सूक्ष्म शिराओं तक को हिला देते हैं । इस प्रकार प्राणायाम से सारे रक्तवाहक अङुसमूह की कसरत एवं मालिश हो जाती है और वह ठीक तरह से काम करने के योग्य बन जागा है ।
रक्त की उत्तमता और उसके समस्त स्नायुओं और ग्रन्थियों में उचित मात्रा में विभक्त होने पर ही इनकी स्वस्थता निर्भर है । प्राणायाम में विशेष कर भस्त्रिका प्राणायाम में रक्त की गति बहुत तेज हो जाती है और रक्त भी उत्तम हो जाता है । इस प्रकार प्राणायाम से Enddocerine ग्रन्थिसमूह को भी उत्तम और पहले की अपेक्षा प्रचुर रक्त मिलने लगता है , जिससे वे पहले की अपेक्षा अधिक स्वस्थ हो जाती हैं । इसी रीति से हम मस्तिष्क , मेरुदण्ड और इनकी नाडियों तथा अन्य सम्बन्धित नाडियो को स्वस्थ बना सकते हैं ।
प्राणायाम का मस्तिष्क पर प्रभाव
सभी शरीरविज्ञानविशारदों का इस विषय में एक मत है कि साँस लेते समय मस्तिष्क में से दूषित रक्त प्रवाहिता होता है और शुद्ध रक्त उसमें संचरित होता है । यदि साँस गहरी हो तो दूषित रक्त एक साथ बह निकलता है और ह्रदय से जो शुद्ध रक्त वहाँ आता है वह और भी सुन्दर आने लगता है । प्राणायाम की यह विधि है कि उसमें साँस गहरे -से गहरा लिया जाय , इसका परिणाम यह होता है कि मस्तिष्क से सारा दूषित रक्त बह जाता है और ह्रदय का शुद्ध रक्त उसे अधिक मात्रा में मिलता हैं । योग उड्डीयान -बन्ध को हमारे सामने प्रस्तुत कर इस स्थिति को और भी स्पष्ट कर देने की चेष्टा करता है । इस उड्डीयानबन्ध से हमें इतना अधिक शुद्ध रक्त मिलता है , जितना किसी श्वास सम्बन्धी व्यायाम से हमें नहीं मिल सकता । प्राणायाम से जो हमें तुरन्त बल और नवीनता प्राप्त होती है उसका यही वैज्ञानिक कारण है ।
प्राणायाम का मेरुदण्ड पर प्रभाव
मेरुदण्ड एवं उससे सम्बन्धित स्नायुओं के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि इन अङों के चारों ओर रक्त की गति साधारणतया मन्द होती है । प्राणायाम से इन अङों में रक्त की गति बढ जाती है और इस प्रकार इन अङों को स्वस्थ रखने में प्राणायाम सहायक होता है ।
योग में कुम्भक करते समय मूल , उड्डीयान और जालन्धर -तीन प्रकार के बन्ध करने का उपदेश दिया गया है । इन बन्धों का एक काल में अभ्यास करने से पृष्ठवंश का , जिसके अंदर मेरुदण्ड स्थित है तथा तत्सम्बन्धित स्नायुओं का उत्तम रीति से व्यायाम हो जाता है । इन बन्धों के करने से पृष्ठवंश को यथास्थान रखने वाली मांसपेशियाँ , जिनमें तत्सबन्धित स्नायु भी रहतें हैं , क्रमशः फैलती हैं और फिर सिमट जाती हैं , जिससे इन पेशियाँ तथा मेरुदण्ड एवं तत्सम्बन्धित स्नायुओं में रक्त की गति बढ जाती है । बन्ध यदि न किये जायँ तो भी प्राणायाम की सामान्य प्रक्रिया , ही ऐसी है कि उससे पृष्ठवंश पर ऊपर की ओर हल्का -सा खिंचाव पडता है , जिससे मेरुदण्ड तथा तत्सम्बन्धित स्नायुओं को स्वस्थ रखने में सहायत मिलती है ।
स्नायुजाल के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालने के लिये तो सबसे उत्तम प्राणायाम भस्त्रिका है । इस प्राणायाम में श्वास की गति होने से शरीर के प्रत्येक सूक्ष्म -से -सूक्ष्म अङु की मालिश हो जाती है और इसका स्नायुजाल पर बहुत अच्छा प्रभाव पडता है ।
निष्कर्ष रुप में कहा जा सकता है कि प्राणायाम हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिये सर्वोत्तम व्यायाम है । इसीलिये भारत के प्राचीन योगाचार्य प्राणायाम को शरीर की प्रत्येक आभ्यन्तर क्रिया को स्वस्थ रखने का एकमात्र साधन मानते थे । उनमें से कुछ तो प्राणायाम को शरीर का स्वाच्छ ठीक रखने में इतना सहायक मानते हैं कि वे इसके लिये अन्य किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं होता , अपितु इस शरीरयन्त्र को जीवन देने वाले प्रत्येक व्यापार पर अधिकार हो जाता है ।
श्वाससम्बन्धी व्यायामों से श्वासोपयोगी अङुसमूह को तो लाभ होता ही है , किंतु उनका असली महत्त्व तो इस बात को लेकर है कि उनसे अन्य अङुसमूहों को भी , खासकर स्नायुजाल को विशेष लाभ पहुँचता है ।
12.. संक्षिप्त विवरण - बन्ध एवं मुद्राएँ
कुछ उपयोगी बन्ध एवं मुद्राएँ
योगसाधना में बन्धों एवं मुद्राओं का विशेषरुप से उल्लेख आया है । इनमें से कुछ उपयोगी बन्धों एवं मुद्राओं का यहाँ विवरण दिया जा रहा है जिनका उल्लेख रुद्रयामला में आया हैं ।
बन्ध
१ . ,मूलबन्ध --- मूल गुदा एवं लिङु -स्थान के रन्ध्र को बन्द करने का नाम मूलबन्ध है । वाम पाद की एडी को गुदा और लिङु के मध्यभाग में दृढ लगाकर गुदा को सिकोडकर योनिस्थान अर्थात् गुदा और लिङु एवं कन्द के बीच के भाग को दृढतापूर्वक संकोचन द्वारा अधोगत अपानवायु को बल के साथ धीरे -धीरे ऊपर की ओर है । अन्य आसनों के साथ एडी को सीवनी पर बिना लगाये हुए भी मूलबन्ध लगाया जा सकता है ।
फल --- इससे अपानवायु का ऊर्ध्व -गमन होकर प्राण के साथ एकता होती है । कुण्डलिनी -शक्ति सीधी होकर ऊपर की ओर चढती की ओर चढती है । कोष्ठबद्धता दूर करने , जठराग्नि को प्रदीप्त करने और वीर्य को ॠर्ध्वरेतस् बनामे में बन्ध अति उत्तम है । साधकों को न केवल भजन के अवसर पर किन्तु हर समय मूल बन्ध को लगाये रखने का अभ्यास करना चाहिये ।
२ . उड्डीयानबन्ध --- दोनों जानुओं को मोडकर पैरों के तलवों को परस्पर भिडाकर पेट के नाभि से नीचे और ऊपर के आठ अंगुल हिस्से को बलपूर्वक खींचकर मेरुदण्ड (रीढ की हड्डी से ) ऐसा लगा दे जिससे कि पेट के स्थान पर गढडा -सा दीखने लगे । पेट को अंदर की ओर जितना अधिक खींचा जायगा , उतना ही यह बन्ध अच्छा होगा । इसमें प्राण पक्षी के सदृश सुषुम्ना की ओर उडने लगता है , इसलिये यह बन्ध उड्डीयान कहलाता है । इस बन्ध को पैरों के तलवों को बिना भिडाये हुए भी किया जा सकता है ।
फल --- प्राण और वीर्य का ऊपर की ओर दौडना , मन्दाग्नि का नाश , क्षुधा की वृद्धि , जठराग्नि का प्रदीप्त और फेफडे का शक्तिशाली होना है , इस बन्ध के फल है ।
३ . जालन्धरबन्ध --- कण्ठ को सिकोडकर ठोढी को दृडतापूर्वक कण्ठकूप में इस प्रकार स्थापित करे कि ह्रदय से ठोडी का अन्तर केवल चार अंगुल का रहे , सीना आगे की ओर तना रहे । यह बन्ध कण्ठस्थान के नाडी -जाल के समूह को बाँधे रखता है , इसलिये इसका नाम जालन्धर -बन्ध है ।
फल --- कण्ठ का सुरीला , मधुर और आर्कषण होना , कण्ठ के संकोच द्वारा इडा , एवं पिङुला नाडियों के बंद होने पर प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश करना है ।
प्रायः सभी आसन मुद्राएँ और प्राणायाम मूलबन्ध और उड्डीयानबन्ध के साथ किये जाते है । किन्तु राजयोग में ध्यानावस्था में जालन्धरबन्ध लगाने की बहुत कम आवश्यकता होती है ।
४ . महाबन्ध --- महाबन्ध की दो विधियों में पहली विधि इस प्रकार है ---बायें पैर की एडी को गुदा और लिङु के मध्यभाग में जमाकर बायीं जंघा के ऊपर दाहिन पैर को रख , समसूत्र में हो , वाम अथवा जिस नासारन्ध्र से वायु चल रहा हो उससे ही पूरक करके जालन्धर -बन्ध लगाये । फिर मूलद्वार से वायु का ऊपर की ओर आकर्षण करके मूलबन्ध लगाये । मन को मध्य नाडी में लगाये हुए यथाशक्ति कुम्भक करे । तत्पश्चात् पूरक के विपरीत वाली नासिका से धीरे -धीरे रेचन करे । इस प्रकार दोनों नासिका से अनुलोम एवं विलोम रिति से समान प्राणायाम करे ।
इसकी दूसरी इस प्रकार है ---पदम अथवा सिद्धासन से बैठे , योनि और गुह्यप्रवेश सिकोड , अपानवायु को ऊर्ध्वगामी कर , नाभिस्थ समानवायु के साथ मिलाकर और ह्रदयस्थ प्राणवायु को अधोमुख करके प्राण और अपानवायुओं के साथ नाभिस्थल पर दृढरुप से कुम्भक करे ।
फल --- प्राण का ऊर्ध्वगामी होना -वीर्य की शुद्धि , इडा , पिङुला और सुषुम्ना का सङुम प्राप्त होना , बल की वृद्धि आदि इसके गुण है ।
५ . महाबन्ध --- यह दो प्रकार से किया जाता है - महाबन्ध की प्रथम विधि के अनुसार मूलब्न्धपूर्वक कुम्भक करके दोनों हाथों की हथेली भूमि में दृढ स्थिर करके , हाथों के बल ऊपर उठाकर दोनों नितम्बों को शनैःशनैः ताडना दे और ऐसा ध्यान करे कि प्राण इडा एवं पिङुला को छोडकर कुण्डलिनी -शक्ति को जगाता हुआ सुषुम्ना में प्रवेश कर रहा है । तत्पश्चात् वायु को शनैः शनैः महाबन्ध की विधि के अनुसार रेचन करे इसकी दूसरी विधि इस प्रकार है --
मूलबन्ध के साथ पद्मासन से बैठे , अपान और प्राणवायु को नाभिस्थान पर एक करके (मिलकर ) दोनों हाथों को तानकर नितम्बों से मिलते हुए भूमि पर जमाकर नितम्ब को आसनसहित उठा -उठाकर भूमि पर ताडित करते रहें ।
फल --- कुण्डलिनी -शक्ति का जाग्रत् होना , प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश करना इसके प्रमुख गुण है । महाबन्ध , महावेध और महामुद्रा - तीनों को मिलाकर करना अधिक फलदायक है ।
मुद्रा
१ . खेचरी मुद्रा --- जीभ को ऊपर की ओर उलटी ले जाकर तालु -कुहर (जीभ के ऊपर तालु के बीच के गढे ) में लगाये रखने का नाम ‘खेचरी -मुद्रा ’ है । इसके निमित्त जिह्रा को बढाने के तीन साधन किये जाते है - छेदन , चालन और दोहन।
( १ ) छेदन --- जीभ के नीचे के भाग मेम सूताकर वाली एक नाडी नीचे वाले दाँतो की जड के साथ जीभ को खींचे रखती है । इसलिये जीभ को ऊपर चढानो कठिन होता है । प्रथम इस नाडी के दाँतो के निकट वाले एक ही स्थान पर स्फटिक ( बिल्लौर ) का धार वाला टुकडा प्रतिदिन प्रातःकाल चार - पाँच बार फेरते रहें । कुछ दिनों तक ऐसा करने के पश्चात् वह नाडी उस स्थान में पूर्ण कट जायगी । इसी प्रकार क्रमशः उससे ऊपर - ऊपर एक - एक स्थान को जिह्रामूल तक काटते चले जायँ । स्फटिक फेरने के पश्चात् माजूफल का कपडछन चूर्ण ( टेरिन ऐसिड ) जीभ के ऊपर - नीचे तथा दाँतो पर मलें नून , हरीतकी और कत्थे का चूर्ण छेदन किये हुए स्थान पर लगाये । यह छेदन - विधि सबसे सुगम है और इससे किसी प्रकार की हानि पहुँचने की सम्भावना नहीं है , यद्यापि इसमें समय अधिक लगेगा । साधारणतया छेदन का कार्य किसी धातु के तीक्ष्ण यन्त्र से प्रति आठवें दिन उस शिरा को बाल के बराबर छेदकर घाव पर कत्था और हरड का चूर्ण लगाकर करते हैं । इसके छेदन के लिये नाखून काटने वाला - जैसा एक तीक्ष्ण यन्त्र और खाल छीलने के लिये एक दूसरे यन्त्र की आवश्यकता होती है , जिससे कटा हुआ भाग फिर न जुडने पावे । इसमें नाडी के सम्पूर्ण अंश के एक साथ कट जाने से वाक् तथा आस्वादन - शक्ति के नष्ट हो जाने का भय रहता है । इसलिये इसे किसी अभिज्ञ पुरुष की सहायता से ही करना चाहिये । छेदन की आवश्यकता केवल उनको होती है , जिनकी जीभ और यह नाडी मोटी होती है । जिनकी जीभ लंबी और यह नाडी पतली होती है , उन्हें छेदने की अधिक आवश्यकता नहीं है ।
( २ - ३ ) चालन व दोहन --- अँगूठे और तर्जनी अँगुली से अथवा बारीक वस्त्र से जीभ को पकडकर चारों तरफ उलट - फेरकर हिलाने और खींचने को चालन कहते हैं । मुक्खन अथवा घी लगाकर दोनों हाथों की अँगुलियों से जीभ का गाय के स्तनदोहन जैसे पुनःपुनः धीरे - धीरे आकर्षण करने की क्रिया का नाम दोहन है ।
निरन्तर अभ्यास करते रहने से अन्तिम अवस्था में जीभ इतनी लम्बी हो सकती है कि नासिका के ऊपर भ्रूमध्यतक पहुँच जाय । इस मुद्रा का बडा महत्त्व बतलाया गया है , इससे ध्यान की अवस्था परिपक्व करने में बडी सहायता मिलती है । जिह्राओं के भी नाना प्रकार के भेद देखने में आये हैं । किसी जिह्रा में सूताकार नाडी के स्थान में मोटा मांस होता है , जिसके काटने में अधिक कठिनाई होती है । किसी -किसी जिह्रा में न यह नाडी होती है , न मांस । उसमें छेदने की आवश्यकता नहीं है । केवल चालन एवं दोहन होना चाहिये ।
२ . महामुद्रा --- इसकी पहली विधि इस प्रकार है --- मूलबन्ध लगाकर बायें पैर की एडी से सीवन (गुदा और अण्डकोष के मध्य का चार अँगुल स्थान ) दबाये और दाहिने पैर को फैलाकर उसकी अँगुलियों को दोनों हाथों से पकडे । पाँच घर्षण करके बायीं नासिका से पूरक करे और जालन्धर -बन्ध लगाये । फिर जालन्धर -बन्ध -खोलकर दाहिनी नासिका से पूरक करे और जालन्धर -बन्ध लगाये । फिर जालन्धर -बन्ध -खोलकर दाहिनी नासिका से रेचक करे । वह वामाङु की मुद्रा समाप्त हुई । इसी प्रकार दक्षिणाङु में इस मुद्रा को करना चाहिये तथा दूसरी विधि इस प्रकार है ---बायें पैर की एडी को सीवन (गुदा और उपस्थ के मध्य के चार अङुल भाग ) में बलपूर्वक जमाकर दायें पैर को लम्बो फैलाये । फिर शनैःशनैः पूरक के साथ मूल तथा जालन्धर बन्ध लगाते हुए दायें पैर का अँगूठा पकडकर मस्तक के दायें पैर के घुटने पर जमाकर यथाशक्ति कुम्भक करे । कुम्भक के समय पूरक की हुई वायु को कोष्ठ में शनैः शनीः फुलावे और ऐसी भावना करे कि प्राण कुण्डलिनी को जाग्रत् करके सुषुम्ना में प्रवेश कर रहा है । तत्पश्चात् मस्तक को घुटने से शनैःशनै रेचक करते हुए उठाकर यथास्थिति में बैठ जाय । इसी प्रकार दूसरे अङु से करना चाहिये । प्राणायाम की संख्या एवं समय बढाता रहे ।
फल --- मन्दाग्नि , अजीर्ण आदि उदर के रोगों तथा प्रमेह का नाश , क्षुधा की वृद्धि और कुण्डलिनी की जाग्रत् होना है ।
३ . आश्विनीमुद्रा --- सिद्ध अथवा पद्मासन से बैठकर योनिमण्डल को अश्व के सदृश पुनः पुनः सिकोडना अश्विनीमुद्रा कहलाती है ।
फल --- यह मुद्रा प्राण के उत्थान और कुण्डलिनी -शक्ति के जाग्रत् करने में सहायक होती है । अपानवायु को शुद्ध और वीर्यवाही स्नायुओं को मजबूत करती है ।
४ . शक्तिचालिनीमुद्रा --- सिद्ध अथवा पद्मासन से बैठकर हाथों की हथेलियाँ पृथ्वी पर जमा दे । बीस -पचीस बार शनैःशनैः दोनों नितम्बो को पृथ्वी से उठा -उठाकर ताडन करे । तत्पश्चात् मूलबन्ध लगाकर दोनों नासिकाओं से अथवा वाम से अथवा जो स्वर चल रहा हो उस नासिका से पूरक करके प्राणवायु को अपानवायु से संयुक्त करके जालन्धर -बन्ध लगाकर यथाशक्ति कुम्भक करे । कुम्भक के समय अश्विनीमुद्रा करे अर्थात् गुह्य -प्रदेश हा आकर्षण -विकर्षण करता रहे । तत्पश्चात् जालन्धर -बन्ध खोलकर यदि दोनों नासिकापुट से पूरक किया हो तो दोनों से अथवा पूरक के विपरीत नासिकापुट से रेचक करे और निर्विकार होकर एकाग्रथापूर्वक बैठ जाय ।
घेरण्डसंहिता में इस मुद्रा को करते समय बालिश्त भर चौडा , चार अङुल लंबा , कोमल , श्वेत और सूक्ष्म वस्त्र नाभि पर कटिसूत्र से बाँधकर सारे शरीर पर भस्म मलकर करना बतलाय गया है ।
फल --- सर्वरोग -नाशक और स्वास्थ्यवर्धक होने के अतिरिक्त कुण्डलिनी -शक्ति को जाग्रत् करने में अत्यन्त सहायक है । इसके साधक अवश्य लाभ प्राप्त करता है ।
५ . योनिमुद्रा --- सिद्धासन से बैठ सम -सूत्र हो षण्मुखी मुद्रा लगाकर अर्थात् दोनों अँगूठों से दोनों कानों को , दोनों तर्जनियों से दोनों नेत्रों को , दोनों मध्यमाओं से नाक के छिद्रो को बंद करके और दोनों अनामिका एवं कनिष्ठिकाओं को दोनों ओठों के पास रखकर काफी मुद्रा द्वारा अर्थात् जिह्रा को कौए की चोंच के सदृश बनाकर उसके द्वारा प्राणवायु को खींचकर अधोगत अपानवायु के साथ मिलाये । तत्पश्चात् ओ३म् जाप करता हुआ ऐसी भावना करे कि उसकी ध्वनि के साथ परस्पर मिलि हुई वायु कुण्डलिनी को जाग्रत् करके षट्चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रदल -कमल में जा रही है । इससे अन्तर्ज्योति का साक्षात्कार होता है ।
६ . योगमुद्रा --- मूलबन्ध के साथ पद्मासन से बैठकर प्रथम दोनों नासिकापुटों से पूरक करके जालन्धनबन्ध लगाये । तत्पश्चात् दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर बायें हाथ से दायें की और दायें हाथ से बायें हाथ की कलाई को पकडे , शरीर को आगे झुकाकर पेट के अन्दर एडियों को दबाते हुए सिर को जमीन पर लगा दें । इस प्रकार यथाशक्ति कुम्भक करने के पश्चात् सिर को जमीन से उठाकर जालन्धर -बन्ध खोलकर दोनों नासिकाओं से रेचन करे ।
फल --- पेट के रोगों को दूर करने और कुण्डलिनी -शक्ति को जागृत् करने में यह मुद्रा सहायक होती है ।
७ . शाम्भवीमुद्रा --- मूल और उड्डीयाबन्ध के साथ सिद्ध अथवा पद्मासन से बैठकर नासिका के अग्रभाग अथवा भ्रूमध्य में दृष्टि को स्थिर करके ध्यान जमाना ‘शाम्भवी मुद्रा ’ कहलाती है ।
८ . तडागी मुद्रा --- तडाग (तालाब ) के सदृश कोष्ठ को वायु से भरने को तडागी मुद्रा कहते हैं । शवासन से चित्त लेटकर जिस नासिका का स्वर चल रहा हो , उससे पूरक तालाब के समान पेट को फैलाकर वायु से भर लेना चाहिए । तत्पश्चात् कुम्भक करते हुए वायु को पेट में इस प्रकार हिलावे , जिस प्रकार तालाब का जल हिलता है । कुम्भक के पश्चात् सावधनी से वायु का शनैःशनैः रेचन कर दे , इससे पेट के सर्वरोग समूल नष्ट होते हैं ।
९ . विपरीतकरणीमुद्रा -शीर्षासन -कपालासन --- पहिले जमीन पर मुलायम गोल लपेटा हुआ वस्त्र रखकर उस पर अपने मस्तक को रखे । फिर दोनों हाथों के तलों को मस्तक के पीछे लगाकर शरीर को उलटा ऊपर उठाकर सीधा खडा कर दे । थोडे ही प्रयत्न से मूल और उड्डीयान स्वयं लग जाता है । यह मुद्रा पद्मासन के साथ भी की जा सकती है । इसको ऊर्ध्व -पद्मासन कहते हैं । आरम्भ में इसको दीवार के सहारे करने में आसानी होगी ।
फल --- वीर्यरक्षा , मस्तिष्क , नेत्र , ह्रदय तथा जठराग्नि का बलवान होना , प्राण की गति स्थिर और शान्त होना , कब्ज , जुकाम , सिरदर्द आदि का दूर होना , रक्त क शुद्ध होना और कफ के विकार का दूर होना है ।
१० . उन्मनी मुद्रा --- किसी सुख -आसन से बैठकर आधी खुली हुई और आधी बंद आँखों से नासिका के अग्रभाग पर टकटकी लगाकर देखते रहना यह ‘उन्मनी मुद्रा ’ कहलाती है । इससे मन एकाग्र होता है ।
13…संक्षिप्त विवरण - रुद्रयामलगत स्वरयोग
रुद्रयामलगत स्वरयोग
एकादश पटल में स्वरोदय पर विचार प्रस्तुत किया गया है । इस सम्बन्ध में द्वादश चक्रों का निर्माण और उनके स्वरज्ञान एवं वायु की गति को जानकर अपने प्रश्नों का विवेचन करना चाहिए । स्वर -योग के अन्य ग्रन्थों से इसे लेकर यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है ---
नरपतिजयचर्या स्वरोदयः के ‘मात्रास्वराऽध्यायः ’ में मात्रा स्वरों के विषय में इस प्रकार कहा गया है ---
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि ख्याता ये ब्रह्मयामले ।
मात्रादिभेदभिन्नानां स्वराणां षोडशोदयान् ॥१॥
मातृकायां पुरा प्रोक्ताः स्वराः षोडशसंख्यया ।
अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ लृ लृ इ ए ऐ ओ औ अं अः ।
तेषां द्वावन्तिमौ (अंअः ) त्याज्यौ -चत्वारश्च (ऋ लृ लृ ) नपुंसकौ ॥२॥
शेषा दश स्वरास्तेषु स्यदेकैको द्विके द्विके ।
ज्ञेयास्तत्र स्वरा आद्या द्दस्वाः (अ इ उ इ ओ ) पञ्च स्वरोदये ॥३॥
लाभलाभं सुखं दुःखं जीवितं मरणं तथा ।
जयः पराजयश्चेति सर्व ज्ञेयं स्वरोदये ॥४॥
स्वरादिमात्रिकोच्चारो मातृव्याप्तं जगत्त्रम् ।
तस्मात्स्वरोद्धवं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥५॥
अकाराद्याः स्वराः पञ्च ब्रह्माद्याः पञ्चदेवताः ।
निवृत्याद्याः कलाः पञ्च इच्छाद्याः शक्तिपञ्चकम् ॥६॥
अब मैं ब्रह्मयामल में कहे हुये मात्राभेद से भिन्न मातृकाचक्र में कहे हुये सोलह स्वरों को कह रहा हूँ । अ , आ , इ , ई , उ , ऊ , ए , ऐ , ओ , औ , अं , अः --ये सोलह स्वर हैं । इनमें दो अन्त के अं अः त्याग देना चाहिए और चार ऋ ऋ लृ लृ - ये नपुंसक स्वर हैं । शेष दशस्वर (अ , आ , इ , ई , उ , ऊ , ए , ऐ , ओ , औ )हैं । इनमें दो दो स्वरों का एक ही स्वर मानना चाहिए --जैसे अ आ को केवल अ मानना चाहिये । इस प्रकार पाँच ही अ , इ , उ , ए ओ स्वर मुख्य हैं ।सभी चराचर पदार्थो के नामोच्चारण करने में अकारादि मातृका के बिना वर्णो का उच्चारण नहीं हो सकता है । इसलिये मातृका से तीनोम जगत् व्याप्त है ।अतःशुभाशुभ फल के कहने के लिये स्वरों की ही प्रधानता है । अकारादि अ , इ , उ , ए ओ स्वरों के क्रम से ब्रह्मा , विष्णु , रुद्र , सूर्य और चन्द्रमा स्वामी हैं , अर्थात् अकारादि स्वरों के उदयकाल में प्रश्नकर्त्ता इन्हीं देवताओं का स्मरण कर कार्य को करे एव्म इन्हीं स्वरों के उदयकाल में प्रश्नकर्ता इन्हीं देवताओं का स्मरण कर कार्य को करे एवं इन्हीं स्वरों के उदयकाल में निवृत्ति आदि क्रम से पाँच कलायें होती है । (निवृत्ती , प्रतिष्ठा , विद्या , शान्ति और अतिशान्ति ) ये पाँच कलाओं के नाम है और इन्हीं स्वरों के उदयकाल में इच्छादि पाँच शक्तियाँ भी होती है । उनके नाम इच्छा , ज्ञान , प्रभा , श्रद्धा और मेधा है ॥१ -६॥
मायाद्याश्चक्रभेदाश्च धराद्यं भूतपञ्चकम् ।
शब्दादिविषायास्ते च कामबाणा इतीरिताः ॥७॥
पिण्ड पदं तथा रुपं रुपातीतं निरञ्जनम् ।
स्वरभेदस्थित ज्ञानं ज्ञायते गुरुतः सदा ॥८॥
अकाराद्याः स्वराः पञ्च तेषामष्टविधास्त्वमी ।
मात्रा वर्णो ग्रहो जीवो राशिर्भ पिण्डयोगकौ ॥९॥
प्रसुप्तो बुध्यते येन येनाच्छति शब्दितः ।
तत्र नामाद्यवर्णे या मात्रा मात्रास्वरः स हि ॥१०॥
अ , इ , उ , ए , ओ , ये प्रसिद्ध पाँच स्वर (ज्यौतिषशास्त्र के स्वर भाग में ) हैं । इन्हीं पाँच स्वरों के मायादि पाँच (चतुरस्त्र , अर्धचन्द्र , त्रिकोण , षट्कोण , वर्तुल ) चक्रभेद हैं , अर्थात् इन स्वरों के उदय वाले अपने अपने चक्रों का पूजन करें या ग्रहण करें । ये ही स्वर गन्धादि पाँच विषय वाले है , अर्थात् अकार के उदय में गन्ध विषयक , इकारोदय में रसविषय , उकार में रुपविषय , एकारोदय में स्पर्शविषय और ओकार में शब्दविषय हैं । इन्हीं पाँच स्वरों के धरा आदि (पृथ्वी , जल , अग्नि , वायु , आकाश ) पाँच तत्त्व है , अर्थात् अकार स्वर के उदय में पृथ्वीगत प्रश्न , इकार के उदय में जलगत , उकार में अग्निगत , एकार में वायुगत और ओकर के उदय में आकाशगत अर्थात् ऊर्ध्वगत प्रश्न है । इन्हीं पाँच स्वरों के पाँच कामबाण (शोषण , मोहन , दीपन , संतापन , प्रमथन ) हैं । पिण्ड अर्थात् शरीर का जो तत्त्व , उसका जो स्वरुप , उसके ज्ञान को रुपाततीत कहते हैं । उसको भी अतिक्रमण करने को निरंजन अर्थात् शून्य कहते हैं ।
अथवा इन पाँच स्वरों की जो पाँच (बाल , कुमार , युवा , वृद्ध मृत्यु या शून्य ) अवस्थायें हैं । उन्हीं को क्रम से पिण्ड , पद , रुप , रुपातीत और निरंजन कहते हैं । यही पाँच अवस्थायें जीवधारियों की भी होती है । वेदान्तशास्त्र के पृथ्वी , अप् , तेज , वायु और आकाश इन पञ्चतत्त्वों के पञ्चकरण से जैसे ब्रह्म प्राप्ति होती है , वैसे ही यहाँ भी योगाभ्यास और गुरुमुख से अध्ययन द्वारा रहस्यमय उक्त ज्यौतिषशास्त्र का एवं रहस्यमय स्वरशास्त्र का ज्ञान भी परमार्थप्राप्ति का परम साधन बताया गया है । किन्तु इन पाँच स्वरों का भेद स्वरों में ही स्थित है जो कि गुरुमुख से ही जाना जा सकता है । जैसे सदानन्द के नाम मेम अकार है । अतः सदानन्द का अकार मात्रास्वर हुआ । शेष चक्र से स्पष्ट ॥७ -१०॥
कादिहान्तं लिखेद्वर्णान् स्वराधो ङञणोज्झितान् ।
( ककारादिहकारान्ताल्लिखेद्वर्णान्स्वराधो ङञणोज्झितान् )
तिर्यक्पंक्तिक्रमेणैव पञ्चत्रिंशत्प्रकोष्ठके ॥११॥
नरनामादिमो वर्णो यस्मात्स्वरादधः स्थितः।
स स्वरस्तस्य वर्णस्य वर्णस्वर इहोच्यते ॥१२॥
न प्रोक्ता ङञणा वर्णा नामादौ सन्ति ते नहि ।
चेद्धवन्ति तदा ज्ञेया गजडास्ते यथाक्रमम् ॥१३॥
यदि नाम्नि भवेद्वर्णः संयुक्ताक्षरलक्षणः ।
ग्राह्यस्तदादिमो वर्ण इत्युक्तं ब्रह्मयामले ॥१४॥
श्लोक ११ -१४ को समझने के लिये आचार्य ने चक्र बनाने का संकेत दिया है , उसे देखकर विषय अतिस्पष्ट हो जाता है । अकारादि पाँचो स्वरों के नीचे क्रम से आरम्भ कर ह पर्यन्त वर्णो को तिर्यक् क्रम से ३५ कोष्ठों में लिखे । किन्तु ङ ञ ण वर्णो को न लिखे । मनुष्य के नाम का प्रथम वर्ण , जिस स्वर हो वही उसका वर्णस्वर होता है । ङ ञ ण , वर्णो को नहीं कहा गया है क्योंकि प्रायः मनुष्य के नाम के आदि में ये वर्ण नहीं पाये जाते हैं । यदि कहीं किसी के नाम के आदि में हो तो इनके स्थान में क्रम से ग , ज ,ड वर्णो को समझना चाहिये , अर्थात् ग , ज , ड वर्णो के जो वर्णस्वर हों वही उन वर्णो के होंगे । यदि नाम के आदि में संयुक्ताक्षर हो तो वहाँ संयुक्ताक्षर में पहला वर्ण लेना चाहिये --ऐसा ब्रह्मयामल में कहा है । जैसे सदानन्द के नाम में आदि वर्ण स है । वह चक्र में ए स्वर के नीच है । अतः सदानन्द का एकार वर्णस्व है । इसी प्रकार श्रीपति के नाम में संयुक्ताक्षर का प्रथम वर्ण श है और वह इकार के नीचे है । इसलिये श्रीपति का इकार वर्णस्वर है । वर्णो में विशेष - स्वरशास्त्र में अ ब , श , स , च , ख , ङ , ञ , ये सजातीय माने जाते हैं । इतिवर्णस्वरः ॥११ -१४॥
यदि एक व्यक्ति के दो तीन नामोपनाम हों तो कौन नाम से स्वर विचारा जाय ? इसका यही समाधान शास्त्र में है । प्रसुप्तो भासते येन येनागच्छति शब्दितः अर्थात् सोया हुआ पुरुष जिस नाम के उच्चारण से जागरुक हो उसके उसी नाम से स्वर विचारना चाहिए ।
14……….संक्षिप्त विवरण - स्वर-विज्ञान
स्वर-विज्ञान और बिना औषध रोगनाश के उपाय
विश्वपिता विधाता ने मनुष्य के जन्म के समय में ही देह साथ एक ऐसा आश्चर्यजनक कौशलपूर्ण अपूर्व उपाय रच दिया है , जिसे जान लेने पर सांसारिक , वैषायिक किसी भी कार्य में असफलता का दुःख नहीं हो सकता । हम इस अपूर्व कौशल को नहीं जानते । इसी कारण हमारा कार्य असफल हो जाता है , आशा भङु हो जाती है । हमें मनस्ताप और रोग भोगना पडता है । यह विषय जिस शास्त्र में है , उसे स्वरोदयशास्त्र कहते है
यह स्वरशास्त्र जैसा दुर्लभ है , स्वरज्ञ गुरु का भी उतना ही अभाव है । स्वरशास्त्र प्रत्यक्ष फल देने वाला है । मुझे पद -पद पर इसका प्रत्यक्ष फल देखकर आश्चर्यचकित होना पडा है । समग्र स्वरशास्त्र को ठीक -ठीक लिपिबद्ध करना बिलकुल असम्भव है । केवल साधकों के काम की कुछ बातें यहाँ संक्षेप में दी जा रही हैं ।
स्वरशास्त्र सीखने के लिये श्वास -प्रश्वास की गति के सम्बन्ध में सम्यक् ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है ।
कायानगरमध्ये तु मारुतः क्षितिपालकः ।
‘ देहरुपी नगर में वायु राजा के समान है । ’ प्राणवायु ‘ निःश्वास ’ और ‘ प्रश्वास ’-- इन दो नामों से पुकारा जाता है । वायु ग्रहण करने का नाम निःश्वास ’ और वायु के परित्याग करने का नाम ‘ प्रश्वास ’ है । जीव के जन्म से मृत्यु के अन्तिम क्षण तक निरन्तर श्वास - प्रश्वास की क्रिया होती रहती है । यह निःश्वास नासिका दे दोनों छेदों से एक ही समय एक साथ समानरुप से नहीं चला करता । कभी बायें और कभी दाहिने पुत से चलता है । कभी - कभी एकाध घडी तक एक ही समय दोनों नाकों से समानभाव से श्वास प्रवाहित होता है ।
बायें नासापुट के श्वास को इडा में चलना , दाहिना नासिका के श्वास को पिंगला में चलना और दोनों पुटोम से एक समान चलने पर उसे सुषुम्नो में चलना कहते है । एक नासापुट को दबाकर दूसरे द्वारा श्वास को बाहर निकालने पर यह साफ मालूम हो जाता है कि एक नासिका से सरलतापूर्वक श्वास -प्रवाह चल रहा है और दूसरा नासापुट मानो बन्द है , अर्थात् उससे दूसरी नासिका की तरह सरलतापूर्वक श्वास बाहर नहीं निकलता । जिस नासिका से सरलतापूर्वक श्वास बाहर निकलता हो , उस समय उसी नासिका का श्वास कहना चाहिये । किस नासिका से श्वास बाहर निकल रहा है , इतको पाठक उपर्युक्त प्रकार से समझ सकते है । क्रमशः अभ्यास होने पर बहुत आसानी से मालूम होने लगता है कि किस नासिका से निःश्वास प्रवाहित होत है । प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय से ढाई -ढाई घडी के हिसाब से एक -एक नासिका से श्वास चलता है । इस प्रकार रात -दिन में बारह बार बायीं और बारह बार दाहिनी नासिका से क्रमानुसार श्वास चलता है । किस दिन किस नासिका से पहले श्वास -क्रिया होती है , इसका एक निर्दिष्ट नियम है । यथा --
आदौ चन्द्रः सिते पक्षे भास्करस्तु सितेतरे ।
प्रतिपत्तो दिनान्याहुस्त्रिणि त्रीणि क्रमोदये ॥ (पवनविजयस्वरोदय )
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि तीन -तीन दिन की बारी से चन्द्र अर्थात् बायीं नासिका से तथा कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से तीन -तीन दिन की बारी से सूर्यनाडी अर्थात् दाहिनी नासिका से पहले श्वास प्रवाहित होता है । अर्थात् शुक्लपक्ष की प्रतिपदा , द्वितीया , तृतीया , सप्तमी , अष्टमी , नवमी , त्रयोदशी , चतुर्दशी , पूर्णिमा -इन नौ दिनों में प्रातःकाल सूर्योदय के समय पहले बायीं नासिका से तथा चतुर्थी , पञ्चमी , षष्ठी , दशमी , एकादशी , द्वादशी -इन छः दिनों को प्रातःकाल पहले दाहिनी नासिका से श्वास चलना आरम्भ होता है और वह ढाई घडो तक रहता है । उसके बाद दूसरी नासिका से श्वास जारी होता है । कृष्णपक्ष की प्रतिपदा , द्वितीया , तृतीया , सप्तमी , अष्टमी , नवमी , त्रयोदशी , चतुर्दशी , अमावास्या -इन नौ दिनों में सूर्योदय के समय पहले दाहिनी नासिका से तथा चतुर्थी , पञ्चमी , षष्ठी , दशमी , एकादशी , द्वादशी -इन छः दिनों में सूर्य के उदयकाल में पहले बायीं नासिका से श्वास आरम्भ होता है और ढाई घडी के बाद दूसरी नासिका से चलता है । इस प्रकार नियमपूर्वक ढाई -ढाई घडी तक एक -एक नासिका से श्वास चलता है । यही मनुष्य -जीवन में श्वास की गति का स्वाभविक नियम है ।
वहेत्तावद् घटीमध्ये पञ्चतत्त्वानि निर्दिशेत् । (स्वरशास्त्र )
प्रतिदिन रात -दिन की ६० घडियों में ढाई -ढाई घडी के हिसाब से एक -एक नासिका से निर्दिष्ट क्रम से श्वास चलने के समय क्रमशः पञ्चतत्त्वों का उदय होता है । इस श्वास -प्रश्वास की गति को समझकर कार्य करने पर शरीर स्वस्थ रहता है और मनुष्य दीर्घजीवी होता है , फलस्वरुप सांसारिक , वैषयिक -सब कार्यो में सफलता मिलने के कारण सुखपूर्वक संसार -यात्रा पूरी होती है ।
वाम नासिका (इडा नाडी ) खाआ श्वासफल
जिस समय इडा नाडी से अर्थात् बायीं नासिका से श्वास चलता हो , उस समय स्थिर कर्मो को करना चाहिये । जैसे - अलंकारधारण , दूर की यात्रा , आश्रम में प्रवेश , राजमन्दिर तथा महल बनाना एवं द्रव्यादि का ग्रहण करना । तालाब कुआँ आदि जलाशय तथा देवस्तम्भ आदि की प्रतिष्ठा करना । इसी समय यात्रा , दान , विवाह , नया कपडा पहनना , शान्तिकर्म , पौष्टिक कर्म , दिव्यौषर्धसेवन , रसायनकार्य , प्रभुदर्शन , मित्रतास्थापन एवं बाहर जाना आदि शुभ कार्य करना चाहिये । बायीं नाक से श्वास चलने के समय शुभ कार्य पर उन सब कार्यो में सिद्धि मिलती है । परंतु वायु , अग्नि और आकाश तत्त्व के उदय के समय उक्त कार्य नहीं करना चाहिये ।
दक्षिण नासिका (पिङुला नाडी ) का श्वासफल
जिस समय पिंगला नाडी अर्थात् दाहिनी नाक से श्वास चलता हो , उस समय कठिन कर्म करना चाहिये । जैसे ---कठिन क्रूर विद्या का अध्ययन और अध्यापन ,स्त्रेसंसर्ग , नौकदि आरोहण तान्त्रिकमतानुसार वीरमन्त्रदिसम्मत उपासना ,वैरी को दण्ड , शस्त्राभ्यास , गमन , पशुविक्रय , ईट , पत्थर , काठ तथा रत्नादि का घिसना और छीलना , संगीत अभ्यास , यन्त्र -तन्त्र बनाना , किले और पहाड पर चढना हाथी -घोडा तथा रथा आदि की सवारी सीखना व्यायाम षट्कर्मसाधन , यक्षिणी -बेताल , तथा भूतदिसाधन , औषध , सेवन , लिपि -लेखन ,दान ,क्रय -विक्रय , युद्ध , भोग , राजदर्शन , स्नानापार आदि।
दोनों नासिका (सुषुम्ना नाडी ) का श्वासफल
दोनों नासा छिद्रों से श्वास चलने के समय किसी प्रकार का शुभ या अशुभ कार्य नहीं करना चाहिये । उस समय कोई भी काम करने से वह निष्फल होगा । उस समय योगाभ्यास और ध्यानधारणादि के द्वारा केवल भगवान् को स्मरण करना उचित है । सुषुम्ना नाडी से श्वास चलने के समय किसी को भी शाप या वरप्रदान करने पर वह सफल होता नहीं है ।
इस प्रकार श्वास -प्रश्वास की गति जानकर , जत्त्वज्ञान के अनुसार , तिथि -नक्षत्र के अनुसार , ठीक -ठोक नियमपूर्वक सब कर्मो को करने पर आशाभङुजनित मनस्ताप आदि नहीं भोगना पडता ।
रोगोत्पत्ति का पूर्ण ज्ञान और उसका प्रतीकार
प्रतिपदा आदि तिथियों को यदि निश्चित नियम के विरुद्ध श्वास चले तो समझना चाहिये कि निस्संदेह कुछ अमङुल होगा । जैसे ,
१ . शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को सबेरे नींद टूटने पर सूर्योदय के समय पहले यदि दाहिनीं नाक से श्वास चलना आरम्भ हो तो उस दिन से पूर्णिमा तक के बीज गर्मी के कारण शरीर में कोई पीडा होगी और
२ . कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि को सूर्योदय के समय पहले बायीं नाक से श्वास चलना आरम्भ हो तो उस दिन से अमावस्या तक के अंदर कफ या सर्दि के कारण कोई पीडा होगी , इसमें संदेह नहीं ।
दो पखवाडों तक इसी प्रकार विपरीत ढंग से सूर्योदय के समय निःश्वास चलता रहे तो किसी आत्मीय स्वजन को भारी बीमारी होगी अथवा मृत्यु होगी या और किसी प्रकार की विपत्ति आयेगी । तीन पखवाडों से ऊपर लगातार गडबड होने पर निश्चय ही अपनी मृत्यु हो जायेगी ।
प्रतीकार --- शुक्ल अथवा कृष्णपक्ष की प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल यदि इस प्रकार विपरीत ढंग से निःश्वास चलने का पता लग जाय तो उस नासिका को कई दिनों तक बंद रखने से रोग उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं रहती । उस नासिका को इस तरह बंद रखना चाहिये , जिसमें उससे निःश्वास न चले । इस प्रकार कुछ दिनों तक दिन -रात निरन्तर (स्नान और भोजन का समय छोडकर ) नाक बंद रखने से उक्त तिथियों के भीतर बिलकुल ही कोई रोग नहीं होगा ।
यदि असावधानी के कारण निःश्वास में गडबडी हो और कोई रोग उत्प्न्न हो जाय तो जब तक रोग दूर न हो जाय , तब तक ऐसा करना चाहिये कि जिससे शुक्लपक्ष में दाहिनी और कृष्णपक्ष में बायीं नासिका से श्वास न चले । ऐसा करने से रोग शीघ्र दूर हो जायगा और यदि कोई भारी रोग होने की सम्भावना होगी तो वह भारी न होकर बहुत सामान्य रुप में होगा और फिर थोडे ही दिनों में दूर हो जायगा । ऐसा करने से न तो रोगजनित कष्ट भोगना पडेगा और न चिकित्सक को धन ही देना पडेगा ।
नासिका बन्द करने का नियम
नाक के छेद में घुस सके इतनी -सी पुरानी रुई लेकर उसकी गोल पोटली -सी बना ले और उसे साफ बारीक कपडे से लपेटकर सी ले । फिर इस पोटली को नाक के छिद्र में घुसाकर छिद्र को इस प्रकार बन्द कर दे जिसमें उस नाम से श्वास -प्रश्वास का कार्य बिल्कुल ही न हों । जिन लोगों को कोई शिरो रोग है अथवा जिनका मस्तक दुर्बल हो , उन्हें रुई से नाक बंद न कर , सिर्फ साफ पतले कपडे की पोटली बनाकर उसी से नाक बंद करनी चाहिये ।
किसी भी कारण से हो , जितने क्षण या जितने दिन नासिका बंद रखने की आवश्यकता हो उतने क्षण या उतने दिनों तक अधिक अरिश्रम का कार्य , धूम्रपान , जोर से चिल्लाना , दौडना आदि नहीं करना चाहिये । जब जिस -किसी कारण से नाक बन्द रखने की आवश्यकता हो , तभी इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिये । नयी अथवा बिना साफ की हुई मैली रुई नाक में कभी नहीं डालनी चाहिये ।
निःश्वास बदलने की विधि
कार्यभेद से तथा अन्यान्य अनेक कारणों से एक नासिका से दूसरी नासिका में वायु की गति बदलने की भी आवश्यकता हुआ करती है । कार्य के अनुकूल नासिका से श्वास चलना आरम्भ होने तक , उस कार्य को न करके चुपचाप बैठे रहना किसी के लिये भी सम्भव नहीं । अतएव अपनी इच्छानुसार श्वास की गति बदलने की क्रिया सीख लेना नितान्त आवश्यक है । इसकी क्रिया अत्य्न्त सहज है , सामान्य चेष्टा से ही श्वास की गति बदली जा सकती है ।
१ . जिस नासिका से श्वास चलता हो , उसके विपरीत दूसरी नासिका को अँगूठे से दबा देना चाहिये और जिससे श्वास चलता हो उसके द्वारा वायु खींचना चाहिये । फिर उसको दबाकर दूसरी नासिका से वायु को निकालना चाहिये । कुछ देर तक इसी तरह एक से श्वास लेकर दूसरी से निकालते रहने से अवश्य श्वास की गति बदल जायगी ।
२ . जिस नासिका से श्वास चलता हो उसी करवट सोकर यह क्रिया करने से बहुत जल्द श्वास की गति बदल जाती है और दूसरी नासिका में श्वास प्रवाहित होने लगता है । इस क्रिया के बिना भी जिस नाक से श्वास चलता है , केवल उस करवट कुछ समय तक सोये रहने से भी श्वास की गति पलट जाती है ।
इस प्रकार जो अपनी इच्छानुसार वायु को रोक सकता है और निकाल सकता है वही पवन पर विजय प्राप्त करता है ।
15….संक्षिप्त विवरण - बिना औषध के रोगनिवारण
बिना औषध के रोगनिवारण
अनियमित क्रिया के कारण जिस तरह मानव -देह में रोग उत्पन्न होते हैं , उसी तरह औषध के बिना ही भीतरी क्रियाओं के द्वारा नीरोग होने के उपाय भगवान् के बनाये हुए हैं । हमलोग उस भगवत्प्रदत्त सहज कौशल को नहीं जानते , इसी कारण दीर्घकाल तक रोग का दुःख भोगते रहते है । यहाँ रोगों के निदान के लिय स्वरशास्त्रोक्त कुछ यौगिक उपायों का उल्लेख किया गया है । इनके प्रयोग से विशेष लाभ हो सकता है ---
१ . ज्वर में स्वर परिवर्तन --- ज्वर का आक्रमण होने पर अथवा आक्रमण की आशङ्का होने पर जिस नासिका से श्वास चलता हो , उस नासिका को बंद कर देना चाहिये । जब तक ज्वर न उतरे और शरीर स्वस्थ न हो जाय , तब तक उस नासिका को बंद ही रखना चाहिये । ऐसा करने से दस -पंद्रह दिनों में उतरने वाला ज्वर पाँच ही सात दिनों में अवश्य ही उतर जायगा। ज्वरकाल में मन -ही -मन सदा चाँदी के समान श्वेत वर्ण का ध्यान करने से और भी शीघ्र लाभ होता है । सिन्दुवार की जड रोगी के हाथ में बाँध देने से सब प्रकार के सब प्रकार के ज्वर निश्चय ही दूर हो जाते हैं ।
अँतरिया ज्वर --- श्वेत अपराजिता अथवा पलाश के कुछ पत्तों को हाथ से मलकर , कपडे से लपेटकर एक पोटली बना लेनी चाहिये और जिस दिन ज्वर की बारी हो उस दिन सबेरे से ही उसे सूँघते रहना चाहिये । अँतरिया ज्वर बंद हो जायगा ।
२ . सिरदर्द में स्वर परिवर्तन --- सिरदर्द होने पर दोनों हाथों की केहुने के ऊपर धोती के किनारे अथवा रस्सी से खूब कसकर बाँध देना चाहिये । इससे पाँच -सात मिनट में ही सिरदर्द जाता रहेगा । केहुनी पर इतने जोर से बाँधना चाहिये कि रोगी को हाथ में अत्यन्त दर्द मालूम हो । सिरदर्द अच्छा होते ही बाँहे खोल देनी चाहिये ।
एक दूसरे प्रकार का सिरदर्द होता है , जिसे साधारणतः ‘अधकपाली ’ या ‘आधासीसी ’ कहते हैं । कपाल के मध्य से बायीं या दाहिने ओर आधे कपाल और मस्तक में अत्यन्त पीडा मालूम होती है । प्रायः यह पीडा सूर्योदय के समय आरम्भ होती है और दिन चढने के साथ -साथ यह भी बढती जाती है । दोपहर के बाद घटनी शुरु होती है और शाम तक प्रायः नहीं ही रहती । इस रो ग का आक्रमण होने पर जिस तरफ के कपाल में दर्द हो , ऊपर लिख -अनुसार उसी तरफ की केहुनी के ऊपर जोर से रस्सी बाँध देनी चाहिये । थोडी ही देर में दर्द शान्त हो जायगा और रोग जाता रहेगा । दूसरे दिन यदि फिर दर्द शुरु हो और रोज एक ही नासिका से श्वास चलते समय शुरु होता हो तो सिरदर्द मालूम होते ही उस नाक को बंद कर देना चाहिये और हाथ को भी बाँध रखना चाहिये । ‘अद्धकपाली ’ सिरदर्द में इस क्रिया से होने वाले आश्चर्यजनक फल को देखकर साधक चकित रह जाते है ।
शिरः पीडा --- शिरः पीडाग्रस्त रोगी को प्रातःकाल शय्या से उठते ही नासापुठ से शीतल जल पीना चाहिये । इससे मस्तिष्क शीतल रहेगा , सिर भारी नहीं होगा और सर्दी नहीं लगेगी । यह क्रिया विशेष कठिन भी नहीं है । एक बरतन में ठंडा जल भरकर उसमें नाक डुबाकर धीरे -धीरे गले भीतर जल खींचना चाहिये । क्रमशः अभ्यास से यह क्रिया सहज हो जायगी । शिरःपीडा होने पर चिकित्सक रोगी के आरोग्य होने की आशा छोड देता है , रोगी को भी भीषण कष्ट होता है , परंतु इस उपाय से काम लेने पर निश्चय ही आशातील लाभ पहुँचता है ।
३ . उदरामय , अजीर्णादि में स्वर परिवर्तन --- भोजन , जलपान आदि जब जो कुछ खाना हो वह दाहिनी नाक से श्वास चलते समय खाना चाहिये । प्रतिदिन इस नियम से आहार करने से वह बहुत आसानी से पच जायगा और कभी अजीर्ण का रोग नहीं होगा । जो लोग इस रोग से कष्ट पा रहे हैं , वे भी यदि इस नियम के अनुसार रोज भोजन करें तो खाए पदार्थ पच जायेगें और धीरे -धीरे उनका रोग दूर हो जायगा । भोजन के बाद थोडी देर बायीं करवट सोना चाहिये । जिन्हें समय न हो उन्हें ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे भोजन के बाद दस -पंद्रह मिनट तक दाहिनी नाक से श्वास चले अर्थात् पूर्वोक्त नियम के अनुसार रुई द्वारा बायीं नाक बंद कर देनी चाहिये । गुरुपाक (भारी ) भोजन होने पर भी इस नियम से वह शीघ्र पच जाता है ।
यौगिक उपाय
स्थिरता के साथ बैठकर एकटक नाभिमण्डल में दृष्टि जमाकर नाभिकन्द का ध्यान करने से एक सप्ताह में उदरामय रोग दूर हो जाता है । श्वास रोककर नाभि को खींचकर नाभि की ग्रन्थि को एक सौ बार मेरुदण्ड से मिलाने से आमादि उदरामयजनित सब तरह की पीडाएँ दूर हो जाती हैं और जठराग्नि तथा पाचनशक्ति बढ जाती है ।
१ . प्लीहा --- रात को बिछौने पर सोकर और सबेरे शय्या -त्याग के समय हाथ और पैरों को सिकोडकर छोड देना चाहिये । फिर कभी इस करवट कभी उस करवट टेढा -मेढा शरीर करके सारे शरीर को सिकोडना और फैलाना चाहिये । प्रतिदिन चार -पाँच मिनट ऐसा करने से प्लीहा -यकृत् (तिल्ली , लीवर ) रोग दूर हो जायगा । सर्वदा इसका अभ्यास करने से प्लीहा -यकृत् रोग की पीडा कभी नहीं भोगनी पडेगी ।
२ . दन्तरोग --- प्रतिदिन जितनी बार मल -मूत्र का त्याग करे , उतनी बार दाँतो की दोनों पंक्तियों को मिलाकर जरा जोर से दबाये रखे । जब तक मल या मूत्र निकलता रहे तब तक दाँतो से दाँत मिलाकर इस प्रकार दबाये रहना चाहिये । दो -चार दिन ऐसा करने से कमजोर दाँतो की जड मजबूत हो जायगी । सदा इसका अभ्यास करने से दन्तमूल दृढ हो जाता है और दाँत दीर्घ कल तक देते हैं तथा दाँतो में किसी प्रकार की बीमारी होने का कोई डर नहीं रहता ।
३ . स्नायविक वेदना --- छाती , पीठ या बगल में ---चाहे जिस स्थान में स्नायविक वेदना या अन्य किसी प्रकार की वेदना हो , वेदना मालूम होते ही जिस नासिका से श्वास चलता हो उसे बंद कर देना चाहिये , दो -चार मिनट बाद अवश्य ही वेदना शान्त हो जायगी ।
४ . दमा या श्वासरोग --- जब दमें का जोर का दौरा हो तब जिस नासिका से निःश्वास चलता हो , उसे बंद करके दूसरी नासिका से श्वास चला देना चाहिये । दस -पंद्रह मिनट में दमे का जोर कम हो जायगा । प्रतिदिन इस प्रकार करने से महीने भर में पीडा शान्त हो जायेगी । दिन में जितने ही अधिक समय तक यह क्रिया की जायगी , उतना ही शीघ्र रह रोग होगा । दमा के समान कष्टदायक कोई रोग नहीं , दमा का जोर होने पर यह क्रिया करने से बिना किसी दवा के बीमारी अच्छी हो जाती है ।
५ . वात --- प्रतिदिन भोजन के बाद कंघी से सिर वाहना चाहिये । कंघी इस प्रकार चलानी चाहिये जिसमें उसके काँटे सिर को स्पर्श करें । उसके बाद वीरासन लगाकर अर्थात् दोनों पैर पीछे की ओर मोडकर उनके ऊपर दबाकर १५ मिनट बैठना चाहिये । प्रतिदिन दोनों समय भोजन के बाद इस प्रकार बैठने से कितना भी पुराना वात क्यों न हो , निश्चय ही अच्छा हो जायगा । अगर स्वस्थ आदमी इस नियम का पालन करे तो उसके वातरोग होने की कोई आशङ्का नहीं रहेगी । कहना न होगा कि रबड की कंघी का व्यवहार नहीम करना चाहिये ।
६ . नेत्ररोग --- प्रतिदिन सबेरे बिछौने से उठते ही सबसे पहले मुँह में जितना पानी भरा जा सके , उतना भरकर दूसरे जल से आँखो को बीस बार झपटा मारकर धोना चाहिये । प्रतिदिन दोनों समय भोजन के बाद हाथ -मुँह धोते समय कम -से -कम सात बार आँखो में जल का झपटा देना चाहिये । जितनी बार मुँह में जल डाले , उतनी बार आँखे और मुँह को धोना न भूले । प्रतिदिन स्नान के वक्त तेल मालिश करते समय सबसे पहले दोनों पैरों के अँगूठों के नखों को तेल से भर देना चाहिये और फिर तेल लगाना चाहिये ।
ये कुछ नियम नेत्रों के लिये विशेष लाभदायक हैं । दृष्टिशक्ति सतेज होती है । आँखे स्निग्ध रहती है और आँखों में कोई बीमारी होने की सम्भावना नहीं रहती । नेत्र मनुष्य के परम धन हैं । अतएव प्रतिदिन नियम -पालन में कभी आलस्य नहीं करना चाहिये ।
16…संक्षिप्त विवरण - हठयोग के षट्कर्म
हठयोग के षट्कर्म
रुद्रयामल के चौंतीसर्वें और पैंतीसवें पटल में नेती , दन्ती , धौती , नेऊली और क्षालन -इन पञ्च स्वर योगों को कहा गया है । हठयोग प्रदीपिका में इन्हीं का विस्तार हैं । अतः उन्हें वहीं से लेकर यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है ।
इस परिदृश्यमान चराचर विश्व प्रपञ्च का उपादान कारण प्रकृति है । मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक होने से प्राणिमात्र के शरीर वात , पित्त , कफ ---इन त्रिधातुओं के नाना प्रकार के रुपान्तरों के सम्मिश्रण हैं । अतः अनेक शरीर वातप्रधान , अनेक पित्तप्रधान और अनेक कफप्रधान होते हैं । वातप्रधान शरीरों में आहार -विहार के दोष से तथा देश -कालादि हेतु से प्रायः वातवृद्धि हो जाती है । पित्तप्रधान शरीरों में पित्तविकृति और कफोल्वण शरीरों में प्रायः कफ -प्रकोप हो जाता है । कफ -धातु के विकृत होन पर दूषित श्लेष्म , आमवृद्धि या मेद का संग्रह हो जाता है । पश्चात् इन मलों के प्रकुपित होन से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं । इन व्याधियों को उत्पन्न न होने देने के लिये और यदि हो गये तो उन्हें दूर करके पुनः देह को पूर्ववत स्वस्थ बनाने के लिये जैसे आयुर्वेद के प्राचीन आचार्यो ने स्नेहपान , स्वेदन , वमन , विरेचन और वस्ति -ये पञ्चकर्म कहे हैं , वैसे ही हठयोग प्रवर्तक महर्षियों ने साधकों के कफप्रधान शरीर की शुद्धि के लिये षट्कर्म निश्चित किये हैं । ये षट्कर्म सब साधकों को करने ही चाहिये , ऐसा आग्रह नहीं है ।
हठयोग के ग्रन्थों में षट्कर्म के कर्तव्याकर्तव्यपर विचार किया गया है । हठयोग के षट्कर्म से जो लाभ होते हैं , वे लाभ प्राणायाम से भी प्राप्त होते हैं । अन्तर केवल समय का है । परन्तु जिस घर में गंदगी इतनी फैल गयी हो कि साधारण झाडू से न हटायी जा सके , उसमें कुदाल और टोकरी की आवश्यकता आ पडेगी । इसी प्रकार शरीर के एकत्रित मल को शीघ्र हटाने के लिये षट्कर्म की आवश्यकता है । इसी कारण ---
मेदः श्लेष्माधिकः पूर्व षट् कर्माणि समाचरेत् ।
अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः ॥ (हठयोगप्रदीपिका )
अर्थात् जिस पुरुष के मेद और श्लेष्मा , अधिक हों वह पुरुष प्राणायाम के पहले इन छः कर्मो को करे और इनके न होने से दोषों की समानता के कारण न करे । इतना ही नहीं , योगीन्द्र स्वात्माराम कारण न करे । इतनी ही नहीं , योगीन्द्र स्वात्माराम आगे चलकर षट्कर्मो को ‘घटशोधनकारकम् ’ अर्थात् देह को शुद्ध करने वाले और ‘विचित्रगुणसंधायि ’ अर्थात् विचित्र गुणों का संधान करने वाले भी कहते हैं ।
यह बात सत्य है कि षट्कर्मो के बिना ही पहले योगसाधन किया जाता था । समय और अनुभव ने दिखाया कि प्राणायाम से जितने समय में मल दूर किया जाता था , उसमें कम समय में षट्कर्मों द्वारा मल दूर किया जा सकता है । इन कर्मो की उन्नति होती गयी और छः से ये कर्म दस हो गये । पीछे गुरुस्परम्परा से प्राप्त गुप्तविद्या लुप्त होने लगीं । तब यो ये कर्म पूरे हुए षट्कर्म तक ही परिमित रह गये । इन षट्कर्मो से लाभ है , इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । यह बात दूसरी है कि सबकी इधर प्रवृत्ति न हो और सब इन्हें न कर सकते हों ।
एक बात और है । वर्तमान समय में अनेक योगाभ्यासी मूल उद्देश्य को न समझने के कारण शरीर में त्रिधातु सम होने पर भी नित्य षट्कर्म करते रहते हैं और अपने शिष्यों को भी जीवनपर्यन्त नियमित रिति से करते रहने का उपदेश देते हैं । यदि शरीरशुद्धि के लिये अथवा इन क्रियाओं पर अपना अधिकार रखने के लिये प्रारम्भ में सिखाया जाय तो कोई आपत्ति नहीं । कारण , भविष्य में कदाचित् देश -कालपरिवर्तन , प्रमाद या आहार -विहार में भूल से वातादि धातु विकृत हो जायँ तो शीघ्र क्रिया द्वारा उनका शमन किया जा सकता है । परंतु आवश्यकता न होने पर भी नित्य करते रहने से समय का अपव्यय , शारीरिक निर्बलता और मानसिक प्रगति में शिथिलता आ जाती है ।
षट्कर्म के नाम --- ‘हठयोगप्रदीपिका ’ ग्रन्थ के कर्ता स्वात्माराम योगी ने १ . धौति , २ . वस्ति , ३ . नेति , ४ .नैलि , ५ .कपालभाति और ६ .त्राटक को षट्कर्म कहा है । आगे चलकर गजकरणी का भी वर्णन किया है । परन्तु हिन्दी में ‘भक्तिसागर ’ ग्रन्थ के रचयिता चरणदास ने १ .नेति , २ .धौति , ३ .वस्ति , ४ .गजकर्म , ५न्योली और ६ .त्राटक को षट्कर्म कहा है । फिर १ . कपालभाति , २ . र्धौकनी , ३ . बाघी और ४ . शंखपषाल -इन चार कर्मो का नाम लेकर उन्हें षट्कर्मो के अन्तर्गत कर दिया है । दोनों में गजकर्म और कपालभाति को षट्कर्म के अंदर रखने में अन्तर पडता है । चूँकि ये षट्कर्म के शाखमात्र है अतएव इस विभेद क कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता ।
षट्कर्म में नियम --- षट्कर्म -साधक को हठयोग में दर्शाये हुए स्थान , भोजन , आचार -विचार आदि नियमों को मानना परमावश्यक है । यहाँ यही कहा जा सकता है कि स्थान रमणीक और निरापद , भोजन सात्त्विक तथा परिमित होना चाहिये । एकान्तसेवन , कम बोलना , वैराग्य , साहस , इत्यादि वातें आचार -विचार से समझनी चाहिये ।
१ . नौलि (=नौलिक , नलक्रिया या न्योली )
अमन्दावर्त्तवेगेन तुन्दं सव्यापसव्यतः ।
नतांसो भ्रामयेदेषा नौलिः सिद्धैः प्रचक्ष्यते ॥ (हठयोगप्रदीपिका )
अर्थात् कन्धों को नवाये हुए अत्यन्त वेग के साथ , जलभ्रमर के समान अपनी तुन्द को दक्षिण -वाम भागों से भ्रमाने को सिद्धों ने नौलि -कर्म कहा है ।
पद्मासन (सिद्धासन या उत्कटासन ) लगाकर , जब शौच , स्नान , प्रातःसन्ध्या आदि से निवृत्त हो लिये हों और पेट साफ तथा हल्का हो गया हो , तब रेचक कर वायु को बाहर रोककर बिना देह हिलाये , केवल मनोबल से पेट को दायें से बायें और बायें से दायें चलाना सोचे और तदनुकूल प्रयास करे । इसी प्रकार सायं -प्रातः स्वेद आने पर्यन्त प्रतिदिन अभ्यास करते -करते पेंट की स्थूलता जाती रहती है । तदनन्तर यह सोचना चाहिये कि दोनों कुक्षियाँ दब गयीं और बीच में दोनों रहती है । तदनन्तर यह सोचना चाहिये कि दोनों कुक्षियाँ दब गयीं और बीच में दोनों ओर से दो नल जुटकर मूलाधार से ह्रदय तक गोलाकार खम्भ खडा हो गया । यही खम्भा जब बँध जाय तब नौलि सुगम हो जाती है । मनोबल और प्रयासपूर्वक अभ्यास बढाने से दायें -बायें घूमने लगती हैं । इसी को चलाने में छाती के समीप , कण्ठ पर और ललाट पर भी नाडियों का द्वन्द्व मालूम पडता है । एक बार न्योली चल जाने पर चलती रहती है । पहले -पहले चलने के समय दस्त ढीला होता है । जिसका पेट हल्का है तथा जो प्रयासपूर्वक अभ्यास करता है उसको एक महीने के भीतर ही न्योली सिद्ध हो जायगी ।
इस क्रिया का आरम्भ करने से पहले पश्चिमोत्तानासन और मयूरासन का थोडा अभ्यास कर लिया हो तो यह क्रिया शीध्र सिद्ध हो जाती है । जब तक आँत पीठ के अवयवों से भलीभाँति पृथक् न हो तब तक उठाने की क्रिया सावधानी के साथ करे , अन्यथा आँते निर्बल हो जायँगी । किसी -किसी समय आघात पहुँचकर उदर रोग , शोथ , आमवात , कटिवात , गृध्रसी , कुब्जवात , शुक्रदोष या अन्य कोई रोग हो जाता है । अतः इस क्रिया को शान्तिपूर्वक करना चाहिये । अँतडी में शोथ , क्षतादि दोष या पित्तप्रकोपजनित अतिसारप्रवाहिका (पेचिश ), संग्रहणी आदि रोगों में नौलि -क्रिया हानिकारक है ।
मन्दाग्निसंदीपनपाचनादि संधापिकानन्दकरी सदैव ।
अशेषदोषामयशोषणी च हठक्रियामौलिरियं च नौलिः ॥
( हठयोगप्रदीपिका )
यह नौलि मन्दग्नि का भली प्रकार दीपन और अन्नादि का पाचन और सर्वदा आनन्द करती है तथा समस्त वात आदि दोष और रोग का शोषण करती है । यह नौली हठयोग की सारी क्रियाओं में उत्तम है ।
अँतडियो के नौलि के वश होने से पाचन और मल का बाहर होना स्वाभाविक नौलि करते समय साँस की क्रिया तो रुक ही जाती है । नौलि कर चुकने पर कण्ठ के समीप एक सुन्दर अकथनीय स्वाद मिलता है । यह हठयोग की सारी क्रियाओं से श्रेष्ठ इसलिये है कि नौलि जान जाने पर तीनों बन्ध सुगम हो जाते हैं । अतएव यह प्राणायाम की सीढी है । धौति , वस्ति में भी नौलि की आवश्यकता होती है । शंखपषाली क्रिया में भी , जिसमें मुख से जल ले अँतडियों में घुमाते हुए पायु -द्वारा ठीक उसी प्रकार निकाल दिया जाता हैं जैसे शंख में एक ओर से जल देनें पर घूमकर जल दूसरी राह से निकल जाता है , नौलि सहायक है ।
२ . वस्तिकर्म ---
वस्ति मूलाधार के समीप है । रंग लाल है और इसके देवता गणेश हैं । वस्ति को साफ करने वाले कर्म को ‘वस्तिकर्म ’ कहते हैं । ‘योगसार ’ पुस्तक में पुराने गुड , त्रिफला और चीते की छाल के रस से बनी गोली देकर अपानवायु को वश में करने को कहा हैं । फिर वस्तिकर्म का अभ्यास करना कहा है ।
वस्तिकर्म दो प्रकार का है । १ . पवनवस्ति , २ . जलवस्ति । नौलिकर्म द्वारा अपानवायु को ऊपर खींच पुनः मयूरासन से त्यागने को ‘वस्तिकर्म ’ कहते हैं । पवनवस्ति पूरी सध जाने पर जलवस्ति सुगम हो जाती है , क्योंकि जल को खींचने का कारण पवन ही होता है । जब जल में डूबे हुए पेट से न्योली जाय तब नौलि से जल ऊपर खिंच जायगा ।
नाभिदघ्नजले पायौ न्यस्तनालोत्कटासनः ।
आधाराकुञ्चनं कुर्यात् क्षालनं वस्तिकर्म तत् ॥ (हठयोगप्रदीपिका )
अर्थात् गुदा के मध्य में छः अंगुल लम्बी बाँस की नली को रखे , जिसका छिद्र कनिष्ठिका अँगुली के प्रवेश योग्य हो , उसे घी अथवा तेल लगाकर सावधानी के साथ चार अंगुल गुदा में प्रवेश करे और दो अंगुल बाहर रखे । पश्चात् बैठने पर नाभि तक जल आ जाय , इतने जल से भरे हुए टब मे उत्कटासन से बैठे अर्थात् दोनों पार्ष्णियों (पैर की एडियों ) को मिलाकर खडी रखकर उन पर अपने स्फिच (नितम्बों ) को रखे और पैरों के अग्रभाग पर बैठे और उक्त आसन से बैठकर आधारकुञ्चन करे जिसमे बृहद् अन्त्र मे अपने -आप जल चढने लगेगा । बाद में भीतर प्रविष्ट हुए जल को नौलि क्रम से चला कर त्याग दे । इस जल के साथ अन्त्रस्थित मल , आँव , कृमि , अन्त्रोत्पन्न सेन्द्रियविष आदि बाहर निकल आते हैं । इस उदर के क्षालन (धोने ) को वस्तिकर्म कहते है ।
नियम --- धौति , वस्ति दोनों कर्म भोजन से पूर्व ही करने चाहिये और इनके करने के अनन्तर हलका भोजन शीघ्र कर लेना चाहिये , उसमें विलम्ब नहीं करना चाहिये । वस्तिक्रिया करने से जल का कुछ अंश बृहद् अन्त्र में शेष रह जाता है , वह धीरे -धीरे मूत्राद्वार बाहर आयेगा । यदि भोजन नहीं किया जायगा तो वह दूषित जल अन्त्रों से सम्बद्ध सूक्ष्म नाडियों द्वारा शोषित होकर रक्त में मिल जायगा । कुछ लोग पहले मूलाधार से प्राणवायु के आकर्षण का अभ्यास करके और जल में स्थित होकर गुदा में नालप्रवेश के बिना ही वस्तिकर्म का अभ्यास करते हैं । उस प्रकार वस्तिकर्म करने से उदर में प्रविष्ट हुआ सम्पूर्ण जल बाहर नहीं आ सकता और उसके न आने से धातुक्षय आदि नाना दोष होते हैं । इससे उस प्रकार वस्तिकर्म नहीं करना चाहिये , अन्यथा ‘न्यस्तनालः ’ (अप्नी गुदा में नाल रखकर ) ऐसा पद स्वात्माराम क्यों देते ? यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि छोटे -छोटे जलजन्तुओं का नलद्वारा पेट में प्रविष्ट हो जाने का भय रहता है । अतएव नल के मुख पर महीन वस्त्र देकर करना चाहिये ।
वस्तिकर्म में मूलाधार के पीडित और प्रक्षालित होने से लिङु और गुदो के रोगों का नाश होना स्वाभाविक है ।
गुल्मप्लीहोदरं चापि वातपित्तकफोदभवाः ।
वस्तिकर्मप्रभावेन क्षीयन्ते सकलामयाः ॥ (हठयोगप्रदीपिका )
अर्थात वस्तिकर्म के प्रभाव से गुल्म , प्लीहा ,उदर (जलोदर )और वात , पित्त , कफ , इनके द्वन्द्व वा एक से उत्पन्न हुए सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं ।
धात्विन्दियान्तःकरणप्रसादं दद्याच्च कान्तिं दहनप्रदीप्तिम् ।
अशेषदोषोपचयं निहन्यादभ्यस्यमानं जलवस्तिकर्म ॥ (हठयोगप्रदीपिका )
अभ्यास किया हुआ यह वस्तिकर्म साधक के सप्त धातुओं , द्स इन्द्रियों और अन्तःकरण को प्रसन्न करता है । मुख्ज पर सात्त्विक कान्ति छा जाती है । जठराग्नि उद्दीप्त होती है । वात , पित्त , कफ , आदि दोषों की वृद्धि और न्यूनता दोनों को नष्ट कर साधक साम्यरुप आरोग्यता को प्राप्त करता है । एक बात इस सम्बन्ध में अवश्य ध्यान देने की है कि वस्ति क्रिया करनेवालों को पहले नेति और धौतिक्रिया करनी ही चाहिये , जिसका वर्णन नीचे दिया जाता है । अन्य क्रियाओं के लिये ऐसा नियम नहीं है ।
राजयक्ष्मा (क्षय ), संग्रहणी , प्रवाहिका , अधोरक्तपित्त , भगंदर , मलाशय और गुदा में शोथ , संततज्वर , आन्त्रसंनिपात , आन्त्रशोथ , आन्त्रव्रण एवं कफवृद्धि जनित तीक्ष्ण श्वासप्रकोप इत्यादि रोगों में वस्तिक्रिया नहीं करनी चाहिये ।
यह वस्तिक्रिया भी प्राणायाम का अभ्यास चालू होने के बाद नित्य करने की नहीं है । नित्य करने से आन्त्रशक्ति परावलम्बिनी और निर्बल हो जायगी , जिससे बिना वस्तिक्रिया के भविष्य में मलशुद्धि नहीं होगी । जैसे तम्बाकू और चाय के व्यसनी को तम्बाकू और चाय लिये बिना शौच नहीं होताम , वैसे नित्य वस्तिकर्म अथवा षटकर्म करने वाले की स्वाभाविक आन्तरिक शक्ति के बल से शरीरशुद्धि नहीं होती ।
३ . धौतिकर्म ---
चतुरङुलविस्तारं हस्तपञ्चदशायतम् ।
गुरुपदिष्टमार्गेण सिक्त्म वस्त्रं शनैर्ग्रसेत् ॥
पुनः प्रत्याहरेच्चैतदुदितं धौतिकर्म तत् ॥ (हठयोगप्रदीपिका )
अर्थात् चार अंगुल चौडे और पंद्रह हाथ लंबे महीन वस्त्र को गरम जल में भिगोकर थोडा निचोड ले। फिर गुरुपदिष्टे मार्ग से धीरे -धीरे प्रतिदिन एक -एक हाथ का अभ्यास हो सकता है । करीब एक हाथ कपडा बाहर रहने दिया जाय । मुख में जो वस्त्र प्रान्त रहे उसे दाढो से भली प्रकार दबा नौलिकर्म करे । फिर धीरे -धीरे वस्त्र निकाले । यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि वस्त्र निगलने के पहले पूरा जल पी लेना चाहिये । इससे कपडे के निगलने में सुभीता तथा कफ -पित्त का उसमें सटना आसान हो जाता है कपडे को बाहर निकलने में भी सहायता मिलती है । धौति को रोज स्वच्छ रखना चाहिये । अन्यथा धौति में लगे हुए दूषित कफरुप विजातीय द्रव्य के परमाणु पुनः दूसरे दिन भीतर जाकर हानि पहुँचायेंगे ।
पाश्चात्यों ने स्टमक ट्यूब बनाया है । कोई एक सवा हाथ की रबर के नली रहती है , जिसका एक मुख खुला रहता है और दूसरे सिरे के कुछ ऊपर हटकर बगल में एक छेद होता है । जल पीकर खुला सिरा ऊपर रखकर दूसरा सिरा निगला जाता है और जल रबर की नलिका द्वारा गिर जाता है ।
चाहे किसी प्रकार की धौति क्यों न हो , उससे , कफ , पित्त और रंग -बिरंगे पदार्थ बाहर गिरते है । ऊपर की नाडी में रहा हुआ एकाध अन्न का दाना भी गिरता है । दाँत खट्टा -सा जाता है । परंतु मन शान्त और प्रसन्न हो जाता है । वसन्त या ग्रीष्मकाल में इसका साधन अच्छा होता है ।
घटिका , कण्ठनलिका या श्वासनलिका में शोथ , शुष्क , काश , हिक्का , वमन , आमाशय में शोथ , ग्रहणी , तीक्ष्ण अतिसार , ऊर्ध्व रक्तिपित्त (मुँह से रक्त गिरना ) इत्यादि कोई रोग हो तब धौतिक्रिया लाभदायक नहीं होती ।
४ .नेतिकर्म ---
नेति दो प्रकार की होती है - जलनेति और सूत्रनेति । पहले जलनेति करनी चाहिये । प्रातःकाल दन्तधावन के पश्चात् जो साँस चलते हो , उसी से चुल्लू में जल ले और दूसरी साँस बंदकर जल नाक द्वारा खींचे । जल मुख में चला जायगा । सिर के पिछले सारे हिस्से मे , जहाँ मस्तिष्क का स्थान हैं , उस कर्म के प्रभाव से गुदगुदाहट और सनसनाहट या गिनगिनाहट पैदा होगी । अभ्यास बढने पर आगे ऐसा नहीं होगा । कुछ लोग नासिका के एक छिद्र से जल खींचकर दूसरे छिद्र से निकालने की क्रिया को ‘जलनेति ’ कहते हैं । एक समय में आध सेर से एक सेर तक जल एक नासापुट से चढाकर दूसरे नासापुट से निकाला जा सकता है एक समय एक तरफ से जल चढा कर दूसरे समय दूसरी तरफ से चढाना चाहिये ।
जलनेति से नेत्रज्योति बलवान होती है । स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिये भी हितकर है । तीक्ष्ण नेत्ररोग , तीक्ष्ण अम्लपित्त और नये ज्वर में जलनेति नहीं करनी चाहिये । अनेक मनुष्य रोज सुबह नासापुट से जल पीते है । यह क्रिया हितकर नहीं है । कारण , जो दोष नासिका में संचित होंगे वे आमाशय में चले जायँगे । अतः उषःपान तो मुँह से ही करना चाहिये ।
नियम - घर्षणनेति --- जलनेति के अनन्तर सूत्र लेना चाहिये । महीन सूत की दस -पन्द्रह तार की एक हाथ लंबी बिना बटी डोर , जिसका छःसात इंच लम्बा इक प्रान्त बटकर क्रमशः पतला बना दिया गया हो , पिघले हुए मोम से चिकना बनाकर जल में भिगो लेना उचित है । फिर इस स्निग्ध भाग को इस रीति से थोडा मोडकर जिस छिद्र से वायु चलती हो उस छिद्र में लगाकर और नाक का दूसरा छेद अँगुली से बन्दकर , खूब जोर से बारंबार पूरक करने से सूत का भाग मुख में आ जाता है । तब उसे तर्जनी और अङुष्ठ से पकडकर बाहर निकाले ले । पुनः नेति को धोकर दूसरे छिद्र में डालकर मुँह में से निकाल ले । कुछ दिन के अभ्यास के बाद एक हाथ से सूत को मुख से खींचकर और दूसरे से नाक वाल प्रान्त पकडकर धीरे -धीरे चालन करे । इस क्रिया को ‘घर्षणनेति ’ कहते हैं । इस प्रकार नाक के दूसरे रन्ध्र से भी , जब वायु उस रन्ध्र से चल रहा हो , अभ्यास करे । इससे भीतर लगा हुआ कफ पृथक् होकर नेति के साथ बाहर आ जाता है । नाक के एक छिद्र से दूसरे छिद्र में भी सूत चलाया जाता है , यद्यपि कुछ लोग इसे दोषयुक्त मानकर इसकी उपेक्षा करते हैं । उसका क्रम यह है कि सूत नाक के एक छिद्र से पूरक द्वारा जब खींचा जाता है , तो रेचक मुखा द्वारा न कर दूसरे रन्ध्र द्वारा करना चाहिये । इस प्रकार सूत एक छिद्र से दूसरे छिद्र में आ जाता है । इस क्रिया के करने में किसी प्रकार का भय नहीं है । सध जाने पर तीसरे दिन करना चाहिये । जलनेति प्रतिदिन कर सकते हैं । नेति डालने में किसी -किसी को छींक आने लगाती हैं , इसालिये एक -दो सेकेण्ड श्वासोच्छ्वास की क्रिया को बन्द करके नेति डालनी चाहिये ।
कपालशोधिनी चैव दिव्यदृष्टिप्रदायिनी ।
जत्रूर्ध्वजातरोगौघं नेतिराशु निहन्ति च ॥ (हठयोगप्रदीपिका )
‘ नेति कपाल को शुद्ध करती है , दिव्य दृष्टि देती है , स्कन्ध , भुजा और सिर की सन्धि के ऊपर के सारे रोगों को नेति शीघ्र नष्ट करती है । ’
त्राटककर्म ---
‘ समाहित अर्थात् एकाग्रचित्त हुआ मनुंष्य निश्चल दृष्टि से सूक्ष्म लक्ष्य को अर्थात् लघु पदार्थ को तब तक देखे जब तक अश्रुपात न होवे । इसे मत्स्येन्द्र आदि आचार्यो ने ‘ त्राटककर्म ’ कहा है । ’
सफेद दिवाल पर सरसों -बराबर काला चिह्र कर दे उसी पर दृष्टी ठहराते -ठहराते चित्त समाहित होता हैं , और दृष्टि शक्तिसम्पत्र हो जाती है । मैस्मेरिज्म में जो शक्ति आ जाती है वही शक्ति त्राटक से भी प्राप्य है ।
‘ त्राटक नेत्ररोगनाशक है । तन्द्रा - आलस्यादि को भीतर नहीं आने देता । त्राटककर्म संसार में इस प्रकार गुप्त रखने योग्य है जैसे सुवर्ण की पेटी संसार में गुप्त रखी जाती है क्योंकि - ‘ भवेद्वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता ’
उपनिषदों में त्राटक के आन्तर , बाह्य औ मध्य -इस प्रकार तीन भेद किये गये हैं । हठयोग के ग्रन्थों में प्रकार -भेद नहीं है ।
नियम --- पाश्चात्यों का अनुकरण करने वाले कुछ लोग मद्यपान , मांसाहार तथा अम्ल -पदार्धादि अपथ्य -सेवन करते हुए भी ‘मैस्मेरिज्म ’ विद्या की सिद्धि के लिये त्राटक किया करते हैं । परन्तु ऐसे लोगों का अभ्यास पूर्ण नहीं होता । अनेक लोगों के नेत्र चले जाते हैं और अनेक पागल हो जाते हैं । जिन्होंने पथ्य का पालन किया है वही सिद्धि प्राप्त कर सके हैं ।
१ . निरिक्षेन्निश्चलदृशा सूक्ष्मलक्ष्यं समाहितः ।
अश्रुसम्पातपर्यन्तमाचार्यैस्त्राटकं स्मृतम् ॥ ( हठयोगप्रदीपिका )
२ . मोचनं नेत्ररोगाणां तन्द्रादीनां कपाटकम् ।
यत्नतस्त्राटकं गोप्य यथा हाटकपेटकम् ॥ ( हठयोगप्रदीपिका )
यम -नियमपूर्वक आसनों के अभ्यास से नाडी समूह मृदु हो जाने पर ही त्राटक करना चाहिये । कठोर नाडियों को आघात पहुँचते देरी नहीं लगती । त्राटक के जिज्ञासुओं को आसनों के अभ्यास के परिपाक काल में नेत्र के व्यायाम का अभ्यास करना विशेष लाभदायक है । प्रातःकाल में शान्तिपूर्वक दृष्टि को शनैः शनैः बायें , दायें , नीचे की ओर , ऊपर की ओर चलाने की क्रिया को नेत्र का व्यायाम कहते हैं । इस व्यायाम से नेत्र की नसें दृढ होती है । इसके अनन्तर त्राटक करने से नेत्र को हानि पहुँचने की भीति कम हो जाती है ।
त्राटक के अभ्यास से नेत्र और मस्तिष्क में उष्णता बढ जाती है । अतः नित्य जलनेति करनी चाहिये तथा रोज सुबह त्रिफला के जल से अथवा गुलाब जल से नेत्रों को धोना चाहिये । भोजन में पित्तवर्धक और मलाविरोध (कब्ज ) करने वाले पदार्थो का सेवन न करे । नेत्र में आँसू आ जाने के बाद फिर उस दिन दूसरी बार त्राटक न करे । केवल एक ही बार प्रातःकाल में करे । वास्तव में त्राटक का अनुकूल समय रात्रि के को से पाँच बजे तक है । शान्ति के समय में चित्त की एकाग्रता बहुत शीघ्र होने लगती है । एकाध वर्षपर्यन्त नियमित रुप से त्राटक करने से साधक के संकल्प सिद्ध होने लगते है , दूसरे मनुष्यें के ह्रदय का भाव मालूम होने लगता है , सुदूर स्थान में स्थित पदार्थ अथवा घटना का सम्यक् प्रकार से बोध हो जाता है
५ . क्षालन ---
रुद्रयामल प्रोक्त पञ्चस्वर (पञ्चकर्म - षट्कर्म ) योग में क्षालन से अर्थ है नाडियोम का प्रक्षालन । यहाँ मुख्य रुप से शीर्षासन से इसे को कहा गया है । हठयोग में इसकी अन्य विधि है ।
ऊद्र्ध्वे मुण्डासनं कृत्वा अधोहस्ते जपं चरेत् ।
यदि त्रिदिनमाकर्तु समर्थो मुण्डिकासनम् ॥
तदा हि सर्वनाड्यश्च वशीभूता न संशयः ।
नाडीक्षालनयोगेन मोक्षदाता स्वय्म भवेत् ॥ (रुद्र० ३५ .३२ .३३ )
( क ) गजकर्म या गजकरणी ---
हाथी जैसें सूँड से जल खींच फेंक देता है , वैसे गजकर्म में किया जाता है । अतःइसका नाम गजकर्म या गजकरणी हुआ । यह कर्म भोजन से पहले करना चाहिये । विषयुक्त या दूषित भोजन करनें में आ गया हो तो भोजन के पीछे भी किया जा सकता है । प्रतिदिन दन्तधावन के पश्चात् इच्छा भर जल पीकर अँगुली मुख में उलटी कर दे । क्रमशः बढा हुआ अभ्यास इछामात्र से जल बाहर फेंक देगा । भीतर गये जल को ज्योलीकर्म से भ्रमा कर फेंकना और अच्छा होता है । जब जल स्वच्छ आ जाय तब जानना चाहिये कि अब मैल मुख की राह नहीं आ रहा है । पित्तप्रधान पुरुषों के लिये यह क्रिया हितकर है ।
( ख ) कपालभातिकर्म ---
अर्थात लोहकार की भस्त्रा (भाथी ) के समान अत्यन्त शीघ्रता से क्रमशः रेचक -पूरक प्राणायाम को शान्तिपूर्वक करना योगशास्त्र में कफदोष का नाशक कह गया है तथा क्रिया ‘कपालभाति ’ नाम से विख्यात है ।
जब सुषुमना में से अथवा फुफ्फुस में से श्वासनलिका द्वारा कफ बार -बार ऊपर आता हो अथवा प्रतिश्याय (जुकाम ) हो गया हो तब सूत्रनेति और धौतिक्रिया से इच्छित शोधन नहीं होता । ऐसे समय पर यह कपालभाति लाभदायक है । इस क्रिया से फुफ्फुस और समस्त कफवहा नाडियों में इकट्ठा हुआ कफ कुच कुछ जल जाता है और कुछ प्रस्वेदद्वार से बाहर निकल जाता है , जिससे फुफ्फुस -कोशों की शुद्धि होकर फुफ्फुस बलवान् होते हैं । साथ -साथ सुषुम्ना , मस्तिष्क और आमाशय की शुद्धि होकर पाचनशक्ति प्रदीप्त होती है ।
नियम --- परंतु उरःक्षत , ह्रदय की निर्बलता , वमनरोग , हुलास (उबाक ), हिक्का , स्वरभङु , मन की भ्रमित अवस्था , तीक्ष्ण ज्वर , निद्रानाश , ऊर्ध्वरक्तपित्त , अम्लपित्त इत्यादि दोषों के समय , यात्रा में और वर्षा हो रही हो , ऐसे समय पर इस क्रिया को न करे ।
अजीर्ण , धूप में भ्रमण से पित्तवृद्धि , पित्तप्रकोपजन्य रोग , जीर्ण कफ -व्याधि , कृमि , रक्तविकार , आमवात , विषविकार और त्वचारोगदि व्याधियों को दूर करने के लिये यह क्रिया गुणकारी है । शरद् ऋतु में स्वाभाविक पित्तवृद्धि होती रहती है । ऐसे समय पर आवश्यकतानुसार यह क्रिया की जा सकती है ।
षट्कर्म से रोग निवारण
हठयोग के अनुसार भौतिक शरीर के दोषों को दूर करने लिये एवं स्वस्थ बने रहने के लिये षटकर्म , आसन , प्राणायाम , मुद्रा , धारण एवं ध्यान का आलम्बन लेना चाहिये । षटकर्म का उपयोग प्रवृद्ध कफ -दोष को दूर करके वात , पित्त एवं कफ एन तीनों दोषों को समभाव में स्थापित करने के लिये होता है । यदि कफ -दोष बढा न हो तो , जिस अङु में विकार या अशक्ति प्रतीत हो , उसी अङु को बलवान बनाने या उक्त अङु से विकार को दूर करने के लिये षट्कर्मों में से यथावश्यक दो या तीन या चार कर्मो का अभ्यास करना चाहिये । १ . धौति , वस्ति , नेति , त्राटक , नौलिक एवं कपालभाति -इन छः क्रियाओं को षट्कर्मो कहते हैं । धौति कर्म कण्ठ से आमाशय तक के मार्ग को स्वच्छ करके सभी प्रकार के कफ -रोगों का नाश कर देता है । यह विशेषरुप से कफप्रधान कास , श्वास , प्लीहा एवं कुष्ठरोग में लाभकारी है । २ . वस्ति -कर्मद्वारा गुदामार्ग एवं छोटी आँत के निचले हिस्से की सफाई हो जाती है । इससे अपानवायु एवं मलान्त्र के विकार से उत्पन्न होने वाले रोगों का शमन हो जाता है । आँतो की गर्मी शान्त होती है , कोष्ठबद्धता दूर होती है । आँतो में स्थित -संचित दोष नष्ट होते हैं । जठराग्नि की वृद्धि होती है । अनेक उदररो नष्ट होते है । वस्तिकर्म करने से वात -पित्त एव्म कफ से उत्पन्न अनेक रोग तथा गुल्म , प्लीहा , और जलोदर दूर होते हैं । ३ . नेतिकर्म नासिकामार्ग को स्वच्छ कर कपाल -शोधन का कार्य करता हैं यह विशेषरुप से नेत्रों को उत्तम दृष्टि प्रदान करता है और गले से ऊपर होने वाले दाँत , मुख , जिह्रा , कर्ण एवं शिरोरोगों को नष्ट करता है । ४ . त्राटक -कर्मद्वारा नेत्रों के अनेक रोग नष्ट होते हैं एवं तन्द्रा , आलस्य आदि दोष नष्ट होते हैं । ५ उदर -रोग एवं अन्य सभी दोषों क नाश करने के लिये नेति प्रमुख है । यह मन्दाग्नि को नष्टकर जठराग्नि की वृद्धि करता है तथा भुक्तान्न को सुन्दर प्रकार से पचाने की शक्ति प्रदान करता है । इसका अभ्यास करने से वातादि दोषों का शमन होने से चित्त सदा प्रसन्न रहता है । ६ . कपालभाति विशेषरुप से कफ -दोष का शोषण करने वाली है । षट्कर्मो का अभ्यास करने से जब शरीरन्तर्गत कफ -दोष मलादिक क्षीण हो जाते है , तब प्राणायाम का अभ्यास करने से अधिक शीघ्र सफलता मिलती है ।
17….संक्षिप्त विवरण - शरीर शोधन
अन्य क्रियाओं द्वारा शरीर शोधन
जिन्हें पित्त की अधिक शिकायत रहती है , उनके लिये गजकर्णी या कुजल -क्रिया लाभदायक रहती है । इस क्रिया में प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होने के बाद पर्यन्त मात्र में नमक मिश्रित कुनकुना जल पीकर फिर वमन कर दिया जाता हैं । इसमे आमाशयस्थ पित्त का शोधन होता है । जिन्हें मन्दाग्नि की शिकायत है या जिनका स्वास्थ्य उत्तम भोजन करने पर भी सुधरता नहीं है , उन्हें अग्निसार नामक क्रिया का अभ्यास करना चाहिये । इस क्रिया में नाभिग्रन्थि को बार -बार मेरु -पृष्ठ में लगाना होता हैं । एक सौं बार लगा सकने का अभ्यास हो जाने पर समझना चाहिये कि इस क्रिया में परिपक्वता प्राप्त हो गयी है । अतः यह सभी प्रकार के उदर -रोगोम को दूर करने में सहायक हैं ।
अष्टाङुयोग से रोग निवारण
आसन का अभ्यास शरीर से जडता , आलस्य एवं चञ्चलता को दूर कर सम्पूर्ण स्नायु -संस्थान एवं प्रत्येक अङु को पुष्ट के लिये होता है । इसके अभ्यास से शरीर के अङो के सभी भागों में एवं सूक्ष्मातिसूक्ष्म नाडियों में रक्त पहुँचता है , सभी ग्रन्थियाँ सुचारुरुप से कार्य करती है । स्नायु -संस्थान बलवान् हो जाने पर साधक काम , क्रोध , भय आदि के आवेगों को सहने में समर्थ होता है । वह मानस -रोगी नहीं बनता । शरीर का स्वास्थ्य , मस्तिष्क , मेरुदण्ड , स्नायु -संस्थान , ह्रदय एवं फेफडे तथा उदर के बलवानू होने निर्भर है । अतःआसनों का चुनाव इन पर पडने वाले प्रभावों को दृष्टि में रखकर करना चाहिये । जिसका जो अङ कमजोर हो उसे सार्वाङिक व्यायाम के आसनों का अभ्यास करने के साथ -साथ उन दुर्बल अङो को पुष्ट करने वालो आसनों का अभ्यास विशेषरुप से करना चाहिये ।
ध्यान के उपयोगी पद्मासन आदि को सर्वरोगनाशक इसलिये कहा जाता है कि इन आसनों से ध्यान या जप में बैठने पर शरीर में साम्यभाव , निश्चलता , शान्ति आदि गुण आ जाते हैं । जो भौतिक स्तर पर सत्त्वगुण की वृद्धि करने में सहायक होते हैं । आरोग्य की दृष्टी से किये जाने वाले आसनों में पश्चिमोत्तान , मत्स्येन्द्र , गोरक्ष , सर्वाङ , मयूर , भुजंग , शलभ , धनु , कुक्कुट , आकर्षणधनु एवं पद्म -आसन मुख्य हैं ।
आसनों को शनैः शनैः किया जाय , जिससे अङो एव्म नाडियों में तनाव , स्थिरता , संतुलन , सहनशीलता एवं शिथिलता आ सके । अपनी पूर्ववत स्थिति में धीरे -धीरे ही आना चाहिये । जो अङु रोगी हो , उस अङु पर बोझ डालने वाले आसनों का धर्म से युक्त हैं , उन्हें उन दिनों पेट के आसन नहीं करने चाहिये । जिस आसन का प्रभाव जिस र्ग्लैड्स या नाडी -चक्र पर पडता है -- आसन करते समय वहीं ध्यान केन्द्रित करना चाहिये तथा गायत्री आदि मन्त्रों का या तेज , बल , शक्ति देन वाले देने वाले मन्त्रों का यथाशक्ति स्मरण करना चाहिये । एक आसन के बाद उसका प्रतियोगी आसन भी करना चाहिये । यथा -पश्चिमोत्तान आसन का प्रतियोगी भुजंगासन और शलभासन है । हस्तपादासन का प्रतियोगी चक्रासन है । सर्वाङासन का अभ्यास आवश्यक है । सूर्यनमस्कार को अन्य आसनों के अभ्यास के पूर्व कर लेना लाभदारी है ।
i प्राणायाम का अभ्यास शरीरस्थ सभी दोषों का निराकरण कर प्राणमयकोष एवं सूक्ष्म शरीर को नीरोगं तथा पुष्ट बनाता है । नाडी - शोधन का अभ्यास करने के बाद की कुम्भक प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिये । प्राणायाम के सभी अभ्यास युक्तिपूर्वक शनैः शनैः ही करने चाहिए तथा भस्त्रिका प्राणायाम को छोडकर सभी शेष प्राणायामों में रेचक् एवं पूरक , दोनों की क्रियाएँ बहुत धीरे - धीरे करनी चाहिये । प्रत्येक कुम्भक की अपनी - अपनी दोषनाशक विशेष शक्ति है । अतःप्रवृद्ध दोष का विचार करके ही उसके दोषनाशक कुम्भक का अभ्यास करना चाहिये । सूर्यभेद प्राणायाम पित्तवर्धक , जरादोषनाशक , वातहर , कपालदोष एवं कृमिदोष को नष्ट करने वाला है । उज्जायी कफ - रोग , क्रूरवायु , अजीर्ण , जलोदर , आमवात , क्षय , कास , ज्वर एवं प्लीहा को नष्ट करता है । स्वास्थ्य एवं पुष्टि की प्राप्ति के लिये उज्जायी प्राणायाम का विशेष रुप से अभ्यास करना चाहिये । शीतली प्राणायाम अजीर्ण , कफ , पित्त , तृषा , गुल्म , प्लीहा एवं ज्वर को नष्ट करता हैं । भस्त्रिका प्राणायाम वात - पित्त - कफ - हर , शरीराग्निवर्धक एवं सर्वरोगहर हैं । व्यवहार में संध्योपासना के उपरान्त एवं जप से पूर्व नाडी - शोधन , उज्जायी एवं भस्त्रिका प्राणायाम का नित्य अभ्यास करने का प्रचलन है ।
अष्टाङ योग से रोग निवारण
आसन का अभ्यास शरीर से जडता , आलस्य एवं चञ्चलता को दूर कर सम्पूर्ण स्नायु -संस्थान एवं प्रत्येक अङु को पुष्ट के लिये होता है । इसके अभ्यास से शरीर के अङो के सभी भागों में एवं सूक्ष्मातिसूक्ष्म नाडियों में रक्त पहुँचता है , सभी ग्रन्थियाँ सुचारुरुप से कार्य करती है । स्नायु -संस्थान बलवान् हो जाने पर साधक काम , क्रोध , भय आदि के आवेगों को सहने में समर्थ होता है । वह मानस -रोगी नहीं बनता । शरीर का स्वास्थ्य , मस्तिष्क , मेरुदण्ड , स्नायु -संस्थान , ह्रदय एवं फेफडे तथा उदर के बलवानू होने निर्भर है । अतःआसनों का चुनाव इन पर पडने वाले प्रभावों को दृष्टि में रखकर करना चाहिये । जिसका जो अङ कमजोर हो उसे सार्वाङिक व्यायाम के आसनों का अभ्यास करने के साथ -साथ उन दुर्बल अङो को पुष्ट करने वालो आसनों का अभ्यास विशेषरुप से करना चाहिये ।
ध्यान के उपयोगी पद्मासन आदि को सर्वरोगनाशक इसलिये कहा जाता है कि इन आसनों से ध्यान या जप में बैठने पर शरीर में साम्यभाव , निश्चलता , शान्ति आदि गुण आ जाते हैं । जो भौतिक स्तर पर सत्त्वगुण की वृद्धि करने में सहायक होते हैं । आरोग्य की दृष्टी से किये जाने वाले आसनों में पश्चिमोत्तान , मत्स्येन्द्र , गोरक्ष , सर्वाङ , मयूर , भुजंग , शलभ , धनु , कुक्कुट , आकर्षणधनु एवं पद्म -आसन मुख्य हैं ।
आसनों को शनैः शनैः किया जाय , जिससे अङो एव्म नाडियों में तनाव , स्थिरता , संतुलन , सहनशीलता एवं शिथिलता आ सके । अपनी पूर्ववत स्थिति में धीरे -धीरे ही आना चाहिये । जो अङु रोगी हो , उस अङु पर बोझ डालने वाले आसनों का धर्म से युक्त हैं , उन्हें उन दिनों पेट के आसन नहीं करने चाहिये । जिस आसन का प्रभाव जिस र्ग्लैड्स या नाडी -चक्र पर पडता है -- आसन करते समय वहीं ध्यान केन्द्रित करना चाहिये तथा गायत्री आदि मन्त्रों का या तेज , बल , शक्ति देन वाले देने वाले मन्त्रों का यथाशक्ति स्मरण करना चाहिये । एक आसन के बाद उसका प्रतियोगी आसन भी करना चाहिये । यथा -पश्चिमोत्तान आसन का प्रतियोगी भुजंगासन और शलभासन है । हस्तपादासन का प्रतियोगी चक्रासन है । सर्वाङासन का अभ्यास आवश्यक है । सूर्यनमस्कार को अन्य आसनों के अभ्यास के पूर्व कर लेना लाभदारी है ।
iप्राणायाम का अभ्यास शरीरस्थ सभी दोषों का निराकरण कर प्राणमयकोष एवं सूक्ष्म शरीर को नीरोगं तथा पुष्ट बनाता है । नाडी -शोधन का अभ्यास करने के बाद की कुम्भक प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिये । प्राणायाम के सभी अभ्यास युक्तिपूर्वक शनैः शनैः ही करने चाहिए तथा भस्त्रिका प्राणायाम को छोडकर सभी शेष प्राणायामों में रेचक् एवं पूरक , दोनों की क्रियाएँ बहुत धीरे -धीरे करनी चाहिये । प्रत्येक कुम्भक की अपनी -अपनी दोषनाशक विशेष शक्ति है । अतःप्रवृद्ध दोष का विचार करके ही उसके दोषनाशक कुम्भक का अभ्यास करना चाहिये । सूर्यभेद प्राणायाम पित्तवर्धक , जरादोषनाशक , वातहर , कपालदोष एवं कृमिदोष को नष्ट करने वाला है । उज्जायी कफ -रोग , क्रूरवायु , अजीर्ण , जलोदर , आमवात , क्षय , कास , ज्वर एवं प्लीहा को नष्ट करता है । स्वास्थ्य एवं पुष्टि की प्राप्ति के लिये उज्जायी प्राणायाम का विशेष रुप से अभ्यास करना चाहिये । शीतली प्राणायाम अजीर्ण , कफ , पित्त , तृषा , गुल्म , प्लीहा एवं ज्वर को नष्ट करता हैं । भस्त्रिका प्राणायाम वात -पित्त -कफ -हर , शरीराग्निवर्धक एवं सर्वरोगहर हैं । व्यवहार में संध्योपासना के उपरान्त एवं जप से पूर्व नाडी -शोधन , उज्जायी एवं भस्त्रिका प्राणायाम का नित्य अभ्यास करने का प्रचलन है ।
18…संक्षिप्त विवरण - स्वरयोग से रोग निवारण
. स्वरयोग से रोग निवारण
रोग -निवारण के लिये स्वर -योग का आश्रय भी लिया जाता है । नीरोगता के लिये भोजन सदा दाहिना स्वर (श्वास ) चलने पर करना चाहिये । वामस्वर शीतल एवं दक्षिणस्वर उष्ण माना जाता है । इसके अनुसार ही वात एवं कफ -प्रधान रोगों में दक्षिण नासिका के श्वास को चलाया जाता है एवं पित्तप्रधान रोग में वाम -स्वर से श्वास को चलाया जाता है । सामान्य नियम यह है कि रोग के प्रारम्भकाल में जिस नासिका से श्वास चल रहा होता है , उसे बंद करके दूसरी नासिका से श्वास रोग -शमन होने तक चलाया जाता है । इस स्वर -परिवर्तन से प्रवृद्ध दोष का संशमन हो जाता है । स्वरयोग की जानकारी के लिये शिव स्वरोदय एवं स्वर -चिन्तामणि नामक ग्रन्थों का अवलोकन करना चाहिये ।
योग सम्बन्धी बन्ध एवं मुद्राओं से रोग -निवारण
मुद्राओं के अभ्यास में महामुद्रा , विपरीतकरणी , खेचरी , मूलबन्ध , उड्डीयान -बन्ध एवं जालन्धरबन्ध मुख्य हैं । महामुद्रा क्षय , कुष्ठ , आवर्त , गुल्म , अजीर्ण आदि रोगों एवं सभी दोषों को नष्ट करती है । इसके अभ्यास से पाचन -शक्ति की प्रचण्ड वृद्धि होकर विष को भी पचाने की क्षमता प्राप्त होती है । महामुद्रा के साथ महाबन्ध एवं महावेध का भी अभ्यास किया जाता है । इन तीनों के अभ्यास से वृद्धत्व दूर होता है एवं अनेक शारीरिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है । खेचरी मुद्रा के अभ्यास से शरीर में अमृतत्व -धर्म की वृद्धि होती है । सिद्धियों की प्राप्ति होती है । शरीर की सोमकला का विकास होता है तथा देह -क्षय की प्रक्रिया रुक जाती है । उड्डीयान का अभ्यास उदर एवं नाभि से नीचे स्थिति अङों के रोगों को दूरकर पुरुषत्व की अभिवृद्धि करता है । जननाङु एवं प्रजननाङु के रोगों से पीडित नर नारियों को उड्डीयानबन्ध का विशेष अभ्यास करना चाहिये । जालन्धर बन्ध से कण्ठ -रोगों एवं शिरोरोगों का नाश होता है तथा मूलबन्ध का अभ्यास गुदा एवं जननेन्द्रिय पर प्राण एवं अपान पर नियन्त्रण प्रदान करता है । उड्डीयान एवं जालन्धरबन्धं का अभ्यास तो प्राणायाम के समय ही किया जाता है , परंतु मूलबन्ध का अभ्यास सतत करना चाहिये । विपरीतकरणी मुद्रा का ठीक -ठीक अभ्यास वलीपलित को दूर कर युवावस्था प्रदान करता है ।
उपर्युक्त मुद्राओं के अतिरिक्त घेरण्डसंहिताप्रोक्त कुछ अन्य मुद्राओं का अभ्यास भी रोगनाश , वलीपलितविनाश एवं स्वास्थ्य -लाभ के लिये उपयोगी है । इनमें से नभोमुद्रा एवं माण्डूकीमुद्रा तालुस्थित अमृतपान में सहायक होने के कारण सभी रोगों का नाश करने वाली है । अश्विनी मुद्रा गुह्यरोगों का नाश करने वाली , अकालमृत्यु को दूर करने वाली तथा बल एवं पुष्टि को प्रदान करने वाली है । पाशिनी मुद्रा से बल एवं पुष्टि की प्राप्ति होती है । तडागी मुद्रा एवं भुजंगिनी मुद्रा -ये दोनों ही उदर के अजीर्णादि रोगों को नष्टकर दीर्घ जीवन प्रदान करती हैं ।
रोगों को दूर करने में ध्यान अथवा चिन्तन का महत्त्वपूर्ण स्थान है । ध्यान से शरीर , प्राण , मन , ह्रदय एवं बुद्धि में शान्ति , पवित्रता एवं निर्मलता आती है । ‘सद प्राणिमात्र के कल्याण का विचार करने से एवं सभी सुखी हों , नीरोग हों , शान्त हों ’ इस प्रकार की भावनाओं की तरंगो को सभी दिशाओं में प्रसारित करने से स्वयं को सुख तथा शान्ति की प्राप्ति होती है । व्यक्ति जैसा चिन्तन करता है , प्रायः वह वैसा बन जाता है । ‘मैं नीरोग हूँ , स्वस्थ हूँ - ऐसा चिन्तन निरन्तर दृढतापूर्वक करते रहने से आरोग्य बना रहता है । इसे आत्मसम्मोहन ‘ऑटो सजेशन ’ की विधि कहते हैं । इसी प्रकार प्रबल संकल्पशक्ति के द्वारा अपने या दूसरी के रोगों को भी दूर किया जाता है । रोगनिवारण के लिये प्रमुख बात यह है कि रोग होने पर उसका चिन्तन ही न करे , उसकी परवाह ही न करे । रोग का चिन्तन करने से रोग बद्धमूल हो जाता है एवं व्यक्ति का मनोबल दुर्बल हो जाता है । मानसिक रोगों का संकल्पशक्ति एवं प्रज्ञाबल से निवारण करना चाहिये एवं शारीरिक रोगों का औषधों से । इन रोगों के उन्मूलन में यौगिक साधनों का अद्भुत योगदान रहा है ।
शारीरिक एवं मानसिक रोगों से मुक्ति चाहने वालों को योग -क्रियाओं का अभ्यास करने के साथ -साथ रोगोत्पादक सभी मूल कारणों का त्याग करना चाहिये तथा अपने लिये अनुकूल एवं चिकित्साशास्त्र द्वारा निर्दिष्ट सात्त्विक पथ्य , सदाचार एवं सत्कर्म का सेवन करना चाहिये । यथासम्भव अनिष्ट -चिन्तन से बचना चाहिये तथा चित्त को राग -द्वेष -मोहादि दोषों से दूर करना चाहिये । सम्पूर्ण दुःखों का मूल कारण तमोगुणजनित अज्ञान , लोभ , क्रोध , तथा मोह है । त्रिगुण के प्रभाव तथा अज्ञान के बन्धन से मुक्त होने का एकमात्र योग है तथा योग -बल से भी बडी शक्ति है भगवान् की अनुग्रह शक्ति ।
अतएव अहंता -ममता का त्याग करके भगवच्चरणों का एकमात्र आश्रय लेकर योगसाधना करने से शारीरिक व्यधि के साथ -साथ त्रिविध ताप एवं भवव्यधि भी कट जाती है और ऐसा साधक पूर्णतम आनन्द को प्राप्त करने में सर्वथा समर्थ हो जाता है ।
19…संक्षिप्त विवरण - कुण्डलिनीयोग
कुण्डलिनीयोग
कुण्डलिनीयोग , कुण्डलिनीशक्ति , षटचक्र आदि का पतञ्जलि के योगसूत्रों में कहीं उल्लेख नहीं है , किन्तु यह निश्चित है कि कुण्डलिनीयोग प्राचीन भारतीय योग की एक विशिष्ट पद्धति है । आगम और तन्त्रशास्त्र की विभिन्न शाखाओं में इसका वर्णन मिलता है । कुछ आचार्य ‘अष्टा चक्रा नवद्वारा ’ (१०।२।३१ ) इत्यादि अथर्ववेदीय मन्त्र में कुण्डलिनी योग योग का उल्लेख मानते हैं । प्रायः सभी आगमिक और तान्त्रिक आचार्य प्रसुप्तभुजगाकारा , सार्धत्रिवलाकृति , मृणालतन्तुनीयसी मूलाधार स्थित शक्ति को कुण्डलिनी के नाम से जानते हैं । जिस योगपद्धति की सहायता से इस कुण्डलिनी शक्ति को जगाकर सुषुम्णा मार्ग द्वारा षट्चक्र का भेदन कर सहस्त्रारकचक्र तक पहुँचाया जाता है और वहाँ उसका अकुल शिव से सामरस्य सम्पादन कराया जाता है , उसी का नाम कुण्डलिनीयोग है । आधारों अथवा चक्रों आदि के विषय में मतभेद होते हुए भी मूलाधार स्थित कुण्डलिनी शक्ति का सहस्त्रार स्थित अपने इष्टदेव से सामरस्य का सम्पादन सभी मतों में निर्विवाद रुप से मान्य है ।
कुण्डलिनीयोग की विधि ---
यहाँ संक्षेप में उसकी विधि इस प्रकार वर्णित है -यम और नियम के नित्य -नियमित आदरपूर्वक निरन्तर अभ्यास में लगा योगी साधक गुरुमुख से मूलाधार से सहस्त्रार -पर्यन्त कुण्डलिनी के उत्थापन क्रम को ठीक से समझ लेने के उपरान्त , पवन और दहन के आक्रमण से प्रतप्त कुण्डलिनी शक्ति को , जो कि स्वयम्भू लिंग को वेष्टित कर सार्धत्रिवलयकार में अवस्थित , है हूँकार बीज का उच्चारण करते हुए जगाता है और स्वयम्भू लिंग के छिद्र से निकाल कर उसे ब्रह्यद्वार तक पहुँचा देता है । कुण्डलिनीशक्ति पहले मूलाधार स्थित स्वयम्भू लिंग का , तब अनाहतचक्र स्थित की सहायता से सहस्त्रदल चक्र में आज्ञाचक्र स्थित इतर लिंग का भेद करती हुई ब्रह्मनाडी की सहायता से सहस्त्रदल चक्र मे प्रविष्ट होकर इतर लिंग का भेद करती हुई ब्रह्मनाडी की सहायता से सहस्त्रदल चक्र में प्रविष्ट होकर परमानन्दमय शिवपद में प्रतिष्ठित हो जाती है । योगी अपने जीवभाव के साथ इस कुलकुण्डलिनी को मूलाधार से उठाकर सहस्त्राचक्र तक ले जाता है और वहाँ उसको परबिन्दु स्थान में स्थित शिव (पर लिंग ) के साथ समरस कर देता है । समरसभावापन्न यह कुण्डलिनीशक्ति सहस्त्रारचक्र में लाक्षा के वर्ण के समान परमामृत का पान तृप्त हो जाती है और इस परमानन्द की अनुभूति को मन में संजोये वह पुनः मूलाधारचक्र में लौट आती है । यही है कुण्डलिनीयोग की इतिकर्तव्यता । इसके सिद्ध हो जाने योगी जीवभाव से मुक्त हो जाता है और शिवभावापन्न (जीवन्मुक्त ) हो जाता है ।
कुलकुण्डलिनी शक्ति कैसे सहस्त्रार स्थित अकुलशिव की ओर उन्मुख होती है और वहाँ शिव के साथ सामरस्य भाव का अनुभव कर पुनः कैसे अपने मूल स्थान में आ जाती है , इसकी अति संक्षिप्त प्रक्रिया नित्याषोडशिकार्णव (४ ।१२ -१६ ) में वर्णित है । इसी प्रकार चार पीठों और चार लिंगो का स्वरुप हमें योगिनी ह्रदय (१ ।४१ -४७ ) में अधिक स्पष्ट रुप में मिलता है ।
कुण्डलिनीशक्ति
मानवलिंग शरीर में सुषुम्नानाडी के सहारे ३२ पद्मों की स्थिति मानी गई है । सबसे नीचे और सबस ऊपर दो सहस्त्रापद्म स्थित हैं । नीचे कुलकुण्डलिनी में स्थित अरुण वर्ण सहस्त्रापद्म ऊर्ध्वमुख तथा ऊपर ब्रह्मारन्ध्र स्थित श्वेत वर्ण सहस्त्रारपद्म अधोमुख हैं । इनमें से अधः सहस्त्रार को कुलकुण्डलिनी और ऊर्ध्व सहस्त्रार को अकुण्डकुण्डलिनी कहा जाता है । अकुलकुण्डलिनी प्रकाशात्मक अकारस्वरुपा और कुलकुण्डलिनी विमर्शात्मक हकारस्वरुण मानी जाती है ।
इन दो कुण्डलिनियों के अतिरिक्त तन्त्रशास्त्र के ग्रन्थों में प्राणकुण्डलिनी का भी वर्णन मिलता है । मूलाधार में जैसे कुण्डलिनी का निवास है , उसी तरह से ह्रदय में भी ‘सार्धत्रिवलया प्राणकुण्डलिनी ’ रहती है । मध्यनाडी सुषुम्ना के भीतर चिदाकाश (बोधगमन ) रुप शून्य का निवास है । उससे प्राणशक्ति निकलती है । इसी को अनच्क कला भी कहते हैं । इसमें अनच्क (अच् =स्वर से रहित ) हकार का निरन्तर नदन होता रहता है । यह नाद भट्टारक की उन्मेष दशा है , जिससे कि प्राणकुण्डलिनी की गति ऊर्ध्वोन्मुख होती है , जो श्वास -प्रश्वास , प्राण -अपान को गति प्रदान करती है और जहाँ इनकी एकता का अनुसन्धान किया जा सकता है । मध्यनाडी में स्थित बिना क्रम के स्वाभविक रुप से उच्चरित होने वाली यह प्राणशक्ति को कुण्डलिनी इसलिये कहते हैं कि मूलाधार स्थित कुण्डलिनी की तरह इसकी भी आकृति कुटिल होती है । जिस प्राणवायु का अपान अनुवर्तन करता है , उसकी गति होकर की लिखावट की तरह टेढी -मेढी होती है । प्राणशक्ति अपनी इच्छा से ही प्राण के अनुरुप कुटिल (घुमावदार ) आकृति धारण कर लेती है । प्राणशक्ति की यह वक्रता (कुटिलता =घुमावदार आकृति ) परमेश्वर की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का खेल है । प्राणशक्ति का एक लपेटा वाम नाडी इडा में और दूसरा लपेटा दक्षिण नाडी पिंगला में रहता है इस तरह से इसके दो वलय (घेरे ) बनते हैं । सुषुम्ना नाम की मध्य नाडी सार्ध कहलाती है । इस प्रकार यह प्राणशक्ति भी सार्धत्रिवलया है । वस्तुतः मूलाधार स्थित कुण्डलिनी में प्राणशक्ति का भी निवास है , किन्तु ह्रदय में इसकीं स्पष्ट अभिव्यक्ति होने से ब्राह्मणवसिष्ठन्याय से उसका यहाँ पृथक् उल्लेख कर दिया गया है । इसका प्रयोजन अजपा (हंसगायत्री ) जप को सम्पन्न करना है ।
20…संक्षिप्त विवरण - नाडीचक्र का रहस्य
नाडीचक्र का रहस्य
षट्चक्र का निरुपण करते यहाँ नाडियों के सम्बन्ध समझ लेना चाहिए कि मेरुदण्ड के बाहर वाम भाग में चन्द्रात्मक इडा नाडी और दक्षिण भाग में सूर्यात्मक पिंगला नाडी अवस्थित है । मेरुदण्ड के मध्य भाग में वज्रा और चित्रिणी नाडी से मिली हुई त्रिगुणात्मिका सुषुम्ना नाडी का निवास है । इनमें सत्त्वगुणात्मिका चित्रिणी चन्द्ररुपा है , रजोगुणात्मिका वज्रा सूर्यरुपा है और तमोगुणात्मिका सुषुम्ना नाडी अग्निरुपा हैं । यह त्रिगुणात्मिका नाडी कन्द के मध्य भाग में सहस्त्रार -पर्यन्त विस्तृत है । इसका आकार खिले हुए धतूरे के पुष्प के सदृश है । इस सुषुम्ना नाडी के मध्य भाग में लिंग से मस्तक तक विस्तृत दीपशिखा के समान प्रकाशमान वज्रा नाडी स्थित है । उस वज्रा नाडी के मध्य में चित्रिणी नाडी का निवास है । यह प्रणव से विभूषित है और मकडी के जाले के समान अत्यन्त सूक्ष्म आकार की है । योगी ही इसको योगज ज्ञान से देख सकते हैं ।
मेरुदण्ड के मध्य में स्थित सुषुम्ना और ब्रह्मनाडी के बीच में मूलाधार आदि छः चक्रों को भेद कर यह नाडी सहस्त्रार चक्र में प्रकाशमान होती हैं । इस चित्रिणी नाडी के मध्य में शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म नाडी स्थित है । यह नाडी मूलाधार स्थित स्वयम्भू लिंग के छिद्र के सहस्त्रार में विलास करने वाले परमशिव पर्यन्त व्याप्त है । यह नाडी विद्युत् के समान प्रकाशमान है । मुनिगण इसके कमलनाल के तन्तुओं के समान अत्यन्त सूक्ष्म आकार का मानस प्रत्यक्ष ही कर सकते हैं । इस नाडी के मुख में ही ब्रह्मद्वार स्थित है और इसी को योगीगण सुषुम्ना नाडी का भी प्रवेश द्वार मानते हैं ।
shriramjyotishsadan Me Pandit Ashu Bahuguna certified astrologer, neromologist, mantra anushthan & gamestone consultant. How may I help you? 9760924411
www astroashupandit.com
ॐ रां रामाय नम: श्रीराम ज्योतिष सदन, पंडित आशु बहुगुणा, संपर्क सूत्र- 9760924411